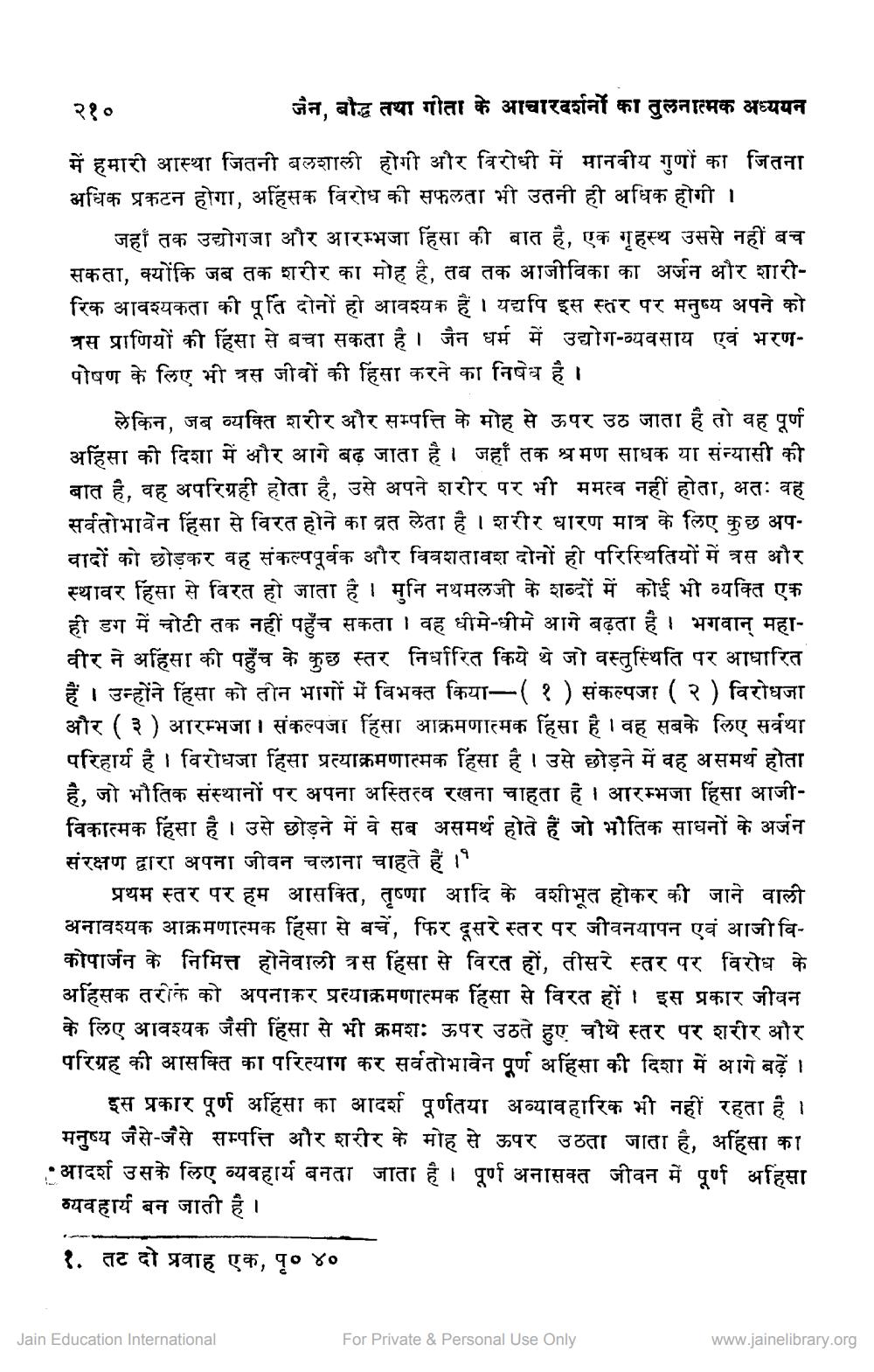________________
२१०
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
में हमारी आस्था जितनी बलशाली होगी और विरोधी में मानवीय गुणों का जितना अधिक प्रकटन होगा, अहिंसक विरोध की सफलता भी उतनी ही अधिक होगी ।
जहाँ तक उद्योगजा और आरम्भजा हिंसा की बात है, एक गृहस्थ उससे नहीं बच सकता, क्योंकि जब तक शरीर का मोह है, तब तक आजीविका का अर्जन और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति दोनों हो आवश्यक हैं । यद्यपि इस स्तर पर मनुष्य अपने को स प्राणियों की हिंसा से बचा सकता है। जैन धर्म में उद्योग-व्यवसाय एवं भरणपोषण के लिए भी त्रस जीवों की हिंसा करने का निषेध है ।
लेकिन, जब व्यक्ति शरीर और सम्पत्ति के मोह से ऊपर उठ जाता है तो वह पूर्ण अहिंसा की दिशा में और आगे बढ़ जाता है । जहाँ तक श्रमण साधक या संन्यासी की बात है, वह अपरिग्रही होता है, उसे अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं होता, अतः वह सर्वतोभावेन हिंसा से विरत होने का व्रत लेता है । शरीर धारण मात्र के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर वह संकल्पपूर्वक और विवशतावश दोनों ही परिस्थितियों में त्रस और स्थावर हिंसा से विरत हो जाता है। मुनि नथमलजी के शब्दों में कोई भी व्यक्ति एक ही डग में चोटी तक नहीं पहुँच सकता । वह धीमे-धीमे आगे बढ़ता है । भगवान् महावीर ने अहिंसा की पहुँच के कुछ स्तर निर्धारित किये थे जो वस्तुस्थिति पर आधारित हैं । उन्होंने हिंसा को तीन भागों में विभक्त किया - ( १ ) संकल्पजा ( २ ) विरोधजा और ( ३ ) आरम्भजा । संकल्पजा हिंसा आक्रमणात्मक हिंसा है । वह सबके लिए सर्वथा परिहार्य है । विरोधजा हिंसा प्रत्याक्रमणात्मक हिंसा है । उसे छोड़ने में वह असमर्थ होता है, जो भौतिक संस्थानों पर अपना अस्तित्व रखना चाहता है । आरम्भजा हिंसा आजीविकात्मक हिंसा है । उसे छोड़ने में वे सब असमर्थ होते हैं जो भौतिक साधनों के अर्जन संरक्षण द्वारा अपना जीवन चलाना चाहते हैं । "
प्रथम स्तर पर हम आसक्ति, तृष्णा आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली अनावश्यक आक्रमणात्मक हिंसा से बचें, फिर दूसरे स्तर पर जीवनयापन एवं आजीवि कोपार्जन के निमित्त होनेवाली त्रस हिंसा से विरत हों, तीसरे स्तर पर विरोध के अहिंसक तरीके को अपनाकर प्रत्याक्रमणात्मक हिंसा से विरत हों। इस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक जैसी हिंसा से भी क्रमशः ऊपर उठते हुए चौथे स्तर पर शरीर और परिग्रह की आसक्ति का परित्याग कर सर्वतोभावेन पूर्ण अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ें ।
इस प्रकार पूर्ण अहिंसा का आदर्श पूर्णतया अव्यावहारिक भी नहीं रहता है । मनुष्य जैसे-जैसे सम्पत्ति और शरीर के मोह से ऊपर उठता जाता है, अहिंसा का • आदर्श उसके लिए व्यवहार्य बनता जाता है । पूर्ण अनासक्त जीवन में पूर्ण अहिंसा व्यवहार्य बन जाती है ।
·
१. तट दो प्रवाह एक, पृ० ४०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org