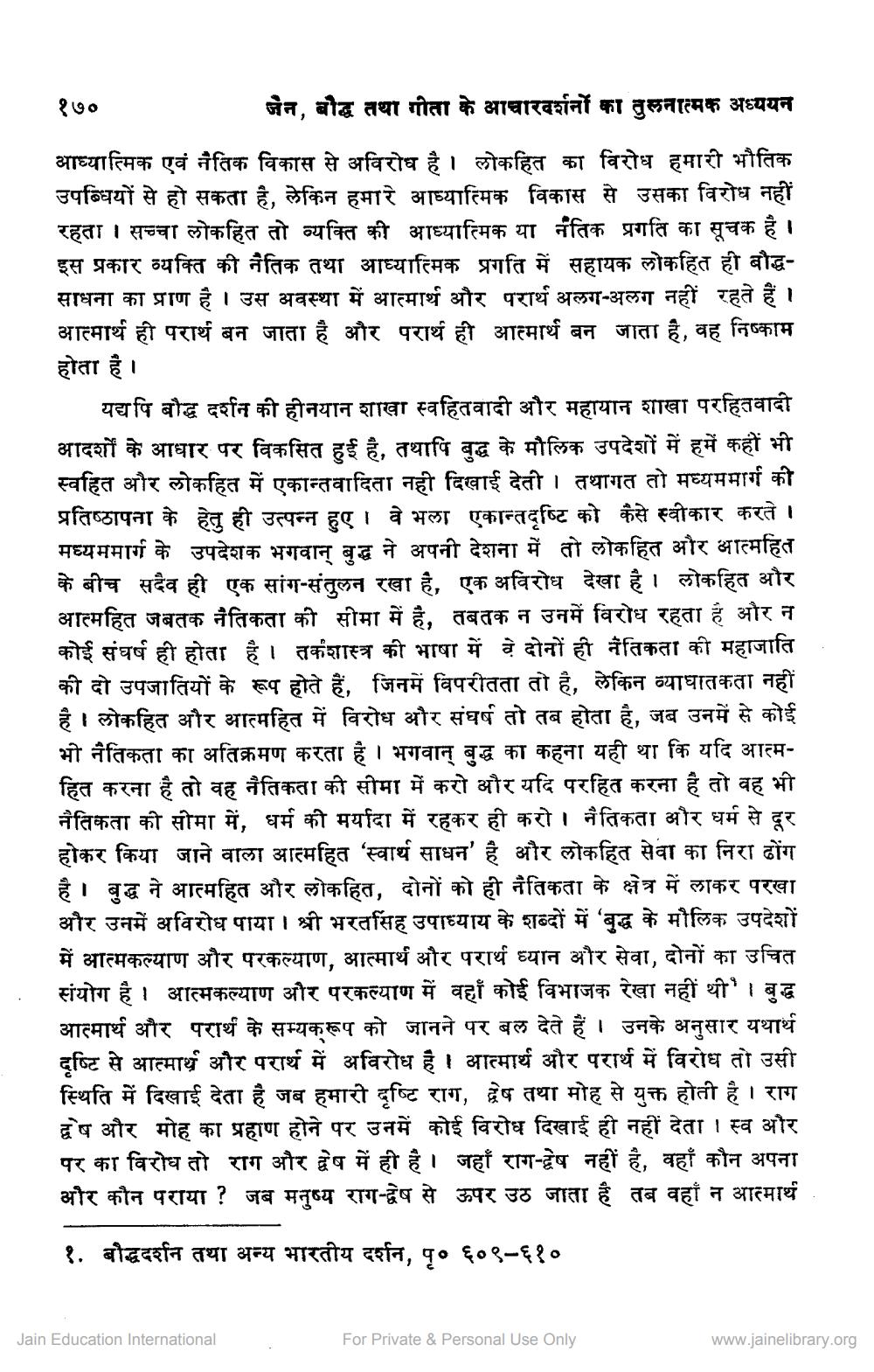________________
१७०
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास से अविरोध है। लोकहित का विरोध हमारी भौतिक उपब्धियों से हो सकता है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक विकास से उसका विरोध नहीं रहता । सच्चा लोकहित तो व्यक्ति की आध्यात्मिक या नैतिक प्रगति का सूचक है । इस प्रकार व्यक्ति की नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति में सहायक लोकहित ही बौद्धसाधना का प्राण है । उस अवस्था में आत्मार्थ और परार्थ अलग-अलग नहीं रहते हैं । आत्मार्थ ही परार्थ बन जाता है और परार्थ ही आत्मार्थ बन जाता है, वह निष्काम होता है।
यद्यपि बौद्ध दर्शन की हीनयान शाखा स्वहितवादी और महायान शाखा परहितवादी आदर्शों के आधार पर विकसित हुई है, तथापि बुद्ध के मौलिक उपदेशों में हमें कहीं भी स्वहित और लोकहित में एकान्तवादिता नही दिखाई देती। तथागत तो मध्यममार्ग की प्रतिष्ठापना के हेतु ही उत्पन्न हुए। वे भला एकान्तदृष्टि को कैसे स्वीकार करते । मध्यममार्ग के उपदेशक भगवान् बुद्ध ने अपनी देशना में तो लोकहित और आत्महित के बीच सदैव ही एक सांग-संतुलन रखा है, एक अविरोध देखा है। लोकहित और आत्महित जबतक नैतिकता की सीमा में है, तबतक न उनमें विरोध रहता है और न कोई संघर्ष ही होता है। तर्कशास्त्र की भाषा में वे दोनों ही नैतिकता की महाजाति की दो उपजातियों के रूप होते हैं, जिनमें विपरीतता तो है, लेकिन व्याघातकता नहीं है। लोकहित और आत्महित में विरोध और संघर्ष तो तब होता है, जब उनमें से कोई भी नैतिकता का अतिक्रमण करता है । भगवान् बुद्ध का कहना यही था कि यदि आत्महित करना है तो वह नैतिकता की सीमा में करो और यदि परहित करना है तो वह भी नैतिकता की सीमा में, धर्म की मर्यादा में रहकर ही करो। नैतिकता और धर्म से दूर होकर किया जाने वाला आत्महित 'स्वार्थ साधन' है और लोकहित सेवा का निरा ढोंग है। बुद्ध ने आत्महित और लोकहित, दोनों को ही नैतिकता के क्षेत्र में लाकर परखा और उनमें अविरोध पाया। श्री भरतसिंह उपाध्याय के शब्दों में 'बुद्ध के मौलिक उपदेशों में आत्मकल्याण और परकल्याण, आत्मार्थ और परार्थ ध्यान और सेवा, दोनों का उचित संयोग है। आत्मकल्याण और परकल्याण में वहाँ कोई विभाजक रेखा नहीं थी। बुद्ध आत्मार्थ और परार्थ के सम्यकरूप को जानने पर बल देते हैं। उनके अनुसार यथार्थ दृष्टि से आत्मार्थ और परार्थ में अविरोध है । आत्मार्थ और परार्थ में विरोध तो उसी स्थिति में दिखाई देता है जब हमारी दृष्टि राग, द्वेष तथा मोह से युक्त होती है । राग द्वष और मोह का प्रहाण होने पर उनमें कोई विरोध दिखाई ही नहीं देता । स्व और पर का विरोध तो राग और द्वेष में ही है। जहाँ राग-द्वेष नहीं है, वहाँ कौन अपना और कौन पराया ? जब मनुष्य राग-द्वेष से ऊपर उठ जाता है तब वहाँ न आत्मार्थ
१. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ६०९-६१०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org