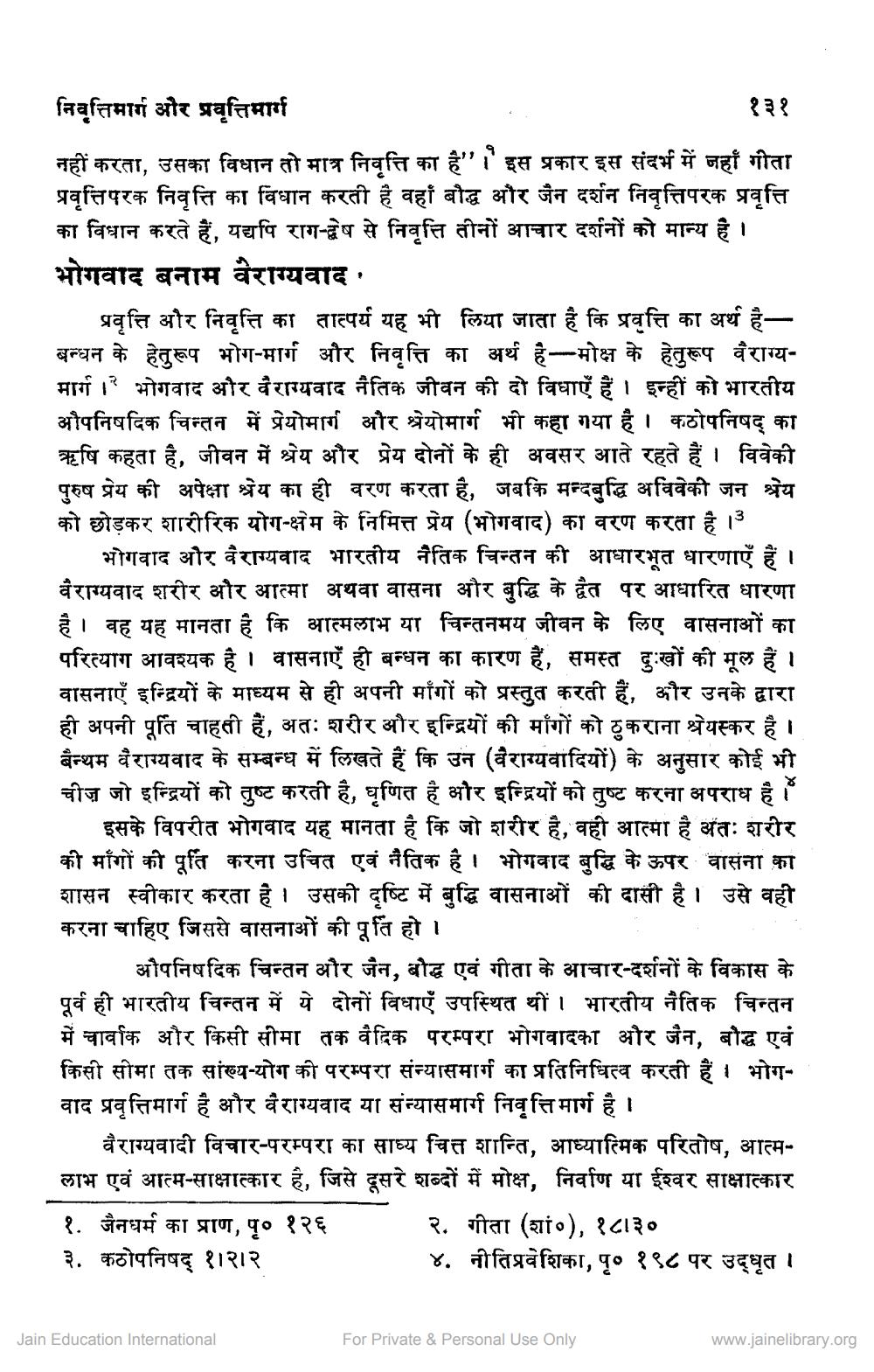________________
निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्तिमार्ग
१३१ नहीं करता, उसका विधान तो मात्र निवृत्ति का है"।' इस प्रकार इस संदर्भ में जहाँ गीता प्रवृत्तिपरक निवृत्ति का विधान करती है वहाँ बौद्ध और जैन दर्शन निवृत्तिपरक प्रवृत्ति का विधान करते हैं, यद्यपि राग-द्वेष से निवृत्ति तीनों आचार दर्शनों को मान्य है। भोगवाद बनाम वैराग्यवाद ।
प्रवृत्ति और निवृत्ति का तात्पर्य यह भी लिया जाता है कि प्रवृत्ति का अर्थ हैबन्धन के हेतुरूप भोग-मार्ग और निवृत्ति का अर्थ है-मोक्ष के हेतुरूप वैराग्यमार्ग ।२ भोगवाद और वैराग्यवाद नैतिक जीवन की दो विधाएँ हैं। इन्हीं को भारतीय औपनिषदिक चिन्तन में प्रेयोमार्ग और श्रेयोमार्ग भी कहा गया है । कठोपनिषद् का ऋषि कहता है, जीवन में श्रेय और प्रेय दोनों के ही अवसर आते रहते हैं । विवेकी पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वरण करता है, जबकि मन्दबुद्धि अविवेकी जन श्रेय को छोड़कर शारीरिक योग-क्षेम के निमित्त प्रेय (भोगवाद) का वरण करता है ।
भोगवाद और वैराग्यवाद भारतीय नैतिक चिन्तन की आधारभूत धारणाएँ हैं। वैराग्यवाद शरीर और आत्मा अथवा वासना और बुद्धि के द्वैत पर आधारित धारणा है। वह यह मानता है कि आत्मलाभ या चिन्तनमय जीवन के लिए वासनाओं का परित्याग आवश्यक है । वासनाएँ ही बन्धन का कारण हैं, समस्त दुःखों की मूल हैं । वासनाएँ इन्द्रियों के माध्यम से ही अपनी मांगों को प्रस्तुत करती हैं, और उनके द्वारा ही अपनी पूर्ति चाहती हैं, अतः शरीर और इन्द्रियों की मांगों को ठुकराना श्रेयस्कर है। बैन्थम वैराग्यवाद के सम्बन्ध में लिखते हैं कि उन (वैराग्यवादियों) के अनुसार कोई भी चीज़ जो इन्द्रियों को तुष्ट करती है, घृणित है और इन्द्रियों को तुष्ट करना अपराध है।
इसके विपरीत भोगवाद यह मानता है कि जो शरीर है, वही आत्मा है अतः शरीर की मांगों की पूर्ति करना उचित एवं नैतिक है। भोगवाद बुद्धि के ऊपर वासना का शासन स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में बुद्धि वासनाओं की दासी है। उसे वही करना चाहिए जिससे वासनाओं की पूर्ति हो ।
औपनिषदिक चिन्तन और जैन, बौद्ध एवं गीता के आचार-दर्शनों के विकास के पूर्व ही भारतीय चिन्तन में ये दोनों विधाएँ उपस्थित थीं। भारतीय नैतिक चिन्तन में चार्वाक और किसी सीमा तक वैदिक परम्परा भोगवादका और जैन, बौद्ध एवं किसी सीमा तक सांख्य-योग की परम्परा संन्यासमार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं । भोगवाद प्रवृत्तिमार्ग है और वैराग्यवाद या संन्यासमार्ग निवृत्ति मार्ग है ।
वैराग्यवादी विचार-परम्परा का साध्य चित्त शान्ति, आध्यात्मिक परितोष, आत्मलाभ एवं आत्म-साक्षात्कार है, जिसे दूसरे शब्दों में मोक्ष, निर्वाण या ईश्वर साक्षात्कार १. जैनधर्म का प्राण, पृ० १२६ २. गीता (शां०), १८३० ३. कठोपनिषद् १।२।२
__ ४. नीतिप्रवेशिका, पृ० १९८ पर उद्धृत ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org