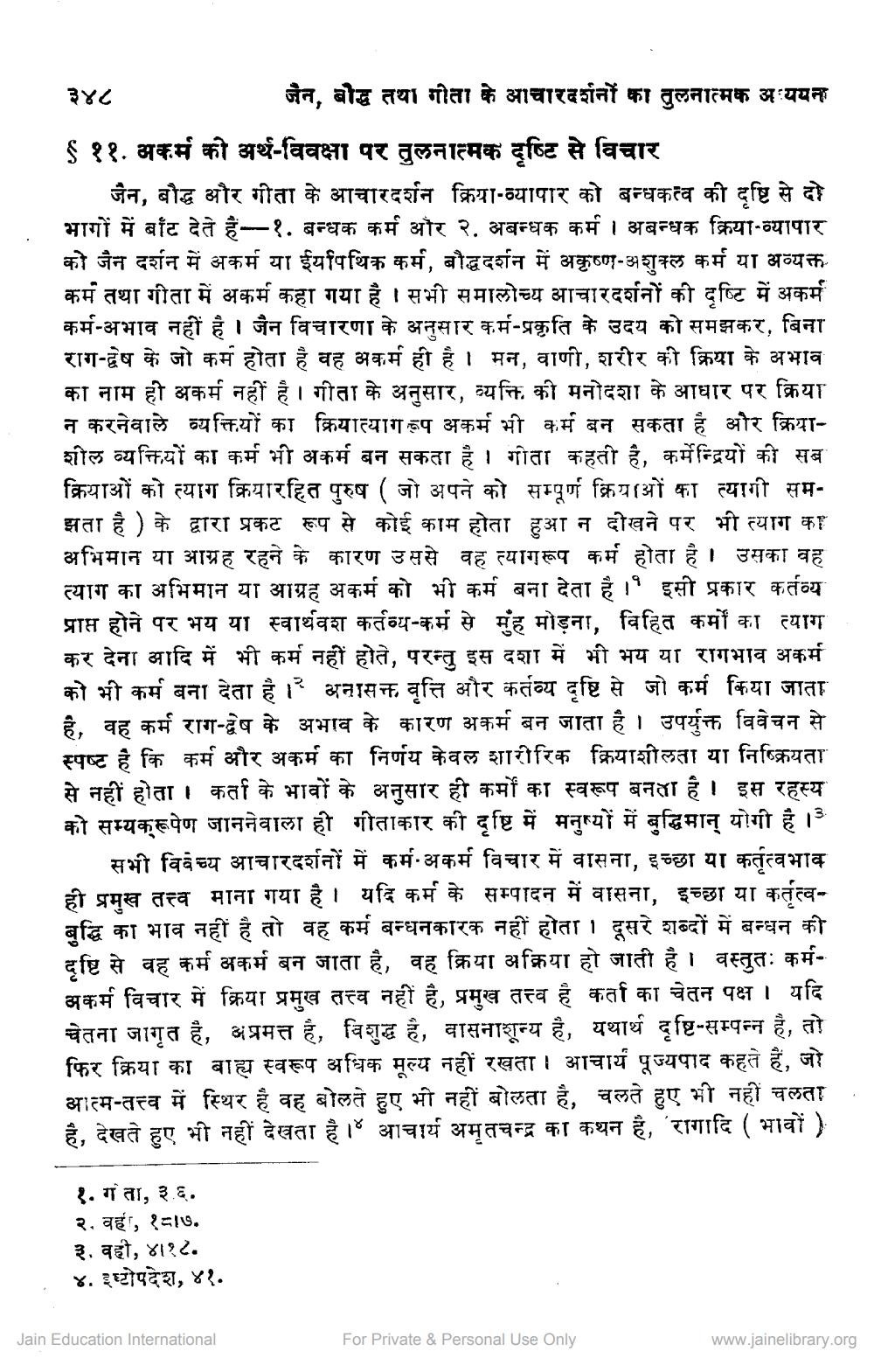________________
३४८
$ ११. अकर्म की अर्थ- विवक्षा पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार
जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन क्रिया - व्यापार को बन्धकत्व की दृष्टि से दो भागों में बाँट देते हैं - १. बन्धक कर्म और २. अबन्धक कर्म । अबन्धक क्रिया - व्यापार को जैन दर्शन में अकर्म या ईर्यापथिक कर्म, बौद्धदर्शन में अकृष्ण- अशुक्ल कर्म या अव्यक्तकर्म तथा गीता में अकर्म कहा गया है। सभी समालोच्य आचारदर्शनों की दृष्टि में अकर्म कर्म-अभाव नहीं है । जैन विचारणा के अनुसार कर्म प्रकृति के उदय को समझकर, बिना राग-द्वेष के जो कर्म होता है वह अकर्म ही है । मन, वाणी, शरीर की क्रिया के अभाव का नाम ही अकर्म नहीं है। गीता के अनुसार, व्यक्ति की मनोदशा के आधार पर क्रिया न करनेवाले व्यक्तियों का क्रियात्यागरूप अकर्म भी कर्म बन सकता है और क्रियाशील व्यक्तियों का कर्म भी अकर्म बन सकता है । गीता कहती है, कर्मेन्द्रियों की सब क्रियाओं को त्याग क्रियारहित पुरुष ( जो अपने को सम्पूर्ण क्रियाओं का त्यागी समझता है ) के द्वारा प्रकट रूप से कोई काम होता हुआ न दोखने पर भी त्याग का अभिमान या आग्रह रहने के कारण उससे वह त्यागरूप कर्म होता है । त्याग का अभिमान या आग्रह अकर्म को भी कर्म बना देता है । इसी प्रकार कर्तव्य प्राप्त होने पर भय या स्वार्थवश कर्तव्य कर्म से मुंह मोड़ना, विहित कर्मों का त्याग कर देना आदि में भी कर्म नहीं होते, परन्तु इस दशा में भी भय या रागभाव अकर्म को भी कर्म बना देता है । अनासक्त वृत्ति और कर्तव्य दृष्टि से जो कर्म किया जाता है, वह कर्म राग-द्वेष के अभाव के कारण अकर्म बन जाता है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म और अकर्म का निर्णय केवल शारीरिक क्रियाशीलता या निष्क्रियता से नहीं होता । कर्ता के भावों के अनुसार ही कर्मों का स्वरूप बनता है । इस रहस्य को सम्यक्रूपेण जाननेवाला ही गीताकार की दृष्टि में मनुष्यों बुद्धिमान् योगी है । सभी विवेच्य आचारदर्शनों में कर्म अकर्म विचार में वासना, इच्छा या कर्तृत्वभाव
उसका वह
ही प्रमुख तत्त्व माना गया है । यदि कर्म के सम्पादन में वासना, इच्छा या कर्तृत्वबुद्धि का भाव नहीं है तो वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता । दूसरे शब्दों में बन्धन की दृष्टि से वह कर्म अकर्म बन जाता है, वह क्रिया अक्रिया हो जाती है । वस्तुतः कर्म
अकर्म विचार में क्रिया प्रमुख तत्त्व नहीं है, प्रमुख तत्त्व है कर्ता का चेतन पक्ष । यदि चेतना जागृत है, अप्रमत्त है, विशुद्ध है, वासनाशून्य है, यथार्थ दृष्टि सम्पन्न है, तो फिर क्रिया का बाह्य स्वरूप अधिक मूल्य नहीं रखता। आचार्यं पूज्यपाद कहते हैं, जो आत्म-तत्त्व में स्थिर है वह बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। आचार्य अमृतचन्द्र का कथन है, 'रागादि ( भावों )
१. गंता, ३.६.
२. वह १८।७.
३. वही, ४।१८. ४. इष्टोपदेश, ४१.
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययना
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org