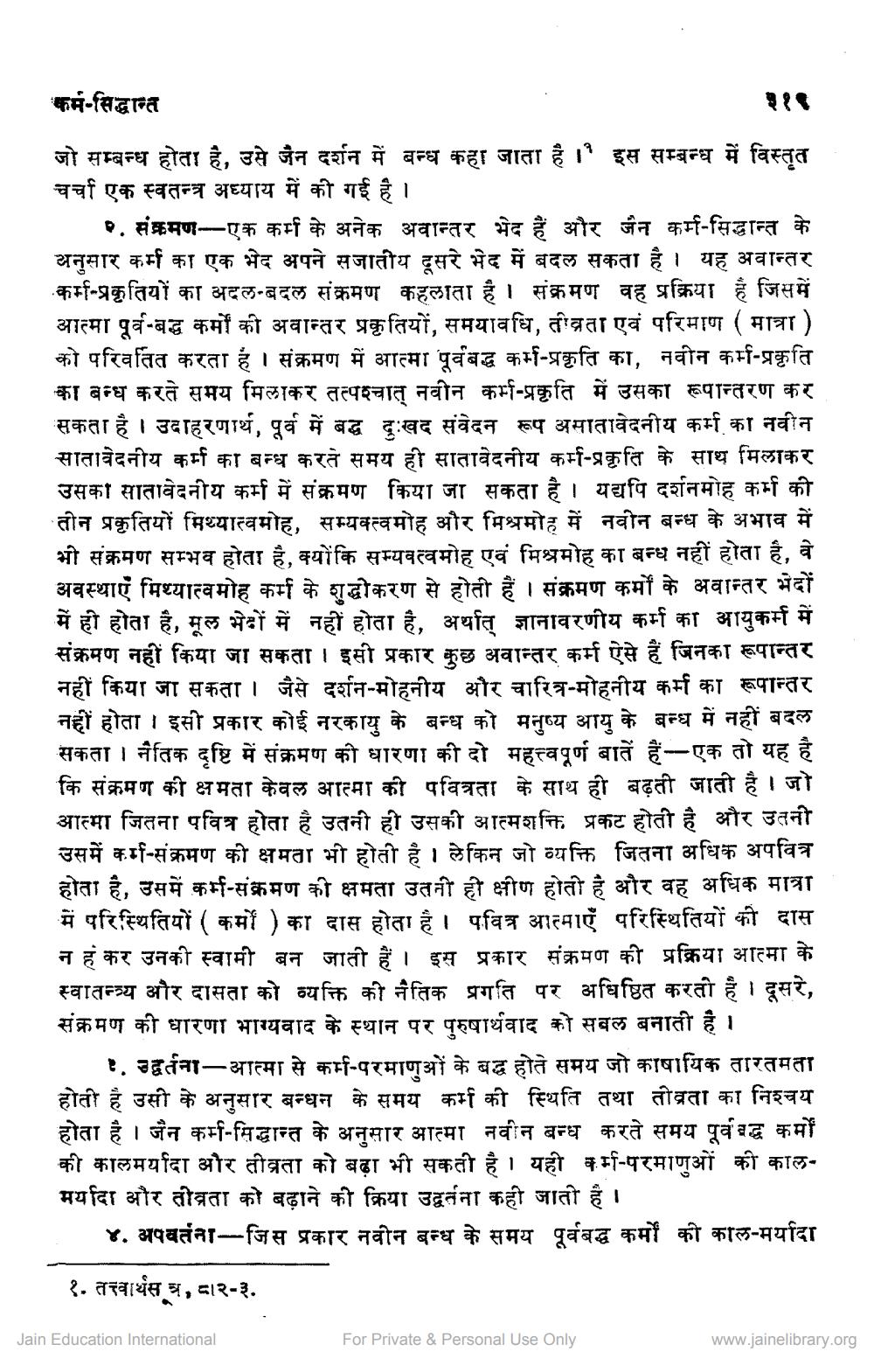________________
३१९
कर्म सिद्धान्त
जो सम्बन्ध होता है, उसे जैन दर्शन में बन्ध कहा जाता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा एक स्वतन्त्र अध्याय में की गई है ।
२. संक्रमण - एक कर्म के अनेक अवान्तर भेद हैं और जैन कर्म सिद्धान्त के अनुसार कर्म का एक भेद अपने सजातीय दूसरे भेद में बदल सकता है । यह अवान्तर कर्म प्रकृतियों का अदल-बदल संक्रमण कहलाता है । संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा पूर्व - बद्ध कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों, समयावधि, तीव्रता एवं परिमाण ( मात्रा ) को परिवर्तित करता है । संक्रमण में आत्मा पूर्वबद्ध कर्म प्रकृति का, नवीन कर्म-प्रकृति का बन्ध करते समय मिलाकर तत्पश्चात् नवीन कर्म-प्रकृति में उसका रूपान्तरण कर सकता है । उदाहरणार्थ, पूर्व में बद्ध दुःखद संवेदन रूप असातावेदनीय कर्म का नवीन सातावेदनीय कर्म का बन्ध करते समय ही सातावेदनीय कर्म-प्रकृति के साथ मिलाकर उसका सातावेदनीय कर्म में संक्रमण किया जा सकता है । यद्यपि दर्शनमोह कर्म की तीन प्रकृतियों मिथ्यात्वमोह, सम्यक्त्वमोह और मिश्रमोह में नवीन बन्ध के अभाव में भी संक्रमण सम्भव होता है, क्योंकि सम्यवत्वमोह एवं मिश्रमोह का बन्ध नहीं होता है, वे अवस्थाएं मिथ्यात्वमोह कर्म के शुद्धीकरण से होती हैं । संक्रमण कर्मों के अवान्तर भेदों में ही होता है, मूल भेदों में नहीं होता है, अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्म का आयुकर्म में संक्रमण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कुछ अवान्तर कर्म ऐसे हैं जिनका रूपान्तर नहीं किया जा सकता । जैसे दर्शन - मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का रूपान्तर नहीं होता । इसी प्रकार कोई नरकायु के बन्ध को मनुष्य आयु के बन्ध में नहीं बदल सकता । नैतिक दृष्टि में संक्रमण की धारणा की दो महत्त्वपूर्ण बातें हैं - एक तो यह है कि संक्रमण की क्षमता केवल आत्मा की पवित्रता के साथ ही बढ़ती जाती है । जो आत्मा जितना पवित्र होता है उतनी ही उसकी आत्मशक्ति प्रकट होती है और उतनी उसमें कर्म संक्रमण की क्षमता भी होती है । लेकिन जो व्यक्ति जितना अधिक अपवित्र होता है, उसमें कर्म संक्रमण की क्षमता उतनी ही क्षीण होती है और वह अधिक मात्रा में परिस्थितियों ( कर्मों ) का दास होता है । पवित्र आत्माएँ परिस्थितियों की दास न हं कर उनकी स्वामी बन जाती । इस प्रकार संक्रमण की प्रक्रिया आत्मा के स्वातन्त्र्य और दासता को व्यक्ति की नैतिक प्रगति पर अधिष्ठित करती है । दूसरे, संक्रमण की धारणा भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद को सबल बनाती है ।
2. उद्वर्तना-आत्मा से कर्म-परमाणुओं के बद्ध होते समय जो काषायिक तारतमता होती है उसी के अनुसार बन्धन के समय कर्म की स्थिति तथा तीव्रता का निश्चय होता है । जैन कर्म- सिद्धान्त के अनुसार आत्मा नवीन बन्ध करते समय पूर्वबद्ध कर्मों की कालमर्यादा और तीव्रता को बढ़ा भी सकती है । यही कर्म-परमाणुओं की कालमर्यादा और तीव्रता को बढ़ाने की क्रिया उद्वर्तना कही जाती हैं ।
४. अपवर्तना-जिस प्रकार नवीन बन्ध के समय पूर्वबद्ध कर्मों की काल मर्यादा
-
१. तत्त्वार्थसत्र, ८२-३.
•
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org