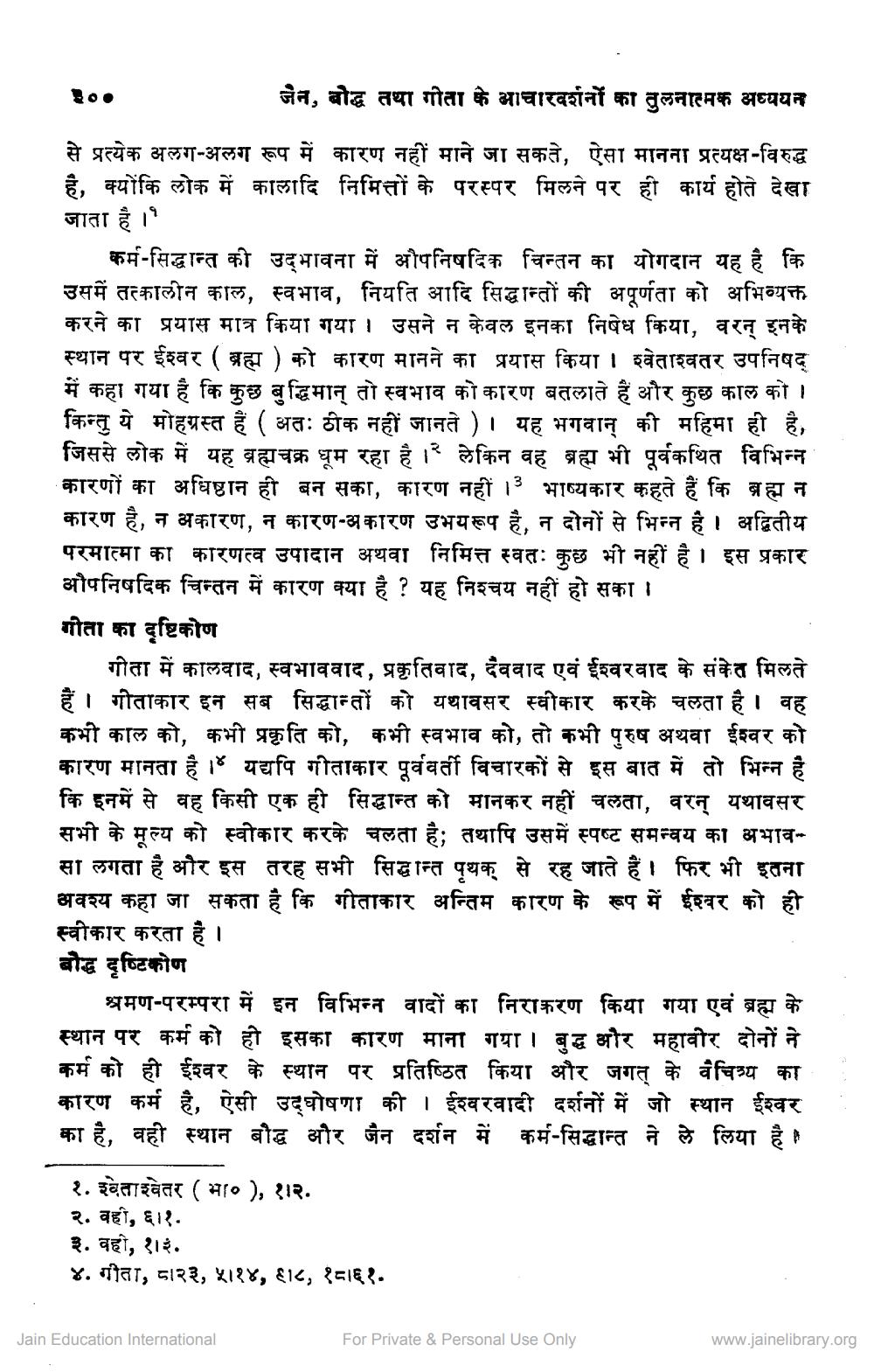________________
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारवर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
से प्रत्येक अलग-अलग रूप में कारण नहीं माने जा सकते, ऐसा मानना प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, क्योंकि लोक में कालादि निमित्तों के परस्पर मिलने पर ही कार्य होते देखा जाता है ।
कर्म-सिद्धान्त की उद्भावना में औपनिषदिक चिन्तन का योगदान यह है कि उसमें तत्कालीन काल, स्वभाव, नियति आदि सिद्धान्तों की अपूर्णता को अभिव्यक्त करने का प्रयास मात्र किया गया। उसने न केवल इनका निषेध किया, वरन् इनके स्थान पर ईश्वर ( ब्रह्म ) को कारण मानने का प्रयास किया । श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है कि कुछ बुद्धिमान् तो स्वभाव को कारण बतलाते हैं और कुछ काल को । किन्तु ये मोहग्रस्त हैं ( अतः ठीक नहीं जानते )। यह भगवान् की महिमा ही है, जिससे लोक में यह ब्रह्मचक्र धूम रहा है । लेकिन वह ब्रह्म भी पूर्वकथित विभिन्न कारणों का अधिष्ठान ही बन सका, कारण नहीं ।3 भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म न कारण है, न अकारण, न कारण-अकारण उभयरूप है, न दोनों से भिन्न है। अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व उपादान अथवा निमित्त स्वतः कुछ भी नहीं है। इस प्रकार औपनिषदिक चिन्तन में कारण क्या है ? यह निश्चय नहीं हो सका। गीता का दृष्टिकोण
गीता में कालवाद, स्वभाववाद, प्रकृतिवाद, दैववाद एवं ईश्वरवाद के संकेत मिलते हैं। गीताकार इन सब सिद्धान्तों को यथावसर स्वीकार करके चलता है। वह कभी काल को, कभी प्रकृति को, कभी स्वभाव को, तो कभी पुरुष अथवा ईश्वर को कारण मानता है। यद्यपि गीताकार पूर्ववर्ती विचारकों से इस बात में तो भिन्न है कि इनमें से वह किसी एक ही सिद्धान्त को मानकर नहीं चलता, वरन् यथावसर सभी के मूल्य को स्वीकार करके चलता है; तथापि उसमें स्पष्ट समन्वय का अभावसा लगता है और इस तरह सभी सिद्धान्त पृथक् से रह जाते हैं। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गीताकार अन्तिम कारण के रूप में ईश्वर को ही स्वीकार करता है। बौद्ध दृष्टिकोण
__ श्रमण-परम्परा में इन विभिन्न वादों का निराकरण किया गया एवं ब्रह्म के स्थान पर कर्म को ही इसका कारण माना गया। बुद्ध और महावीर दोनों ने कर्म को ही ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किया और जगत् के वैचित्र्य का कारण कर्म है, ऐसी उद्घोषणा की । ईश्वरवादी दर्शनों में जो स्थान ईश्वर का है, वही स्थान बौद्ध और जैन दर्शन में कर्म-सिद्धान्त ने ले लिया है।
१. श्वेताश्वेतर ( भा०), १२. २. वही, ६।१. ३. वही, १॥३. ४. गीता, ८२३, ५।१४, ६८, १८६१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org