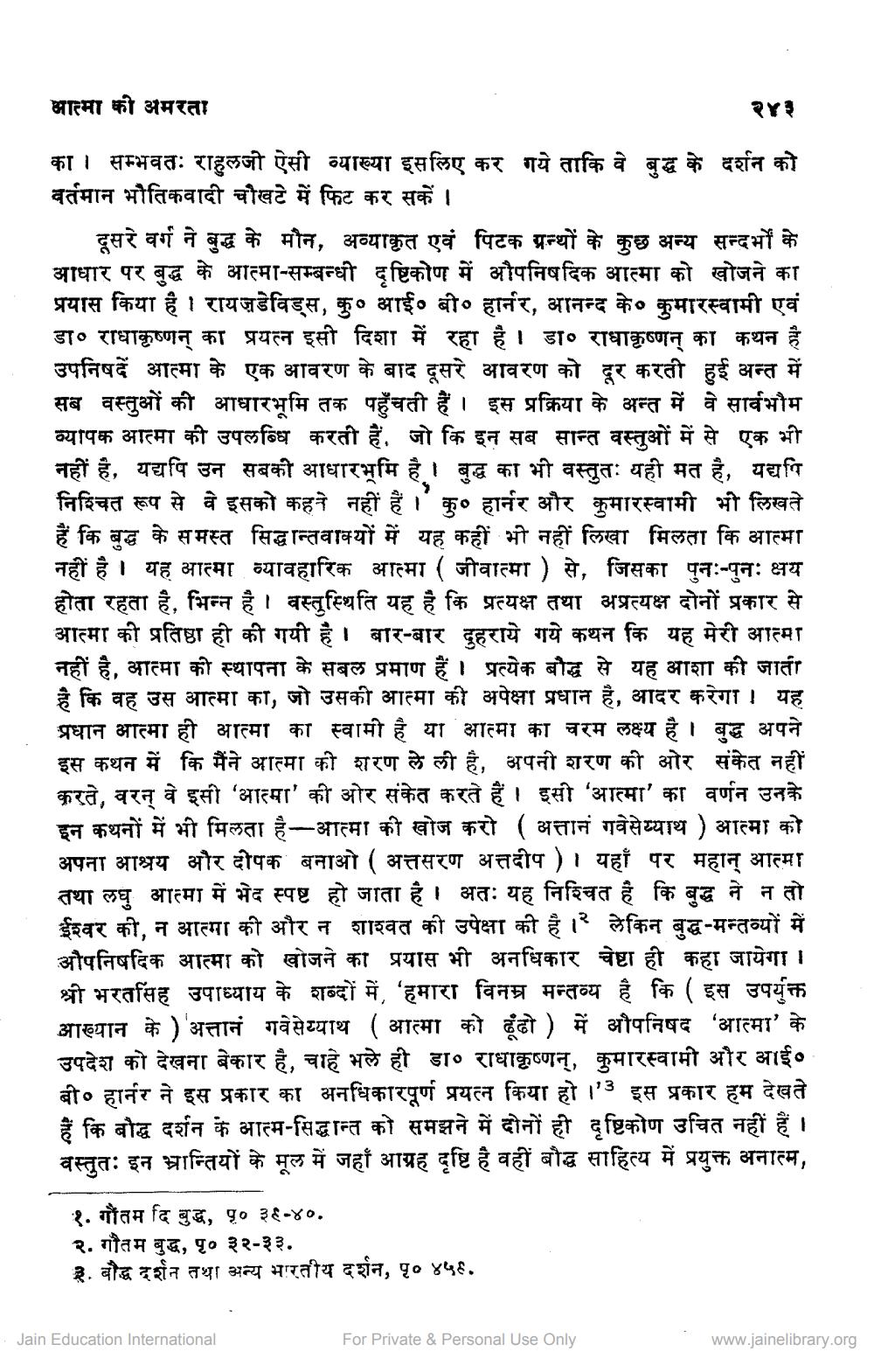________________
आत्मा की अमरता
का। सम्भवतः राहुलजी ऐसी व्याख्या इसलिए कर गये ताकि वे बुद्ध के दर्शन को वर्तमान भौतिकवादी चौखटे में फिट कर सकें।
दूसरे वर्ग ने बुद्ध के मौन, अव्याकृत एवं पिटक ग्रन्थों के कुछ अन्य सन्दर्भो के आधार पर बुद्ध के आत्मा-सम्बन्धी दृष्टिकोण में औपनिषदिक आत्मा को खोजने का प्रयास किया है । रायज़डेविड्स, कु० आई० बी० हार्नर, आनन्द के० कुमारस्वामी एवं डा० राधाकृष्णन् का प्रयत्न इसी दिशा में रहा है। डा० राधाकृष्णन् का कथन है उपनिषदें आत्मा के एक आवरण के बाद दूसरे आवरण को दूर करती हुई अन्त में सब वस्तुओं की आधारभूमि तक पहुँचती हैं। इस प्रक्रिया के अन्त में वे सार्वभौम व्यापक आत्मा की उपलब्धि करती हैं. जो कि इन सब सान्त वस्तुओं में से एक भी नहीं है, यद्यपि उन सबकी आधारभूमि है। बुद्ध का भी वस्तुतः यही मत है, यद्यपि निश्चित रूप से वे इसको कहते नहीं हैं। कुछ हार्नर और कुमारस्वामी भी लिखते हैं कि बुद्ध के समस्त सिद्धान्तवाक्यों में यह कहीं भी नहीं लिखा मिलता कि आत्मा नहीं है । यह आत्मा व्यावहारिक आत्मा ( जीवात्मा ) से, जिसका पुनः-पुनः क्षय होता रहता है, भिन्न है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से आत्मा की प्रतिष्ठा ही की गयी है। बार-बार दुहराये गये कथन कि यह मेरी आत्मा नहीं है, आत्मा की स्थापना के सबल प्रमाण हैं। प्रत्येक बौद्ध से यह आशा की जाती है कि वह उस आत्मा का, जो उसकी आत्मा की अपेक्षा प्रधान है, आदर करेगा। यह प्रधान आत्मा ही आत्मा का स्वामी है या आत्मा का चरम लक्ष्य है। बुद्ध अपने इस कथन में कि मैंने आत्मा की शरण ले ली है, अपनी शरण की ओर संकेत नहीं करते, वरन् वे इसी 'आत्मा' की ओर संकेत करते हैं। इसी 'आत्मा' का वर्णन उनके इन कथनों में भी मिलता है-आत्मा की खोज करो ( अत्तानं गवेसेय्याथ ) आत्मा को अपना आश्रय और दीपक बनाओ ( अत्तसरण अत्तदीप)। यहाँ पर महान् आत्मा तथा लघु आत्मा में भेद स्पष्ट हो जाता है। अतः यह निश्चित है कि बुद्ध ने न तो ईश्वर की, न आत्मा की और न शाश्वत की उपेक्षा की है । लेकिन बुद्ध-मन्तव्यों में औपनिषदिक आत्मा को खोजने का प्रयास भी अनधिकार चेष्टा ही कहा जायेगा। श्री भरतसिंह उपाध्याय के शब्दों में, 'हमारा विनम्र मन्तव्य है कि ( इस उपर्युक्त आख्यान के ) अत्तानं गवेसेय्याथ ( आत्मा को ढूंढो ) में औपनिषद 'आत्मा' के उपदेश को देखना बेकार है, चाहे भले ही डा० राधाकृष्णन्, कुमारस्वामी और आई० बी० हार्नर ने इस प्रकार का अनधिकारपूर्ण प्रयत्न किया हो ।'3 इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन के आत्म-सिद्धान्त को समझने में दोनों ही दृष्टिकोण उचित नहीं हैं । वस्तुतः इन भ्रान्तियों के मूल में जहाँ आग्रह दृष्टि है वहीं बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त अनात्म,
१. गौतम दि बुद्ध, पृ० ३६-४०. २. गौतम बुद्ध, पृ० ३२-३३. ३. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ४५६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org