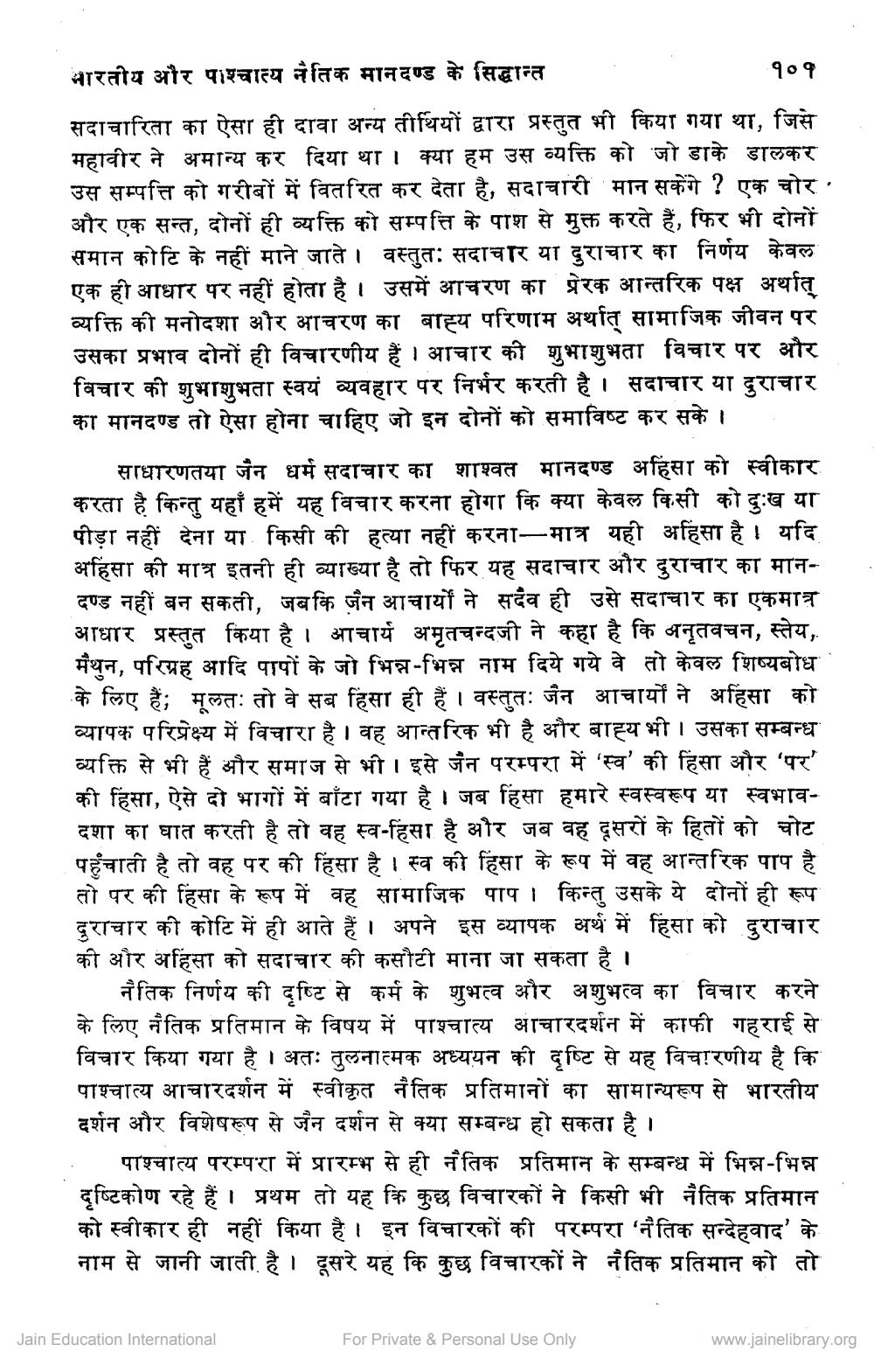________________
भारतीय और पाश्चात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त
१०१
सदाचारिता का ऐसा ही दावा अन्य तीर्थियों द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था, जिसे महावीर ने अमान्य कर दिया था | क्या हम उस व्यक्ति को जो डाके डालकर उस सम्पत्ति को गरीबों में वितरित कर देता है, सदाचारी मान सकेंगे ? एक चोर और एक सन्त, दोनों ही व्यक्ति को सम्पत्ति के पाश से मुक्त करते हैं, फिर भी दोनों समान कोटि के नहीं माने जाते । वस्तुतः सदाचार या दुराचार का निर्णय केवल एक ही आधार पर नहीं होता है । उसमें आचरण का प्रेरक आन्तरिक पक्ष अर्थात् व्यक्ति की मनोदशा और आचरण का बाह्य परिणाम अर्थात् सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव दोनों ही विचारणीय हैं । आचार की शुभाशुभता विचार पर और विचार की शुभाशुभता स्वयं व्यवहार पर निर्भर करती है । सदाचार या दुराचार का मानदण्ड तो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को समाविष्ट कर सके ।
साधारणतया जैन धर्म सदाचार का शाश्वत मानदण्ड अहिंसा को स्वीकार करता है किन्तु यहाँ हमें यह विचार करना होगा कि क्या केवल किसी को दुःख या पीड़ा नहीं देना या किसी की हत्या नहीं करना - मात्र यही अहिंसा है । यदि अहिंसा की मात्र इतनी ही व्याख्या है तो फिर यह सदाचार और दुराचार का मानदण्ड नहीं बन सकती, जबकि जैन आचार्यों ने सदैव ही उसे सदाचार का एकमात्र आधार प्रस्तुत किया है । आचार्य अमृतचन्दजी ने कहा है कि अनृतवचन, स्तेय, मैथुन, परिग्रह आदि पापों के जो भिन्न-भिन्न नाम दिये गये वे तो केवल शिष्यबोध के लिए हैं; मूलतः तो वे सब हिंसा ही हैं । वस्तुतः जैन आचार्यों ने अहिंसा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचारा है । वह आन्तरिक भी है और बाह्य भी । उसका सम्बन्ध व्यक्ति से भी हैं और समाज से भी । इसे जैन परम्परा में 'स्व' की हिंसा और 'पर' की हिंसा, ऐसे दो भागों में बाँटा गया है । जब हिंसा हमारे स्वस्वरूप या स्वभावदशा का घात करती है तो वह स्व-हिंसा है और जब वह दूसरों के हितों को चोट पहुंचाती है तो वह पर की हिंसा है । स्व की हिंसा के रूप में वह आन्तरिक पाप है तो पर की हिंसा के रूप में वह सामाजिक पाप । किन्तु उसके ये दोनों ही रूप दुराचार की कोटि में ही आते हैं । अपने इस व्यापक अर्थ में हिंसा को दुराचार की और अहिंसा को सदाचार की कसौटी माना जा सकता है ।
नैतिक निर्णय की दृष्टि से कर्म के शुभत्व और अशुभत्व का विचार करने के लिए नैतिक प्रतिमान के विषय में पाश्चात्य आचारदर्शन में काफी गहराई से विचार किया गया है । अतः तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह विचारणीय है कि पाश्चात्य आचारदर्शन में स्वीकृत नैतिक प्रतिमानों का सामान्यरूप से भारतीय दर्शन और विशेषरूप से जैन दर्शन से क्या सम्बन्ध हो सकता है ।
पाश्चात्य परम्परा में प्रारम्भ से ही नैतिक प्रतिमान के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं । प्रथम तो यह कि कुछ विचारकों ने किसी भी नैतिक प्रतिमान को स्वीकार ही नहीं किया है । इन विचारकों की परम्परा 'नैतिक सन्देहवाद' के नाम से जानी जाती है । दूसरे यह कि कुछ विचारकों ने नैतिक प्रतिमान को तो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
+
www.jainelibrary.org