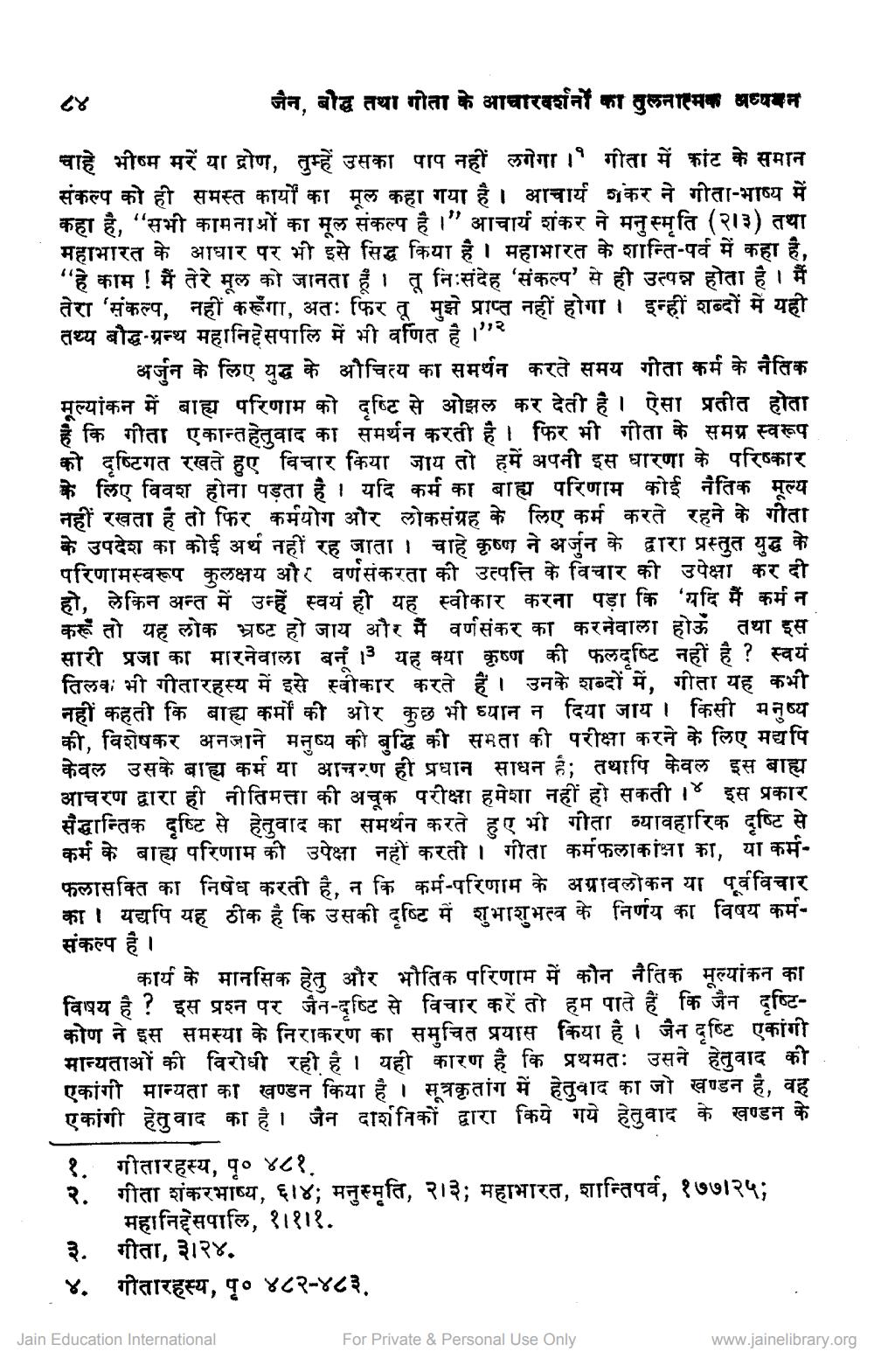________________
जैन, बौद्ध तथा गोता के आचारवर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
चाहे भीष्म मरें या द्रोण, तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा।' गीता में कांट के समान संकल्प को ही समस्त कार्यों का मूल कहा गया है। आचार्य शंकर ने गीता-भाष्य में कहा है, "सभी कामनाओं का मूल संकल्प है।" आचार्य शंकर ने मनुस्मृति (२।३) तथा महाभारत के आधार पर भी इसे सिद्ध किया है। महाभारत के शान्ति-पर्व में कहा है, "हे काम ! मैं तेरे मूल को जानता है। तू निःसंदेह 'संकल्प' से ही उत्पन्न होता है । मैं तेरा 'संकल्प, नहीं करूंगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। इन्हीं शब्दों में यही तथ्य बौद्ध-ग्रन्थ महानिहेसपालि में भी वर्णित है ।"
अर्जुन के लिए युद्ध के औचित्य का समर्थन करते समय गीता कर्म के नैतिक मूल्यांकन में बाह्य परिणाम को दृष्टि से ओझल कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गीता एकान्त हेतुवाद का समर्थन करती है। फिर भी गीता के समग्र स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाय तो हमें अपनी इस धारणा के परिष्कार के लिए विवश होना पड़ता है। यदि कर्म का बाह्य परिणाम कोई नैतिक मूल्य नहीं रखता है तो फिर कर्मयोग और लोकसंग्रह के लिए कर्म करते रहने के गीता के उपदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चाहे कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत युद्ध के परिणामस्वरूप कुलक्षय और वर्णसंकरता की उत्पत्ति के विचार की उपेक्षा कर दी हो, लेकिन अन्त में उन्हें स्वयं ही यह स्वीकार करना पड़ा कि 'यदि मैं कर्म न करूं तो यह लोक भ्रष्ट हो जाय और मैं वर्णसंकर का करनेवाला होऊँ तथा इस सारी प्रजा का मारनेवाला बनं । यह क्या कृष्ण की फलदृष्टि नहीं है ? स्वयं तिलक भी गीतारहस्य में इसे स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में, गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कर्मों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया जाय । किसी मनुष्य की, विशेषकर अनजाने मनुष्य की बुद्धि की समता की परीक्षा करने के लिए मद्यपि केवल उसके बाह्य कर्म या आचरण ही प्रधान साधन है; तथापि केवल इस बाह्य आचरण द्वारा ही नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हमेशा नहीं हो सकती।४ इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से हेतुवाद का समर्थन करते हुए भी गीता व्यावहारिक दृष्टि से कर्म के बाह्य परिणाम की उपेक्षा नहीं करती। गीता कर्मफलाकांक्षा का, या कर्मफलासक्ति का निषेध करती है, न कि कर्म-परिणाम के अग्रावलोकन या पूर्वविचार का। यद्यपि यह ठीक है कि उसकी दृष्टि में शुभाशुभत्व के निर्णय का विषय कर्मसंकल्प है।
__ कार्य के मानसिक हेतु और भौतिक परिणाम में कौन नैतिक मूल्यांकन का विषय है ? इस प्रश्न पर जैन-दृष्टि से विचार करें तो हम पाते हैं कि जैन दृष्टिकोण ने इस समस्या के निराकरण का समुचित प्रयास किया है । जैन दृष्टि एकांगी मान्यताओं की विरोधी रही है । यही कारण है कि प्रथमतः उसने हेतुवाद की एकांगी मान्यता का खण्डन किया है। सूत्रकृतांग में हेतुवाद का जो खण्डन है, वह एकांगी हेतुवाद का है। जैन दार्शनिकों द्वारा किये गये हेतुवाद के खण्डन के १. गीतारहस्य, पृ० ४८१. २. गीता शंकरभाष्य, ६।४; मनुस्मृति, २।३; महाभारत, शान्तिपर्व, १७७।२५;
महानिर्देसपालि, १११११. ३. गीता, ३।२४. ४. गीतारहस्य, पृ० ४८२-४८३.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org