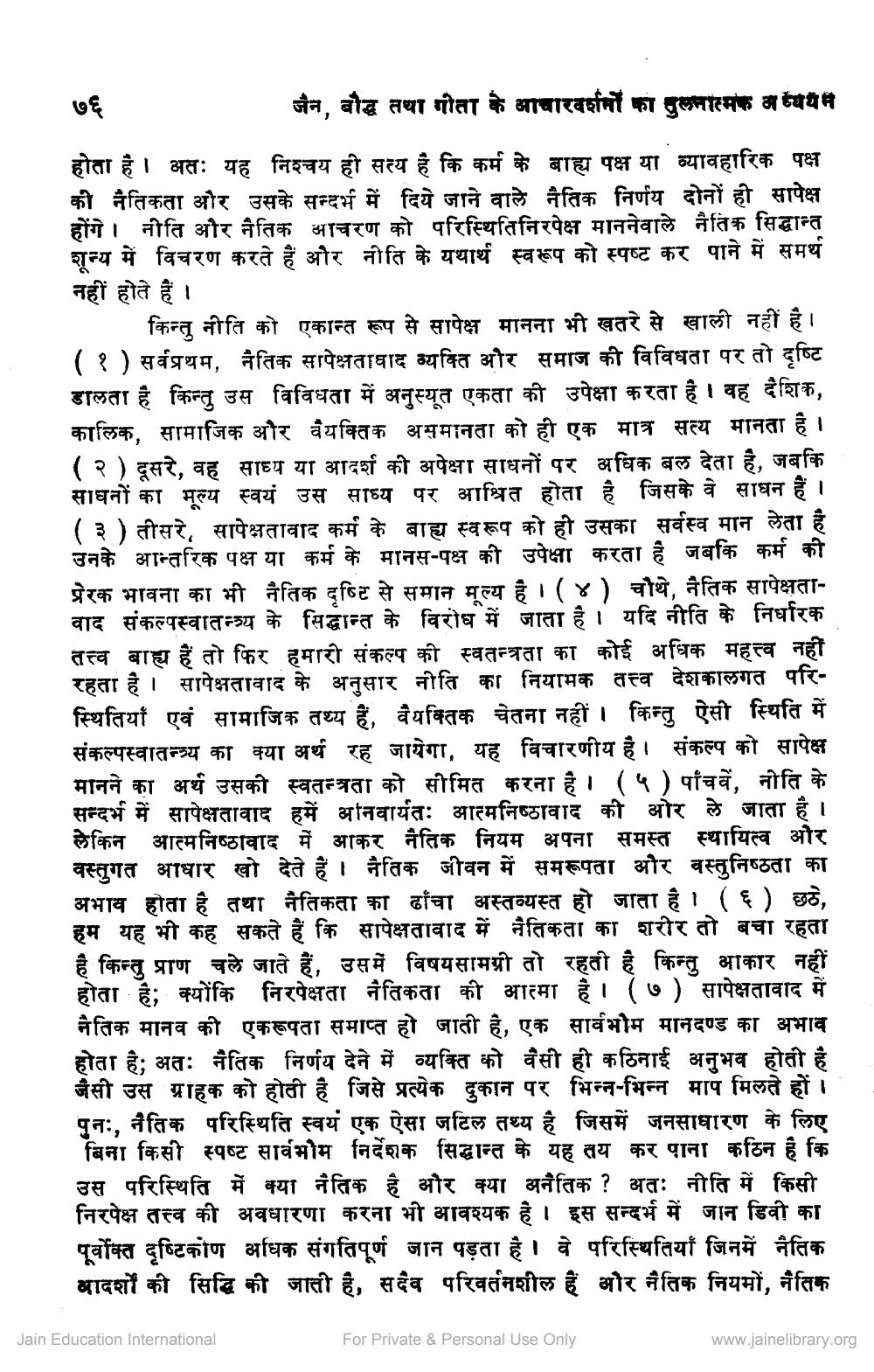________________
७६
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारवर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
होता है। अतः यह निश्चय ही सत्य है कि कर्म के बाह्य पक्ष या व्यावहारिक पक्ष की नैतिकता और उसके सन्दर्भ में दिये जाने वाले नैतिक निर्णय दोनों ही सापेक्ष होंगे। नीति और नैतिक आचरण को परिस्थितिनिरपेक्ष माननेवाले नैतिक सिद्धान्त शून्य में विचरण करते हैं और नीति के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं।
किन्तु नीति को एकान्त रूप से सापेक्ष मानना भी खतरे से खाली नहीं है। (१) सर्वप्रथम, नैतिक सापेक्षताघाद व्यक्ति और समाज की विविधता पर तो दृष्टि डालता है किन्तु उस विविधता में अनुस्यूत एकता की उपेक्षा करता है । वह दैशिक, कालिक, सामाजिक और वैयक्तिक असमानता को ही एक मात्र सत्य मानता है । (२) दूसरे, वह साध्य या आदर्श की अपेक्षा साधनों पर अधिक बल देता है, जबकि साधनों का मूल्य स्वयं उस साध्य पर आश्रित होता है जिसके वे साधन हैं । ( ३ ) तीसरे, सापेक्षतावाद कर्म के बाह्य स्वरूप को ही उसका सर्वस्व मान लेता है उनके आन्तरिक पक्ष या कर्म के मानस-पक्ष की उपेक्षा करता है जबकि कर्म की प्रेरक भावना का भी नैतिक दृष्टि से समान मूल्य है । ( ४ ) चौथे, नैतिक सापेक्षतावाद संकल्पस्वातन्त्र्य के सिद्धान्त के विरोध में जाता है। यदि नीति के निर्धारक तत्त्व बाह्य हैं तो फिर हमारी संकल्प की स्वतन्त्रता का कोई अधिक महत्त्व नहीं रहता है। सापेक्षतावाद के अनुसार नीति का नियामक तत्त्व देशकालगत परिस्थितियाँ एवं सामाजिक तथ्य हैं, वैयक्तिक चेतना नहीं। किन्तु ऐसी स्थिति में संकल्पस्वातन्त्र्य का क्या अर्थ रह जायेगा, यह विचारणीय है। संकल्प को सापेक्ष मानने का अर्थ उसकी स्वतन्त्रता को सीमित करना है। (५ ) पांचवें, नीति के सन्दर्भ में सापेक्षतावाद हमें अनिवार्यतः आत्मनिष्ठावाद की ओर ले जाता है । लेकिन आत्मनिष्ठावाद में आकर नैतिक नियम अपना समस्त स्थायित्व और वस्तुगत आधार खो देते हैं । नैतिक जीवन में समरूपता और वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है तथा नैतिकता का ढाँचा अस्तव्यस्त हो जाता है। (६) छठे, हम भी कह सकते हैं कि सापेक्षतावाद में नैतिकता का शरीर तो बचा रहता है किन्तु प्राण चले जाते हैं, उसमें विषयसामग्री तो रहती है किन्तु आकार नहीं होता है; क्योंकि निरपेक्षता नैतिकता की आत्मा है। (७) सापेक्षतावाद में नैतिक मानव की एकरूपता समाप्त हो जाती है, एक सार्वभौम मानदण्ड का अभाव होता है; अतः नैतिक निर्णय देने में व्यक्ति को वैसी ही कठिनाई अनुभव होती है जैसी उस ग्राहक को होती है जिसे प्रत्येक दुकान पर भिन्न-भिन्न माप मिलते हों। पुनः, नैतिक परिस्थिति स्वयं एक ऐसा जटिल तथ्य है जिसमें जनसाधारण के लिए बिना किसी स्पष्ट सार्वभौम निर्देशक सिद्धान्त के यह तय कर पाना कठिन है कि उस परिस्थिति में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक ? अतः नीति में किसी निरपेक्ष तत्त्व की अवधारणा करना भी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में जान डिवी का पूर्वोक्त दृष्टिकोण अधिक संगतिपूर्ण जान पड़ता है। वे परिस्थितियाँ जिनमें नैतिक भादों की सिद्धि की जाती है, सदैव परिवर्तनशील हैं और नैतिक नियमों, नैतिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org