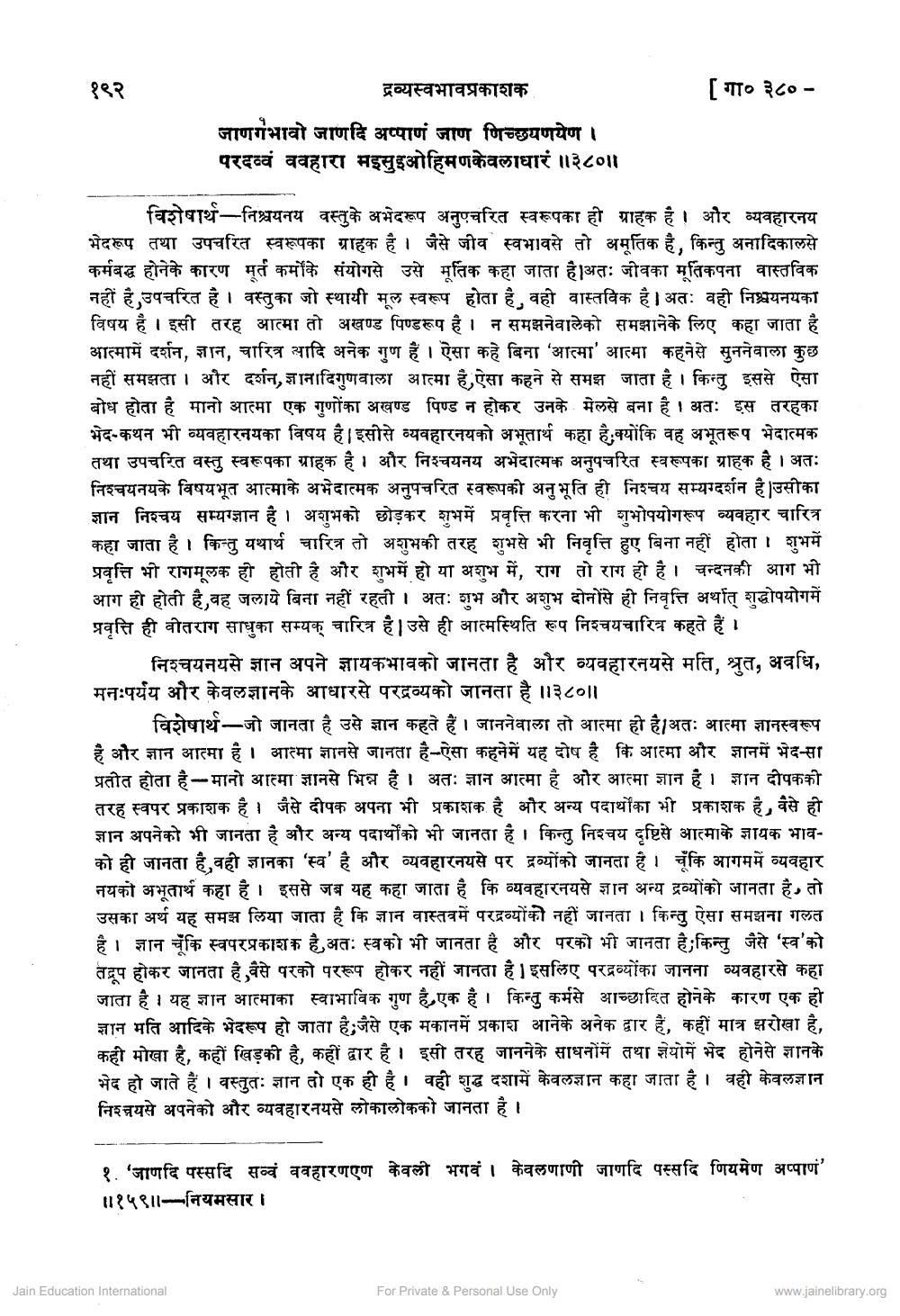________________
१९२
द्रव्यस्वभावप्रकाशक
[गा० ३८०
जाणगंभावो जाणदि अप्पाणं जाण णिच्छयणयेण । परदव्वं ववहारा मइसुइओहिमणकेवलाधारं ॥३८०॥
विशेषार्थ-निश्चयनय वस्तुके अभेदरूप अनुएचरित स्वरूपका ही ग्राहक है । और व्यवहारनय भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक है। जैसे जीव स्वभावसे तो अमूर्तिक है, किन्तु अनादिकालसे कर्मबद्ध होनेके कारण मूर्त कर्मोंके संयोगसे उसे मूर्तिक कहा जाता है।अतः जीवका मूर्तिकपना वास्तविक नहीं है उपचरित है। वस्तुका जो स्थायी मूल स्वरूप होता है, वही वास्तविक है। अतः वही निश्चयनयका विषय है । इसी तरह आत्मा तो अखण्ड पिण्डरूप है। न समझनेवालेको समझानेके लिए कहा जाता है आत्मामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण हैं । ऐसा कहे बिना 'आत्मा' आत्मा कहने से सूननेवाला कुछ नहीं समझता। और दर्शन, ज्ञानादिगुणवाला आत्मा है,ऐसा कहने से समझ जाता है। किन्तु इससे ऐसा बोध होता है मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे बना है। अतः इस तरहका भेद-कथन भी व्यवहारनयका विषय है। इसीसे व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है क्योंकि वह अभूतरूप भेदात्मक तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक है। और निश्चयनय अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक है । अतः निश्चयनयके विषयभूत आत्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपको अनुभूति ही निश्चय सम्यग्दर्शन है उसीका ज्ञान निश्चय सम्यग्ज्ञान है। अशुभको छोड़कर शुभमें प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र कहा जाता है। किन्तु यथार्थ चारित्र तो अशुभकी तरह शुभसे भी निवृत्ति हुए बिना नहीं होता। शुभमें प्रवृत्ति भी रागमूलक ही होती है और शुभमें हो या अशुभ में, राग तो राग ही है। चन्दनकी आग भी आग ही होती है,वह जलाये बिना नहीं रहती। अतः शुभ और अशुभ दोनोंसे ही निवृत्ति अर्थात् शुद्धोपयोगमें प्रवृत्ति ही वीतराग साधुका सम्यक् चारित्र है। उसे ही आत्मस्थिति रूप निश्चयचारित्र कहते हैं ।
निश्चयनयसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है और व्यवहारनयसे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानके आधारसे परद्रव्यको जानता है ।।३८०।।
विशेषार्थ-जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । जाननेवाला तो आत्मा ही है। अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान आत्मा है । आत्मा ज्ञानसे जानता है-ऐसा कहने में यह दोष है कि आत्मा और ज्ञानमें भेद-सा प्रतीत होता है-मानो आत्मा ज्ञानसे भिन्न है। अतः ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है। ज्ञान दीपककी तरह स्वपर प्रकाशक है। जैसे दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य पदार्थों का भी प्रकाशक है, वैसे ही ज्ञान अपनेको भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। किन्तु निश्चय दृष्टिसे आत्माके ज्ञायक भावको ही जानता है,वही ज्ञानका 'स्व' है और व्यवहारनयसे पर द्रव्योंको जानता है। चूंकि आगममें व्यवहार नयको अभूतार्थ कहा है। इससे जब यह कहा जाता है कि व्यवहारनयसे ज्ञान अन्य द्रव्योंको जानता है, तो उसका अर्थ यह समझ लिया जाता है कि ज्ञान वास्तवमें परद्रव्योंको नहीं जानता। किन्तु ऐसा समझना गलत है। ज्ञान चूंकि स्वपरप्रकाशक है, अतः स्वको भी जानता है और परको भी जानता है किन्तु जैसे 'स्व'को तद्रूप होकर जानता है वैसे परको पररूप होकर नहीं जानता है । इसलिए परद्रव्योंका जानना व्यवहारसे कहा जाता है। यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है,एक है। किन्तु कर्मसे आच्छादित होनेके कारण एक ही ज्ञान मति आदिके भेदरूप हो जाता है जैसे एक मकान में प्रकाश आनेके अनेक द्वार है, कहीं मात्र झरोखा है, कही मोखा है, कहीं खिड़की है, कहीं द्वार है। इसी तरह जाननेके साधनोंमें तथा ज्ञेयोमें भेद होनेसे ज्ञानके भेद हो जाते हैं । वस्तुतः ज्ञान तो एक ही है। वही शुद्ध दशामें केवलज्ञान कहा जाता है। वही केवलज्ञान निश्चयसे अपनेको और व्यवहारनयसे लोकालोकको जानता है।
१. 'जाणदि पस्सदि सव्वं ववहारणएण केवली भगवं। केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं' ॥१५९॥-नियमसार ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org