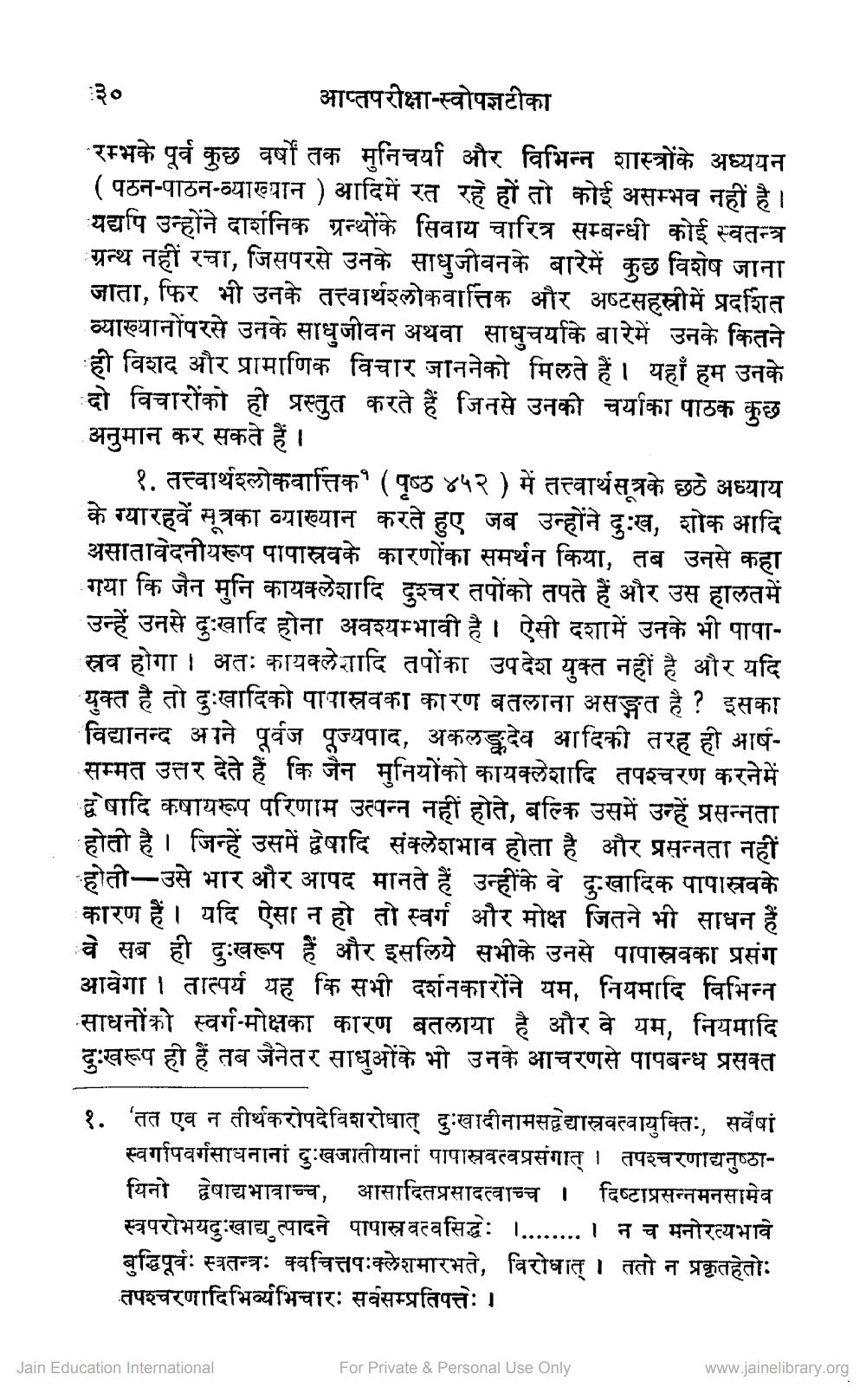________________
आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका रम्भके पूर्व कुछ वर्षों तक मुनिचर्या और विभिन्न शास्त्रोंके अध्ययन ( पठन-पाठन-व्याख्यान ) आदिमें रत रहे हों तो कोई असम्भव नहीं है। यद्यपि उन्होंने दार्शनिक ग्रन्थोंके सिवाय चारित्र सम्बन्धी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा, जिसपरसे उनके साधुजीवनके बारेमें कुछ विशेष जाना जाता, फिर भी उनके तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक और अष्टसहस्रीमें प्रदर्शित व्याख्यानोंपरसे उनके साधुजीवन अथवा साधुचर्या के बारेमें उनके कितने ही विशद और प्रामाणिक विचार जाननेको मिलते हैं। यहाँ हम उनके दो विचारोंको हो प्रस्तुत करते हैं जिनसे उनको चर्याका पाठक कुछ अनुमान कर सकते हैं।
१. तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक' (पृष्ठ ४५२ ) में तत्त्वार्थसूत्रके छठे अध्याय के ग्यारहवें सूत्रका व्याख्यान करते हुए जब उन्होंने दुःख, शोक आदि असातावेदनीयरूप पापास्रवके कारणोंका समर्थन किया, तब उनसे कहा गया कि जैन मुनि कायक्लेशादि दुश्चर तपोंको तपते हैं और उस हालतमें उन्हें उनसे दुःखादि होना अवश्यम्भावी है। ऐसी दशामें उनके भी पापास्रव होगा। अतः कायक्लेशादि तपोंका उपदेश युक्त नहीं है और यदि युक्त है तो दुःखादिको पापास्रवका कारण बतलाना असङ्गत है ? इसका विद्यानन्द अपने पूर्वज पूज्यपाद, अकलङ्कदेव आदिकी तरह ही आर्षसम्मत उत्तर देते हैं कि जैन मुनियोंको कायक्लेशादि तपश्चरण करने में द्वेषादि कषायरूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें उन्हें प्रसन्नता होती है। जिन्हें उसमें द्वेषादि संक्लेशभाव होता है और प्रसन्नता नहीं होती-उसे भार और आपद मानते हैं उन्हींके वे दुःखादिक पापास्रवके कारण हैं। यदि ऐसा न हो तो स्वर्ग और मोक्ष जितने भी साधन हैं वे सब ही दुःखरूप हैं और इसलिये सभीके उनसे पापास्रवका प्रसंग आवेगा। तात्पर्य यह कि सभी दर्शनकारोंने यम, नियमादि विभिन्न साधनोंको स्वर्ग-मोक्षका कारण बतलाया है और वे यम, नियमादि दुःखरूप ही हैं तब जैनेतर साधुओंके भी उनके आचरणसे पापबन्ध प्रसक्त
१. 'तत एव न तीर्थकरोपदेविशरोधात् दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवत्वायुक्तिः , सर्वेषां
स्वर्गापवर्गसाधनानां दुःखजातीयानां पापास्रवत्वप्रसंगात् । तपश्चरणाद्यनुष्ठायिनो द्वेषाद्यभावाच्च, आसादितप्रसादत्वाच्च । दिष्टाप्रसन्नमनसामेव स्वपरोभयदुःखाद्य त्पादने पापात्र वत्वसिद्धेः ।........। न च मनोरत्यभावे बुद्धिपूर्वः स्वतन्त्रः क्वचित्तपःक्लेशमारभते, विरोधात् । ततो न प्रकृतहेतोः तपश्चरणादिभिर्व्यभिचारः सर्वसम्प्रतिपत्तेः ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org