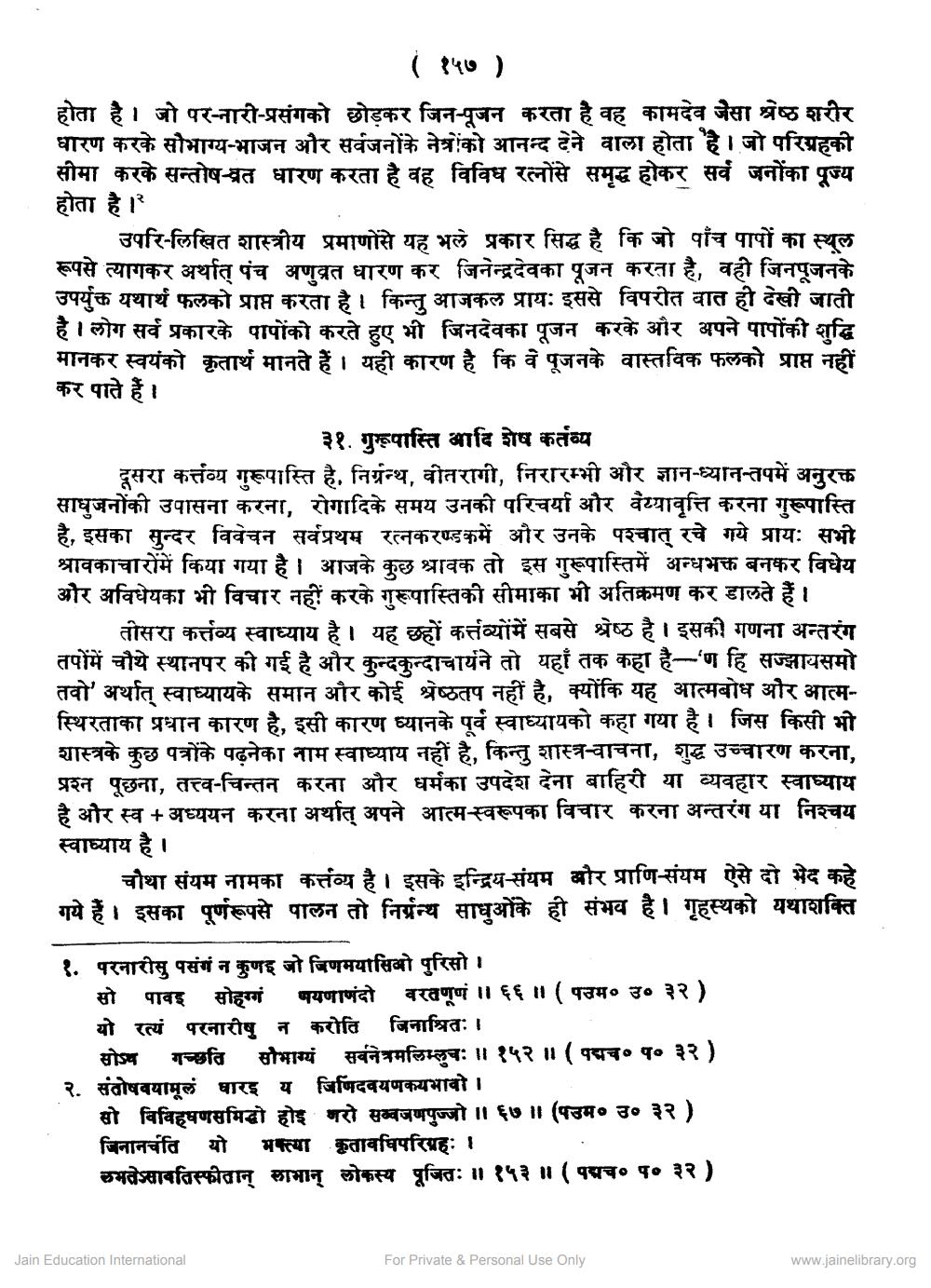________________
( १५७ ) होता है। जो पर-नारी-प्रसंगको छोड़कर जिन-पूजन करता है वह कामदेव जैसा श्रेष्ठ शरीर धारण करके सौभाग्य-भाजन और सर्वजनोंके नेत्रोंको आनन्द देने वाला होता है। जो परिग्रहकी सीमा करके सन्तोष-व्रत धारण करता है वह विविध रत्नोंसे समृद्ध होकर सर्व जनोंका पूज्य होता है।
उपरि-लिखित शास्त्रीय प्रमाणोंसे यह भले प्रकार सिद्ध है कि जो पाँच पापों का स्थल रूपसे त्यागकर अर्थात् पंच अणुव्रत धारण कर जिनेन्द्रदेवका पूजन करता है, वही जिनपूजनके उपर्युक्त यथार्थ फलको प्राप्त करता है। किन्तु आजकल प्रायः इससे विपरीत बात ही देखी जाती है। लोग सर्व प्रकारके पापोंको करते हुए भी जिनदेवका पूजन करके और अपने पापोंकी शद्धि मानकर स्वयंको कृतार्थ मानते हैं। यही कारण है कि वे पूजनके वास्तविक फलको प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
३१. गुरूपास्ति आदि शेष कर्तव्य दूसरा कर्तव्य गुरूपास्ति है. निग्रन्थ, वीतरागी, निरारम्भी और ज्ञान-ध्यान-तपमें अनुरक्त साधुजनोंकी उपासना करना, रोगादिके समय उनको परिचर्या और वैय्यावृत्ति करना गुरूपास्ति है, इसका सुन्दर विवेचन सर्वप्रथम रत्नकरण्डकमें और उनके पश्चात् रचे गये प्रायः सभी श्रावकाचारोंमें किया गया है। आजके कुछ श्रावक तो इस गुरूपास्तिमें अन्धभक्त बनकर विधेय और अविधेयका भी विचार नहीं करके गुरूपास्तिकी सीमाका भी अतिक्रमण कर डालते हैं।
तीसरा कर्तव्य स्वाध्याय है। यह छहों कर्तव्योंमें सबसे श्रेष्ठ है । इसकी गणना अन्तरंग तपोमें चौथे स्थानपर की गई है और कुन्दकुन्दाचार्यने तो यहाँ तक कहा है-'ण हि सज्झायसमो तवो' अर्थात् स्वाध्यायके समान और कोई श्रेष्ठतप नहीं है, क्योंकि यह आत्मबोध और आत्मस्थिरताका प्रधान कारण है, इसी कारण ध्यानके पूर्व स्वाध्यायको कहा गया है। जिस किसी भी शास्त्रके कुछ पत्रोंके पढ़नेका नाम स्वाध्याय नहीं है, किन्तु शास्त्र वाचना, शुद्ध उच्चारण करना, प्रश्न पूछना, तत्त्व-चिन्तन करना और धर्मका उपदेश देना बाहिरी या व्यवहार स्वाध्याय है और स्व + अध्ययन करना अर्थात् अपने आत्म-स्वरूपका विचार करना अन्तरंग या निश्चय स्वाध्याय है।
चौथा संयम नामका कर्तव्य है। इसके इन्द्रिय-संयम बौर प्राणि-संयम ऐसे दो भेद कहे गये हैं। इसका पूर्णरूपसे पालन तो निर्ग्रन्थ साधुओंके ही संभव है। गृहस्थको यथाशक्ति
१. परनारीसु पसंग न कुणइ जो जिणमयासियो पुरिसो।
सो पावइ सोहग्गं गयणाणंदो वरतणूणं ।। ६६ ॥ ( पउम० उ० ३२) यो रत्यं परनारीष न करोति जिनाश्रितः ।
सोऽथ गच्छति सौभाग्यं सर्वनेत्रमलिम्लुचः ।। १५२ ।। ( पाच. प. ३२) २. संतोषवयामूलं धारइ य जिणिदवयणकयभावो ।
सो विविहरणसमिद्धो होइ गरो सम्बजणपुज्जो ।। ६७ ॥ (पउम० उ० ३२) जिनानति यो भक्त्या कृतावधिपरिग्रहः । लभतेऽसावतिस्फीतान् सामान् लोकस्य पूजितः ॥ १५३ ॥ ( पाच. प. ३२)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org