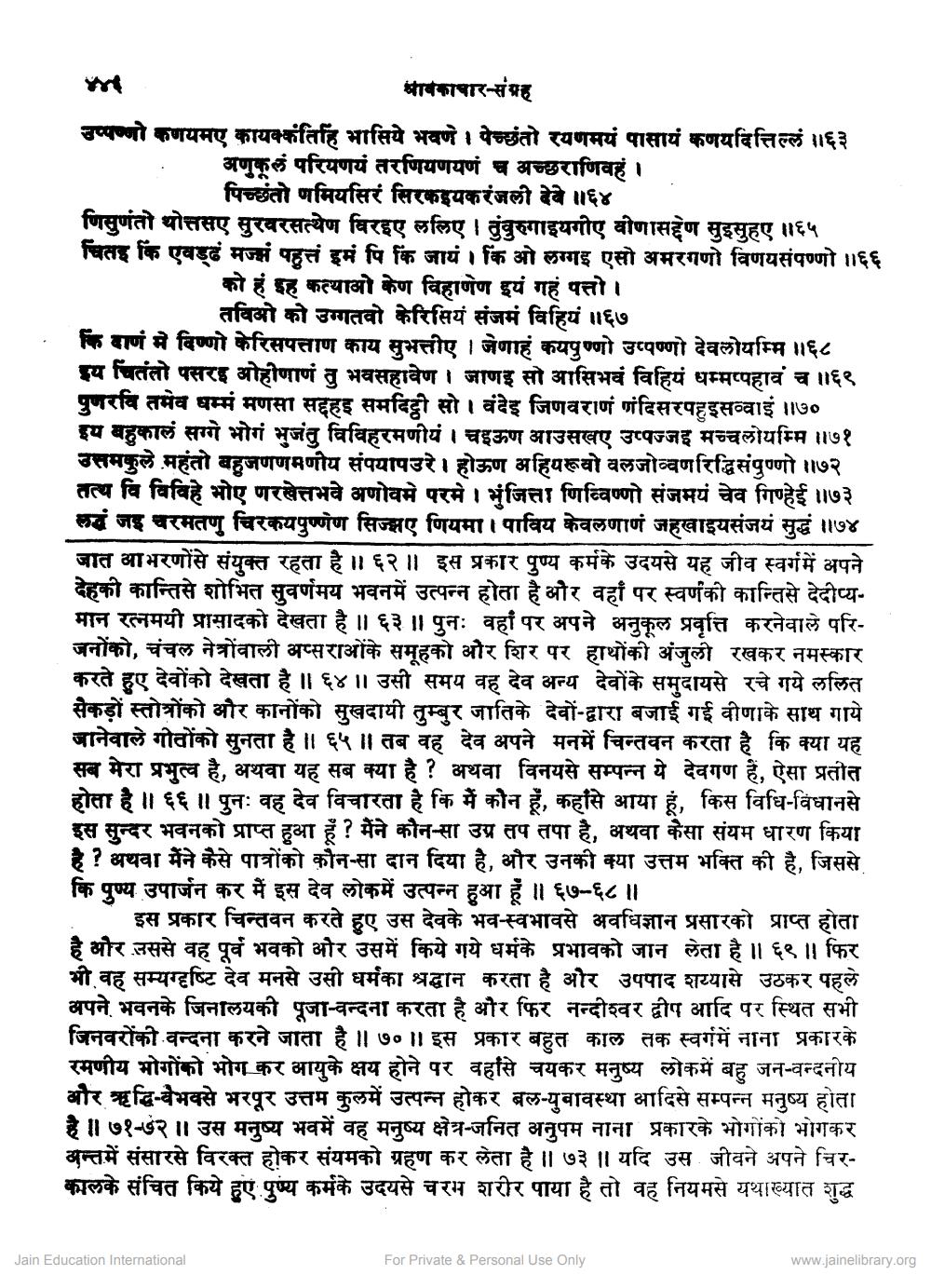________________
श्रावकाचार-संग्रह उप्पणो कणयमए कायक्कतिहि भासिये भवणे । पेच्छंतो रयणमयं पासायं कणयवित्तिल्लं ॥६३ . अणुकूलं परियणयं तरणियणयणं च अच्छराणिवहं।।
पिच्छंतो गमियसिरं सिरकइयकरंजली देवे ॥६४ । णिसुणंतो थोत्तसए सुरवरसत्येण विरइए ललिए । तुंवुरुगाइयगीए वोणासद्देण सुइसुहए ॥६५ चितइ किं एवड्ढं ममं पहत्तं इमं पि कि जायं। कि ओ लग्गइ एसो अमरगणो विणयसंपण्णो ॥६६
को हं इह कत्थाओ केण विहाणेण इयं गहं पत्तो।
तविमओ को उग्गतवो केरिसियं संजमं विहियं ॥६७ कि दाणं मे विण्णो केरिसपत्ताण काय सुभत्तीए । जेणाहं कयपुण्णो उप्पण्णो देवलोयम्मि ॥६८ इय चिप्लो पसरइ ओहोणाणं तु भवसहावेण । जाणइ सो आसिभवं विहियं धम्मप्पहावं च ॥६९ पुणरवि तमेव धम्म मणसा सद्दहइ समदिट्टी सो। वंदेड जिणवराणं गंदिसरपहुइसव्वाइं ॥७० इय बहुकालं सग्गे भोगं भुजंतु विविहरमणीयं । चइऊण आउसखए उप्पज्जइ मच्चलोयम्मि ॥७१ उत्तमकुले महंतो बहुजणणमणीय संपयापउरे। होऊण अहियरूवो वलजोव्वणरिद्धिसंपुण्णो ॥७२ तत्य वि विविहे भोए गरखेत्तभवे अणोवमे परमे । भुंजित्ता णिविण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ॥७३ ललं जइ चरमतणु चिरकयपुण्णेण सिझए णियमा। पाविय केवलणाणं जहखाइयसंजयं सुद्धं ॥७४ जात आभरणोंसे संयुक्त रहता है ॥ ६२॥ इस प्रकार पुण्य कर्मके उदयसे यह जीव स्वर्गमें अपने देहको कान्तिसे शोभित सुवर्णमय भवनमें उत्पन्न होता है और वहां पर स्वर्णको कान्तिसे देदीप्यमान रत्नमयी प्रासादको देखता है ।। ६३ । पुनः वहां पर अपने अनुकूल प्रवृत्ति करनेवाले परिजनोंको, चंचल नेत्रोंवाली अप्सराओंके समूहको और शिर पर हाथोंकी अंजुली रखकर नमस्कार करते हुए देवोंको देखता है ।। ६४ ।। उसी समय वह देव अन्य देवोंके समुदायसे रचे गये ललित सैकड़ों स्तोत्रोंको और कानोंको सुखदायी तुम्बुर जातिके देवों-द्वारा बजाई गई वीणाके साथ गाये जानेवाले गीतोंको सुनता है ।। ६५ ।। तब वह देव अपने मनमें चिन्तवन करता है कि क्या यह सब मेरा प्रभुत्व है, अथवा यह सब क्या है ? अथवा विनयसे सम्पन्न ये देवगण हैं, ऐसा प्रतीत होता है ।। ६६ ॥ पुनः वह देव विचारता है कि मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूं, किस विधि-विधानसे इस सुन्दर भवनको प्राप्त हुआ हूँ? मैंने कौन-सा उग्र तप तपा है, अथवा कैसा संयम धारण किया है ? अथवा मैंने कैसे पात्रोंको कौन-सा दान दिया है, और उनकी क्या उत्तम भक्ति की है, जिससे कि पुण्य उपार्जन कर मैं इस देव लोकमें उत्पन्न हुआ हूँ॥ ६७-६८ ॥
इस प्रकार चिन्तवन करते हुए उस देवके भव-स्वभावसे अवधिज्ञान प्रसारको प्राप्त होता है और उससे वह पूर्व भवको और उसमें किये गये धर्मके प्रभावको जान लेता है ।। ६९ ॥ फिर भी वह सम्यग्दृष्टि देव मनसे उसी धर्मका श्रद्धान करता है और उपपाद शय्यासे उठकर पहले अपने भवनके जिनालयकी पूजा-वन्दना करता है और फिर नन्दीश्वर द्वीप आदि पर स्थित सभी जिनवरोंकी वन्दना करने जाता है ।। ७०॥ इस प्रकार बहुत काल तक स्वर्गमें नाना प्रकारके रमणीय भोगोंको भोग कर आयुके क्षय होने पर वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें बह जन-वन्दनीय और ऋद्धि-वैभवसे भरपूर उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर बल-युवावस्था आदिसे सम्पन्न मनुष्य होता है ।। ७१-७२ ।। उस मनुष्य भवमें वह मनुष्य क्षेत्र-जनित अनुपम नाना प्रकारके भोगोंको भोगकर अन्तमें संसारसे विरक्त होकर संयमको ग्रहण कर लेता है ।। ७३ ।। यदि उस जीवने अपने चिरकालके संचित किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे चरम शरीर पाया है तो वह नियमसे यथाख्यात शुद्ध
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org