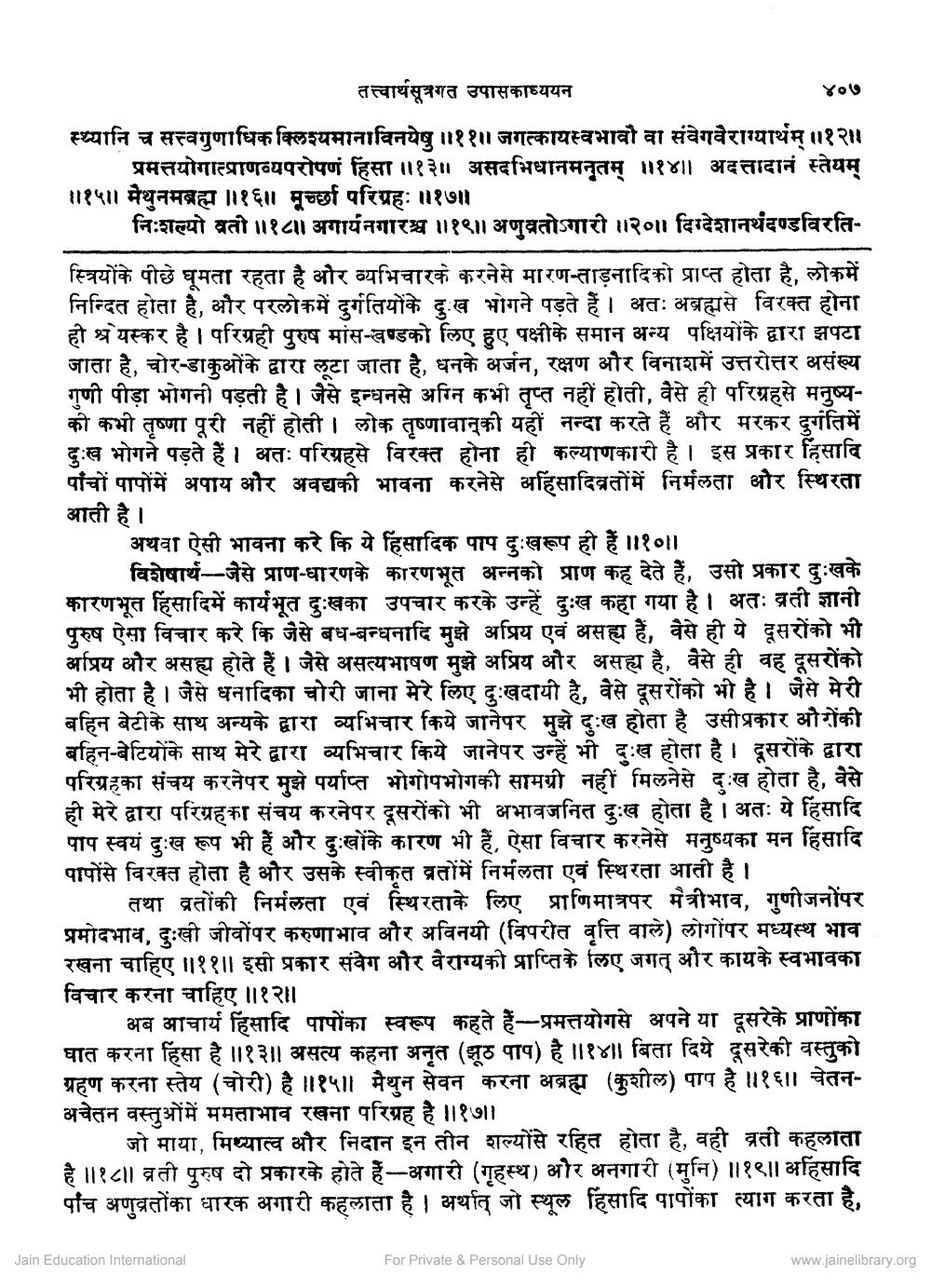________________
तत्त्वार्थसूत्रगत उपासकाध्ययन
४०७ स्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक क्लिश्यमानाविनयेषु ॥११॥ जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥
प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥१३॥ असदभिधानमनुतम् ॥१४॥ अदत्तादानं स्तेयम् ॥१५॥ मैथुनमब्रह्म ॥१६॥ मूर्छा परिग्रहः ॥१७॥
निःशल्यो वती॥१८॥ अगार्यनगारश्च ॥१९॥ अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशानर्थदण्डविरतिस्त्रियोंके पीछे घूमता रहता है और व्यभिचारके करनेसे मारण-ताड़नादिको प्राप्त होता है, लोकमें निन्दित होता है, और परलोकमें दुर्गतियोंके दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः अब्रह्मसे विरक्त होना ही श्रेयस्कर है। परिग्रही पुरुष मांस-खण्डको लिए हए पक्षीके समान अन्य पक्षियोंके द्वारा झपटा जाता है, चोर-डाकुओंके द्वारा लूटा जाता है, धनके अर्जन, रक्षण और विनाशमें उत्तरोत्तर असंख्य गुणी पीड़ा भोगनी पड़ती है। जैसे इन्धनसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, वैसे ही परिग्रहसे मनुष्यकी कभी तृष्णा पूरी नहीं होती। लोक तृष्णावान्की यहीं नन्दा करते हैं और मरकर दुर्गतिमें दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः परिग्रहसे विरक्त होना ही कल्याणकारी है। इस प्रकार हिंसादि पांचों पापोंमें अपाय और अवद्यकी भावना करनेसे अहिंसादिव्रतोंमें निर्मलता और स्थिरता आती है।
अथवा ऐसी भावना करे कि ये हिंसादिक पाप दुःखरूप ही हैं ॥१०॥
विशेषार्थ-जैसे प्राण-धारणके कारणभूत अन्नको प्राण कह देते हैं, उसी प्रकार दुःखके कारणभूत हिंसादिमें कार्यभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कहा गया है। अतः व्रती ज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करे कि जैसे बध-बन्धनादि मुझे अप्रिय एवं असह्य हैं, वैसे ही ये दूसरोंको भी अप्रिय और असह्य होते हैं। जैसे असत्यभाषण मझे अप्रिय और असह्य है, वैसे ही वह दूसरोंको भी होता है । जैसे धनादिका चोरी जाना मेरे लिए दुःखदायी है, वैसे दूसरोंको भी है। जैसे मेरी बहिन बेटीके साथ अन्यके द्वारा व्यभिचार किये जानेपर मुझे दुःख होता है उसीप्रकार औरोंकी बहिन-बेटियोंके साथ मेरे द्वारा व्यभिचार किये जानेपर उन्हें भी दुःख होता है। दूसरोंके द्वारा परिग्रहका संचय करनेपर मुझे पर्याप्त भोगोपभोगकी सामग्री नहीं मिलनेसे दुःख होता है, वैसे ही मेरे द्वारा परिग्रहका संचय करनेपर दूसरोंको भी अभावजनित दुःख होता है । अतः ये हिंसादि पाप स्वयं दुःख रूप भी हैं और दुःखोंके कारण भी हैं, ऐसा विचार करनेसे मनुष्यका मन हिंसादि पापोंसे विरक्त होता है और उसके स्वीकृत व्रतोंमें निर्मलता एवं स्थिरता आती है।
तथा व्रतोंकी निर्मलता एवं स्थिरताके लिए प्राणिमात्रपर मैत्रीभाव, गुणीजनोंपर प्रमोदभाव, दुःखी जीवोंपर करुणाभाव और अविनयी (विपरीत वृत्ति वाले) लोगोंपर मध्यस्थ भाव रखना चाहिए ॥११।। इसी प्रकार संवेग और वैराग्यको प्राप्तिके लिए जगत् और कायके स्वभावका विचार करना चाहिए ॥१२॥
__ अब आचार्य हिंसादि पापोंका स्वरूप कहते हैं-प्रमत्तयोगसे अपने या दूसरेके प्राणोंका घात करना हिंसा है ।।१३।। असत्य कहना अनृत (झूठ पाप) है ॥१४॥ बिता दिये दूसरेकी वस्तुको ग्रहण करना स्तेय (चोरी) है ॥१५॥ मैथुन सेवन करना अब्रह्म (कुशील) पाप है ॥१६॥ चेतनअचेतन वस्तुओं में ममताभाव रखना परिग्रह है ॥१७॥
जो माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे रहित होता है, वही व्रती कहलाता है ।।१८॥ व्रती पुरुष दो प्रकारके होते हैं-अगारी (गृहस्थ) और अनगारी (मुनि) ॥१९|| अहिंसादि पांच अणुव्रतोंका धारक अगारी कहलाता है । अर्थात् जो स्थूल हिंसादि पापोंका त्याग करता है,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org