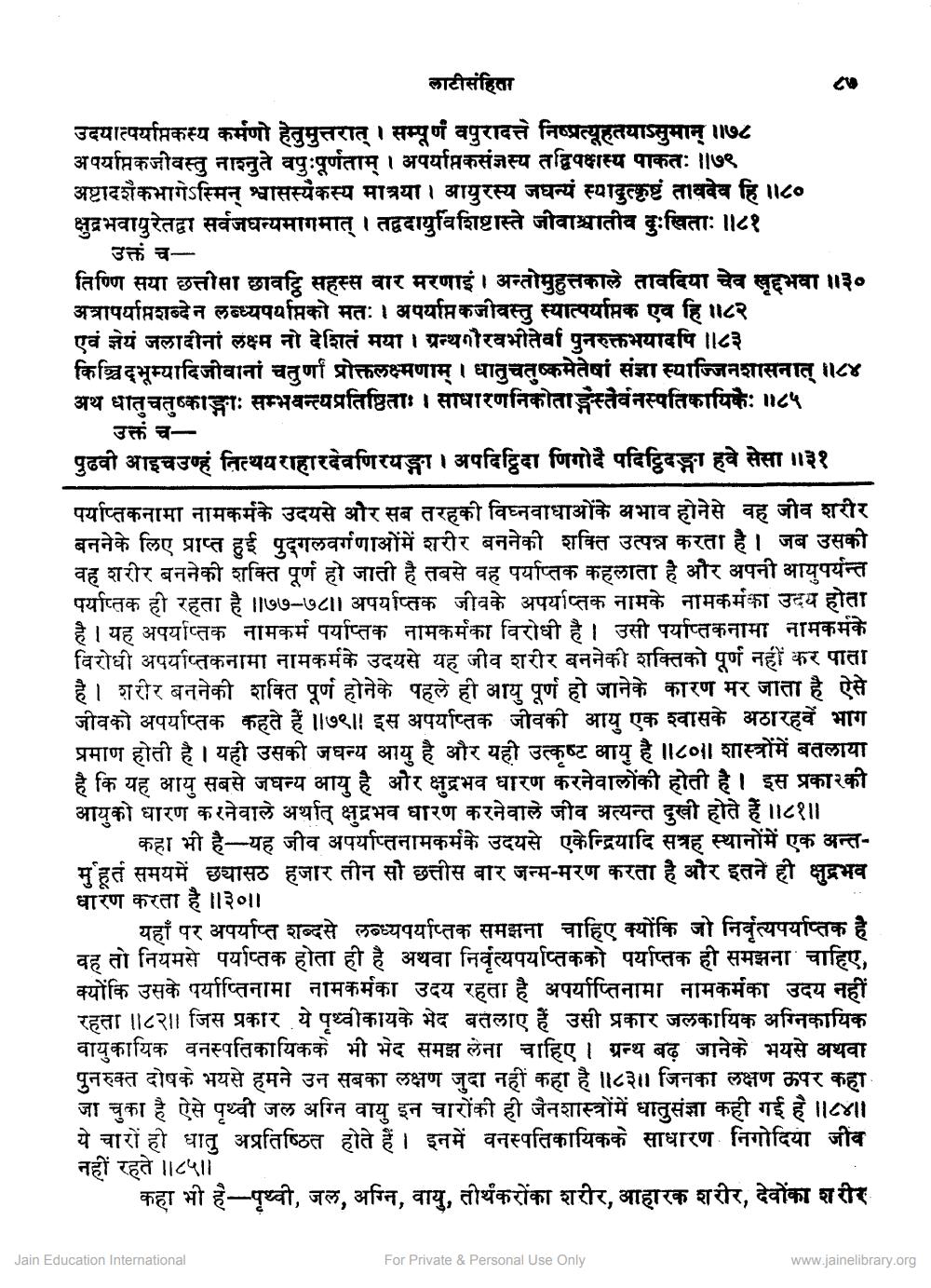________________
लाटीसंहिता
उदयात्पर्याप्तकस्य कर्मणो हेतुमुत्तरात् । सम्पूर्ण वपुरादत्ते निष्प्रत्यूहतयाऽसुमान् ॥७८ अपर्याप्तकजीवस्तु नाश्नुते वपुःपूर्णताम् । अपर्याप्तकसंजस्य तद्विपक्षास्य पाकतः ॥७९ अष्टादशैकभागेऽस्मिन् श्वासस्यैकस्य मात्रया। आयुरस्य जघन्यं स्यादुत्कृष्टं तावदेव हि ॥८० क्षुद्रभवायुरेतद्वा सर्वजघन्यमागमात् । तद्वदायुविशिष्टास्ते जीवाश्चातीव दुःखिताः ॥८१
उक्तं चतिण्णि सया छत्तीसा छावटि सहस्स वार मरणाई। अन्तोमुत्तकाले तावदिया चेव खुद्दभवा ॥३० अत्रापर्याप्तशब्देन लब्ध्यपर्याप्तको मतः । अपर्याप्त कजीवस्तु स्यात्पर्याप्तक एव हि ॥८२ एवं ज्ञेयं जलादीनां लक्ष्म नो देशितं मया। ग्रन्थगौरवभीतेर्वा पुनरुक्तभयावपि ॥८३ किञ्चिद्भूम्यादिजीवानां चतुर्णां प्रोक्तलक्ष्मणाम् । धातुचतुष्कमेतेषां संज्ञा स्याज्जिनशासनात् ॥८४ अथ धातुचतुष्काङ्गाः सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिताः । साधारणनिकोताङ्गैस्तैर्वनस्पतिकायिकैः ॥८५
उक्तं चपुढवी आइचउण्हं तित्थयराहारदेवणिरयङ्गा । अपदिट्ठिदा णिगोदै पदिदिदङ्गा हवे सेसा ॥३१ पर्याप्तकनामा नामकर्मके उदयसे और सब तरहकी विघ्नवाधाओंके अभाव होनेसे वह जीव शरीर बननेके लिए प्राप्त हुई पुद्गलवर्गणाओंमें शरीर बननेकी शक्ति उत्पन्न करता है। जब उसकी वह शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण हो जाती है तबसे वह पर्याप्तक कहलाता है और अपनी आयुपर्यन्त पर्याप्तक ही रहता है ॥७७-७८॥ अपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकर्मका उदय होता है । यह अपर्याप्तक नामकर्म पर्याप्तक नामकर्मका विरोधी है। उसी पर्याप्तकनामा नामकर्मके विरोधी अपर्याप्तकनामा नामकर्मके उदयसे यह जीव शरीर बननेकी शक्तिको पूर्ण नहीं कर पाता है। शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण होनेके पहले ही आयु पूर्ण हो जानेके कारण मर जाता है ऐसे जीवको अपर्याप्तक कहते हैं ॥७९॥ इस अपर्याप्तक जीवकी आयु एक श्वासके अठारहवें भाग प्रमाण होती है। यही उसकी जघन्य आयु है और यही उत्कृष्ट आयु है ।।८०॥ शास्त्रोंमें बतलाया है कि यह आयु सबसे जघन्य आयु है और क्षुद्रभव धारण करनेवालोंकी होती है। इस प्रकारको आयको धारण करनेवाले अर्थात क्षद्रभव धारण करनेवाले जीव अत्यन्त दुखी होते हैं॥८॥
कहा भी है-यह जीव अपर्याप्तनामकर्मके उदयसे एकेन्द्रियादि सत्रह स्थानोंमें एक अन्तमहर्त समयमें छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म-मरण करता है और इतने ही क्षद्रभव धारण करता है ॥३०॥
यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे लब्ध्यपर्याप्तक समझना चाहिए क्योंकि जो निर्वृत्यपर्याप्तक है वह तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निवृत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके पर्याप्तिनामा नामकर्मका उदय रहता है अपर्याप्तिनामा नामकर्मका उदय नहीं रहता ।।८२।। जिस प्रकार ये पृथ्वीकायके भेद बतलाए हैं उसी प्रकार जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक वनस्पतिकायिकके भी भेद समझ लेना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे अथवा पुनरुक्त दोषके भयसे हमने उन सबका लक्षण जुदा नहीं कहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण ऊपर कहा जा चुका है ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारोंकी ही जैनशास्त्रोंमें धातुसंज्ञा कही गई है ॥४॥ ये चारों ही धातु अप्रतिष्ठित होते हैं। इनमें वनस्पतिकायिकके साधारण निगोदिया जीव नहीं रहते ॥८५॥
कहा भी है-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीर्थंकरोंका शरीर, आहारक शरीर, देवोंका शरीर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org