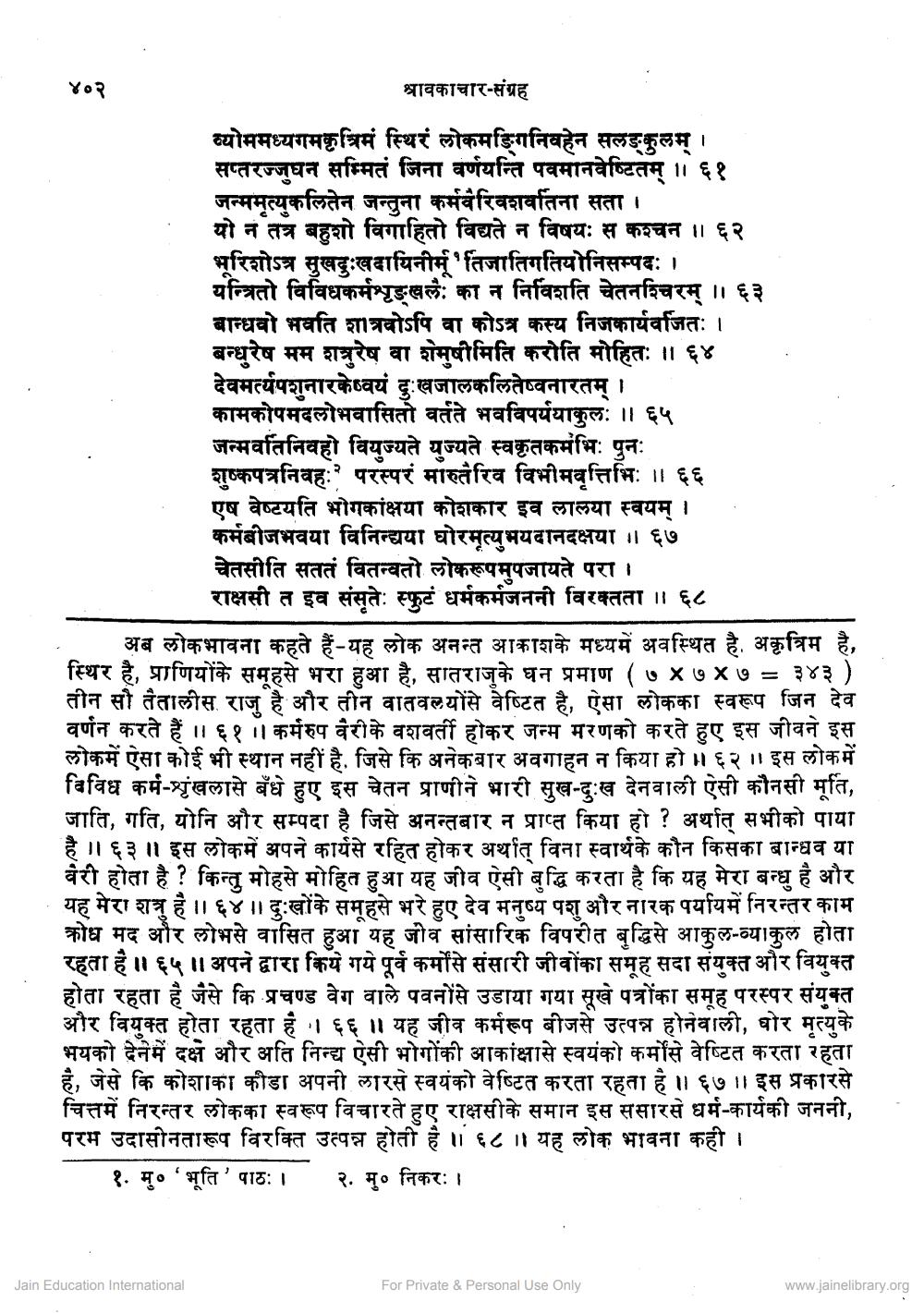________________
४०२
श्रावकाचार-संग्रह
व्योममध्यगमकृत्रिमं स्थिरं लोकमगिनिवहेन सलकुलम् । सप्तरज्जुधन सम्मितं जिना वर्णयन्ति पवमानवेष्टितम् ।। ६१ जन्ममृत्युकलितेन जन्तुना कर्मवैरिवशतिना सता । यो न तत्र बहुशो विगाहितो विद्यते न विषयः स कश्चन ।। ६२ भूरिशोऽत्र सुखदुःखदायिनीतिजातिगतियोनिसम्पदः । यन्त्रितो विविधकर्मशृङ्खलैः का न निविंशति चेतनश्चिरम् ।। ६३ बान्धवो भवति शात्रवोऽपि वा कोऽत्र कस्य निजकार्यजितः । बन्धुरेष मम शत्रुरेष वा शेमुषीमिति करोति मोहितः ।। ६४ देवमर्त्यपशुनारकेष्वयं दुःखजालकलितेष्वनारतम् । कामकोपमदलोभवासितो वर्तते भवविपर्ययाकुल: ।। ६५ जन्मतिनिवहो वियुज्यते युज्यते स्वकृतकर्मभिः पुनः शुष्कपत्रनिवहः परस्परं मारुतैरिव विभीमवृत्तिभिः ।। ६६ एष वेष्टयति भोगकांक्षया कोशकार इव लालया स्वयम् । कर्मबीजभवया विनिन्द्यया घोरमृत्युभयदानदक्षया ।। ६७ चेतसीति सततं वितन्वतो लोकरूपमुपजायते परा।
राक्षसी त इव संसृतेः स्फुटं धर्मकर्मजननी विरक्तता ।। ६८ अब लोकभावना कहते हैं-यह लोक अनन्त आकाशके मध्य में अवस्थित है. अकृत्रिम है, स्थिर है, प्राणियोंके समहसे भरा हुआ है, सातराजके घन प्रमाण (७४ ७४७ = ३४३ ) तीन सौ तैतालीस राज है और तीन वातवलयोंसे वेष्टित है. ऐसा लोकका स्वरूप जिन देव वर्णन करते हैं ।। ६१ ।। कर्मरुप वैरीके वशवर्ती होकर जन्म मरणको करते हुए इस जीवने इस लोकमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं है. जिसे कि अनेकबार अवगाहन न किया हो।। ६२ ।। इस लोक में विविध कर्म-शृंखलासे बँधे हुए इस चेतन प्राणीने भारी सुख-दुःख देनवाली ऐसी कौनसी मूर्ति, जाति, गति, योनि और सम्पदा है जिसे अनन्तबार न प्राप्त किया हो ? अर्थात् सभीको पाया है ।। ६३ ॥ इस लोकमें अपने कार्यसे रहित होकर अर्थात् विना स्वार्थके कौन किसका बान्धव या वैरी होता है ? किन्तु मोहसे मोहित हुआ यह जीव ऐसी बुद्धि करता है कि यह मेरा बन्धु है और यह मेरा शत्रु है ।। ६४ ॥ दुःखोंके समूहसे भरे हुए देव मनुष्य पशु और नारक पर्यायमें निरन्तर काम क्रोध मद और लोभसे वासित हुआ यह जीव सांसारिक विपरीत बुद्धिसे आकुल-व्याकुल होता रहता है ।। ६५ ।। अपने द्वारा किये गये पूर्व कर्मोंसे संसारी जीवोंका समूह सदा संयुक्त और वियुक्त होता रहता है जैसे कि प्रचण्ड वेग वाले पवनोंसे उडाया गया सूखे पत्रोंका समूह परस्पर संयुक्त और वियुक्त होता रहता है । ६६ ॥ यह जीव कर्मरूप बीजसे उत्पन्न होनेवाली, घोर मृत्युके भयको देने में दक्ष और अति निन्द्य ऐसी भोगोंकी आकांक्षासे स्वयंको कर्मोंसे वेष्टित करता रहता है, जैसे कि कोशाका कौडा अपनी लारसे स्वयंको वेष्टित करता रहता है ॥६७ ।। इस प्रकारसे चित्तमें निरन्तर लोकका स्वरूप विचारते हुए राक्षसीके समान इस ससारसे धर्म-कार्यकी जननी, परम उदासीनतारूप विरक्ति उत्पन्न होती है ।। ६८ ॥ यह लोक भावना कही ।
१. मु० 'भूति' पाठः । २. मु० निकरः ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org