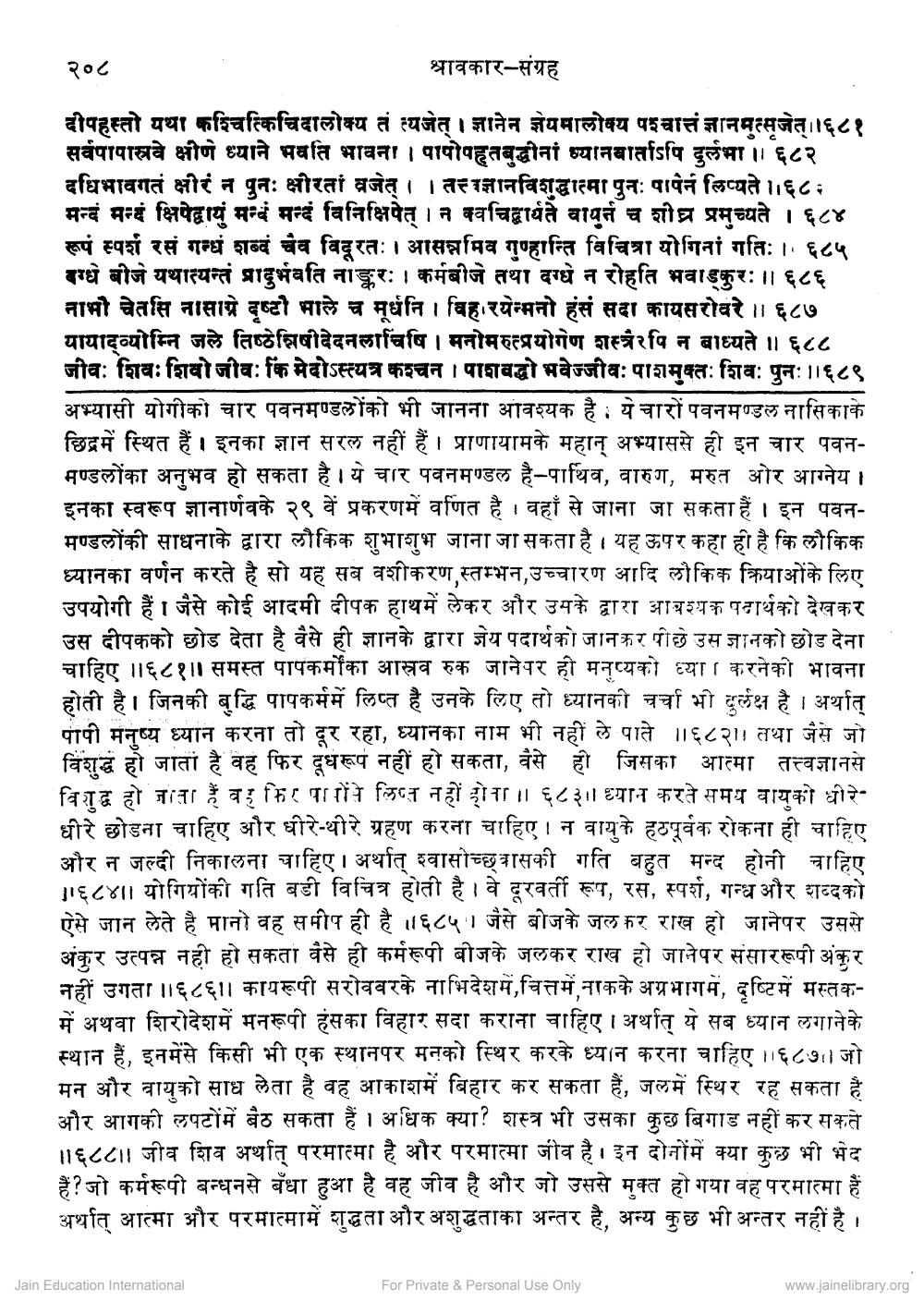________________
२०८
श्रावकार-संग्रह
दीपहस्तो यथा कश्चित्किचिदालोक्य तं त्यजेत् । ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चात्तं ज्ञानमुत्सजेत्।।६८१ सर्वपापासवे क्षीणे ध्याने भवति भावना । पापोपहतबुद्धीनां ध्यानबार्ताऽपि दुर्लभा॥ ६८२ दधिभावगतं क्षीरं न पुनः क्षीरतां व्रजेत् । । तत्त्वज्ञानविशुद्धात्मा पुनः पापन लिप्यते ।।६८ः मन्दं मन्दं क्षिपेद्वायु मन्दं मन्दं विनिक्षिपेत् । न क्वचिद्वार्यते वायर्न च शीघ्र प्रमुच्यते । ६८४ रूपं स्पर्श रसं गन्धं शब्दं चैव विदूरतः । आसन्नमिव गुण्हान्ति विचित्रा योगिनां गतिः ।। ६८५ बग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्करः । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाड्कुरः ।। ६८६ नाभी चेतसि नासाग्रे दृष्टो भाले च मूर्धनि । विहारयेन्मनो हंसं सदा कायसरोवरे ।। ६८७ यायाव्योम्नि जले तिष्ठेन्निषीदेदनलाचिषि । मनोमरुत्प्रयोगेण शस्त्रैरपि न बाध्यते ॥ ६८८ जीवः शिवः शिवो जीवः कि मेदोऽस्त्यत्र कश्चन । पाशवद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः शिवः पुनः ।। ६८९ अभ्यासी योगीको चार पवनमण्डलोंको भी जानना आवश्यक है : ये चारों पवनमण्डल नासिकाके छिद्र में स्थित हैं। इनका ज्ञान सरल नहीं हैं। प्राणायामके महान् अभ्याससे ही इन चार पवनमण्डलोंका अनुभव हो सकता है। ये चार पवनमण्डल है-पार्थिव, वारुग, मरुत ओर आग्नेय। इनका स्वरूप ज्ञानार्णवके २९ वें प्रकरण में वर्णित है । वहाँ से जाना जा सकता हैं । इन पवनमण्डलोंकी साधनाके द्वारा लौकिक शुभाशुभ जाना जा सकता है। यह ऊपर कहा ही है कि लौकिक ध्यानका वर्णन करते है सो यह सब वशीकरण स्तम्भन,उच्चारण आदि लौकिक क्रियाओंके लिए उपयोगी हैं। जैसे कोई आदमी दीपक हाथ में लेकर और उसके द्वारा आवश्यक पदार्थको देखकर उस दीपकको छोड़ देता है वैसे ही ज्ञानके द्वारा ज्ञेय पदार्थको जानकर पीछे उस ज्ञानको छोड देना चाहिए ॥६८१।। समस्त पापकर्मोका आस्रव रुक जानेपर ही मनुष्यको ध्या। करनेकी भावना होती है। जिनकी बुद्धि पापकर्ममें लिप्त है उनके लिए तो ध्यानकी चर्चा भी दुर्लक्ष है । अर्थात् पापी मनष्य ध्यान करना तो दूर रहा, ध्यानका नाम भी नहीं ले पाते ॥६८२।। तथा जैसे जो विशुद्ध हो जाता है वह फिर दूधरूप नहीं हो सकता, वैसे ही जिसका आत्मा तत्त्वज्ञानसे विशद्व हो जाता हैं वह फिर पापोंसे लिप्त नहीं होता ।। ६८३।। ध्यान करते समय बायुको धीरेधीरे छोडना चाहिए और धीरे-धीरे ग्रहण करना चाहिए । न वायुके हठपूर्वक रोकना ही चाहिए और न जल्दी निकालना चाहिए । अर्थात् श्वासोच्छ्वासकी गति बहुत मन्द होनी चाहिए ६८४|| योगियोंकी गति बडी विचित्र होती है। वे दूरवर्ती रूप, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्दको ऐसे जान लेते है मानो वह समीप ही है ।।६८५ । जैसे बीजके जल कर राख हो जानेपर उससे अंकर उत्पन्न नही हो सकता वैसे ही कर्मरूपी बीजके जलकर राख हो जानेपर संसाररूपी अंकुर नहीं उगता ॥६८६।। कायरूपी सरोववरके नाभिदेशम,चित्तमें नाकके अग्रभागम, दृष्टि में मस्तकमें अथवा शिरोदेशमें मनरूपी हंसका विहार सदा कराना चाहिए । अर्थात् ये सब ध्यान लगाने के स्थान हैं, इनमेंसे किसी भी एक स्थानपर मनको स्थिर करके ध्यान करना चाहिए ।।६८७। जो मन और बायको साध लेता है वह आकाशमें बिहार कर सकता हैं, जल में स्थिर रह सकता है और आगकी लपटोंमें बैठ सकता हैं । अधिक क्या? शस्त्र भी उसका कुछ बिगाड नहीं कर सकते ॥६८८। जीव शिव अर्थात् परमात्मा है और परमात्मा जीव है। इन दोनोंमें क्या कुछ भी भेद हैं? जो कर्मरूपी बन्धनसे बँधा हुआ है वह जीव है और जो उससे मुक्त हो गया वह परमात्मा हैं अर्थात् आत्मा और परमात्मामें शुद्धता और अशुद्धताका अन्तर है, अन्य कुछ भी अन्तर नहीं है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org