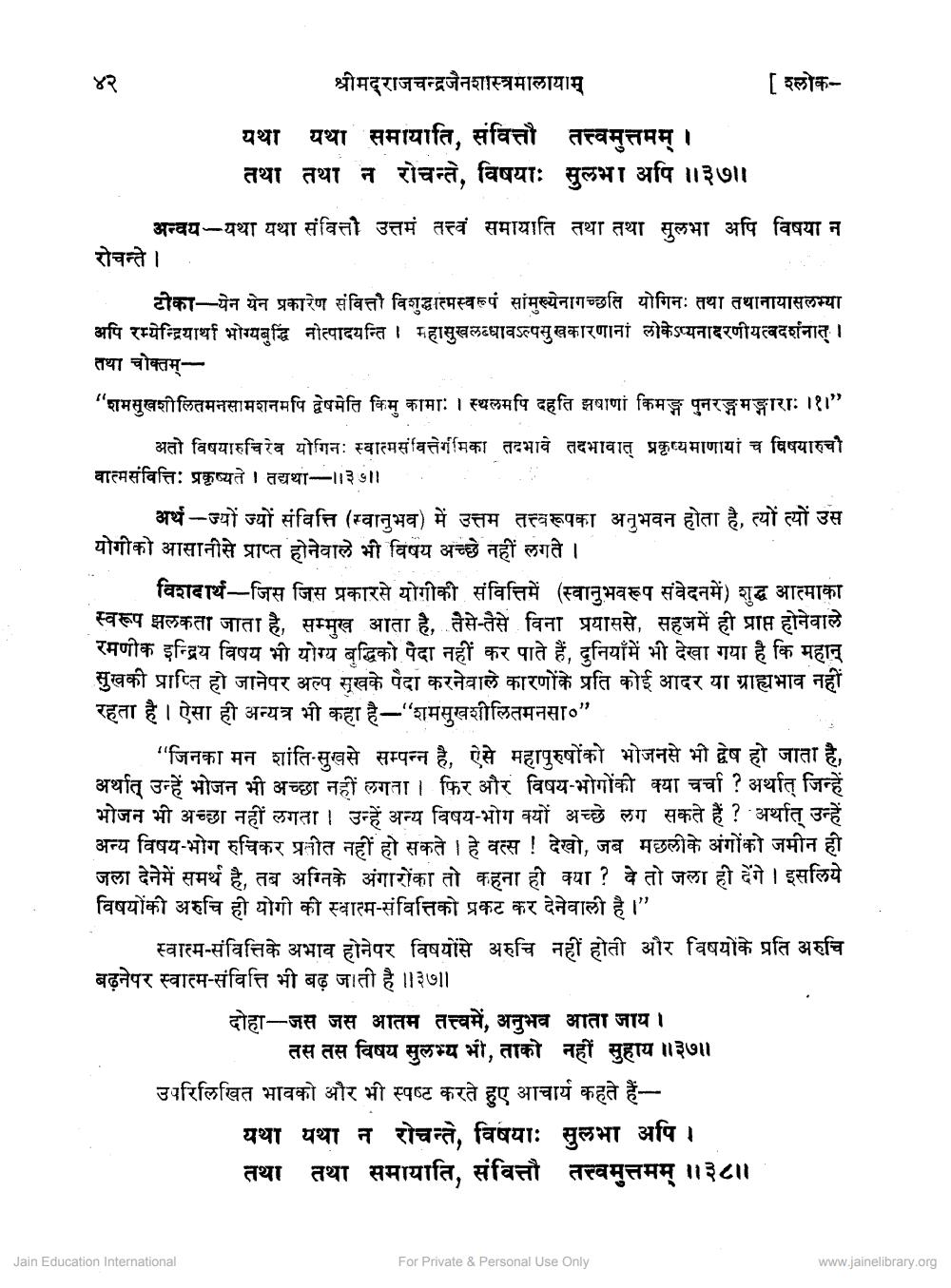________________
श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्
[ श्लोकयथा यथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ।
तथा तथा न रोचन्ते, विषयाः सुलभा अपि ॥३७॥ अन्वय-यथा यथा संवित्ती उत्तमं तत्त्वं समायाति तथा तथा सुलभा अपि विषया न
रोचन्ते।
टोका-येन येन प्रकारेण संवित्तौ विशुद्धात्मस्वरूपं सांमुख्येनागच्छति योगिनः तथा तथानायासलभ्या अपि रम्येन्द्रियार्था भोग्यबुद्धि नोत्पादयन्ति । महासुखलब्धावऽल्पसुखकारणानां लोकेऽप्यनादरणीयत्वदर्शनात् । तथा चोक्तम्"शमसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किमु कामाः । स्थलमपि दहति झषाणां किमङ्ग पुनरङ्गमगाराः ।।"
अतो विषयारुचिरेव योगिनः स्वात्मसंवित्तेमिका तदभावे तदभावात् प्रकृष्यमाणायां च विषयारुची वात्मसंवित्तिः प्रकृष्यते । तद्यथा-॥३७॥
अर्थ-ज्यों ज्यों संवित्ति (स्वानुभव) में उत्तम तत्त्वरूपका अनुभवन होता है, त्यों त्यों उस योगीको आसानीसे प्राप्त होनेवाले भी विषय अच्छे नहीं लगते ।
विशदार्थ-जिस जिस प्रकारसे योगीकी संवित्तिों (स्वानुभवरूप संवेदनमें) शुद्ध आत्माका स्वरूप झलकता जाता है, सम्मख आता है, तैसे-तैसे विना प्रयाससे, सहजमें ही प्राप्त होनेवाले रमणीक इन्द्रिय विषय भी योग्य बुद्धिको पैदा नहीं कर पाते हैं, दुनियाँमें भी देखा गया है कि महान् सुखकी प्राप्ति हो जानेपर अल्प सूखके पैदा करनेवाले कारणोंके प्रति कोई आदर या ग्राह्यभाव नहीं रहता है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है-"शमसुखशीलितमनसा०"
"जिनका मन शांति-सुखसे सम्पन्न है, ऐसे महापुरुषोंको भोजनसे भी द्वेष हो जाता है, अर्थात् उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता। फिर और विषय-भोगोंकी क्या चर्चा ? अर्थात् जिन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें अन्य विषय-भोग क्यों अच्छे लग सकते हैं ? अर्थात् उन्हें अन्य विषय-भोग रुचिकर प्रतीत नहीं हो सकते । हे वत्स ! देखो, जब मछलीके अंगोंको जमीन ही जला देनेमें समर्थ है, तब अग्निके अंगारोंका तो कहना ही क्या? वे तो जला ही देंगे । इसलिये विषयोंकी अरुचि ही योगी की स्वात्म-संवित्तिको प्रकट कर देनेवाली है ।"
स्वात्म-संवित्तिके अभाव होनेपर विषयोंसे अरुचि नहीं होती और विषयोंके प्रति अरुचि बढ़नेपर स्वात्म-संवित्ति भी बढ़ जाती है ॥३७॥
दोहा-जस जस आतम तत्त्वमें, अनुभव आता जाय ।
तस तस विषय सुलभ्य भी, ताको नहीं सुहाय ॥३७॥ उपरिलिखित भावको और भी स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं
यथा यथा न रोचन्ते, विषयाः सुलभा अपि । तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्वमुत्तमम् ॥३८॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org