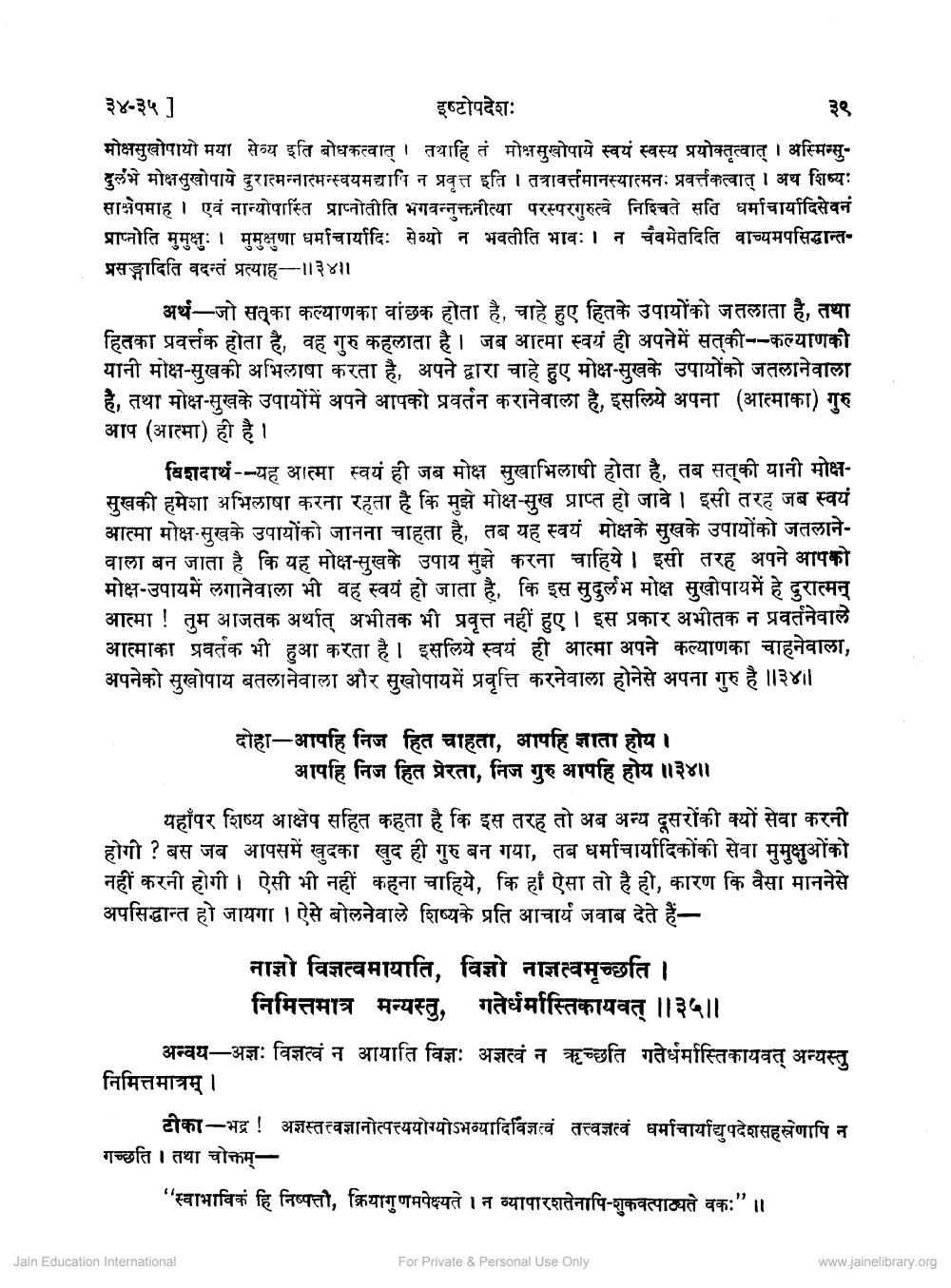________________
३४-३५]
इष्टोपदेशः
मोक्षसुखोपायो मया सेव्य इति बोधकत्वात् । तथाहि तं मोक्षसुखोपाये स्वयं स्वस्य प्रयोक्तृत्वात् । अस्मिन्सुदुर्लभे मोक्षसुखोपाये दुरात्मन्नात्मन्स्वयमद्यापि न प्रवृत्त इति । तत्रावर्त्तमानस्यात्मनः प्रवर्तकत्वात् । अथ शिष्यः साक्षेपमाह । एवं नान्योपास्ति प्राप्नोतीति भगवन्नक्तनीत्या परस्परगुरुत्वे निश्चिते सति धर्माचार्यादिसेवनं प्राप्नोति मुमुक्षुः । मुमुक्षुणा धर्माचार्यादिः सेव्यो न भवतीति भावः । न चैवमेतदिति वाच्यमपसिद्धान्तप्रसङ्गादिति वदन्तं प्रत्याह-॥३४॥
अर्थ-जो सत्का कल्याणका वांछक होता है, चाहे हुए हितके उपायोंको जतलाता है, तथा हितका प्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है। जब आत्मा स्वयं ही अपनेमें सत्की--कल्याणकी यानी मोक्ष-सुखकी अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष-सुखके उपायोंको जतलानेवाला है, तथा मोक्ष-सुखके उपायोंमें अपने आपको प्रवर्तन करानेवाला है, इसलिये अपना (आत्माका) गुरु आप (आत्मा) ही है।
विशदार्थ--यह आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुखाभिलाषी होता है, तब सत्की यानी मोक्षसुखकी हमेशा अभिलाषा करता रहता है कि मुझे मोक्ष-सुख प्राप्त हो जावे। इसी तरह जब स्वयं आत्मा मोक्ष-सुखके उपायोंको जानना चाहता है, तब यह स्वयं मोक्षके सुखके उपायोंको जतलानेवाला बन जाता है कि यह मोक्ष-सुखके उपाय मुझे करना चाहिये। इसी तरह अपने आपको मोक्ष-उपायमें लगानेवाला भी वह स्वयं हो जाता है, कि इस सुदुर्लभ मोक्ष सुखोपायमें हे दुरात्मन् आत्मा ! तुम आजतक अर्थात् अभीतक भी प्रवृत्त नहीं हुए। इस प्रकार अभीतक न प्रवर्तनेवाले आत्माका प्रवर्तक भी हुआ करता है। इसलिये स्वयं ही आत्मा अपने कल्याणका चाहनेवाला, अपनेको सुखोपाय बतलानेवाला और सुखोपायमें प्रवृत्ति करनेवाला होनेसे अपना गुरु है ॥३४॥
दोहा-आपहि निज हित चाहता, आपहि ज्ञाता होय।
आपहि निज हित प्रेरता, निज गुरु आपहि होय ॥३४॥ यहाँपर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अन्य दूसरोंकी क्यों सेवा करनी होगी ? बस जब आपसमें खुदका खुद ही गुरु बन गया, तब धर्माचार्यादिकोंकी सेवा मुमुक्षुओंको नहीं करनी होगी। ऐसी भी नहीं कहना चाहिये, कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि वैसा माननेसे अपसिद्धान्त हो जायगा । ऐसे बोलनेवाले शिष्यके प्रति आचार्य जवाब देते हैं
नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति ।
निमित्तमात्र मन्यस्तु, गतेधर्मास्तिकायवत् ।।३५॥ अन्वय-अज्ञः विज्ञत्वं न आयाति विज्ञः अज्ञत्वं न ऋच्छति गतेधर्मास्तिकायवत् अन्यस्तु निमित्तमात्रम् ।
टीका-भद्र ! अज्ञस्तत्त्वज्ञानोत्पत्त्ययोग्योऽभव्यादिविज्ञत्वं तत्त्वज्ञत्वं धर्माचार्याधुपदेशसहस्रेणापि न गच्छति । तथा चोक्तम्
"स्वाभाविक हि निष्पत्ती, क्रियागुणमपेक्ष्यते । न व्यापारशतेनापि-शकवत्पाठ्यते वकः" ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org