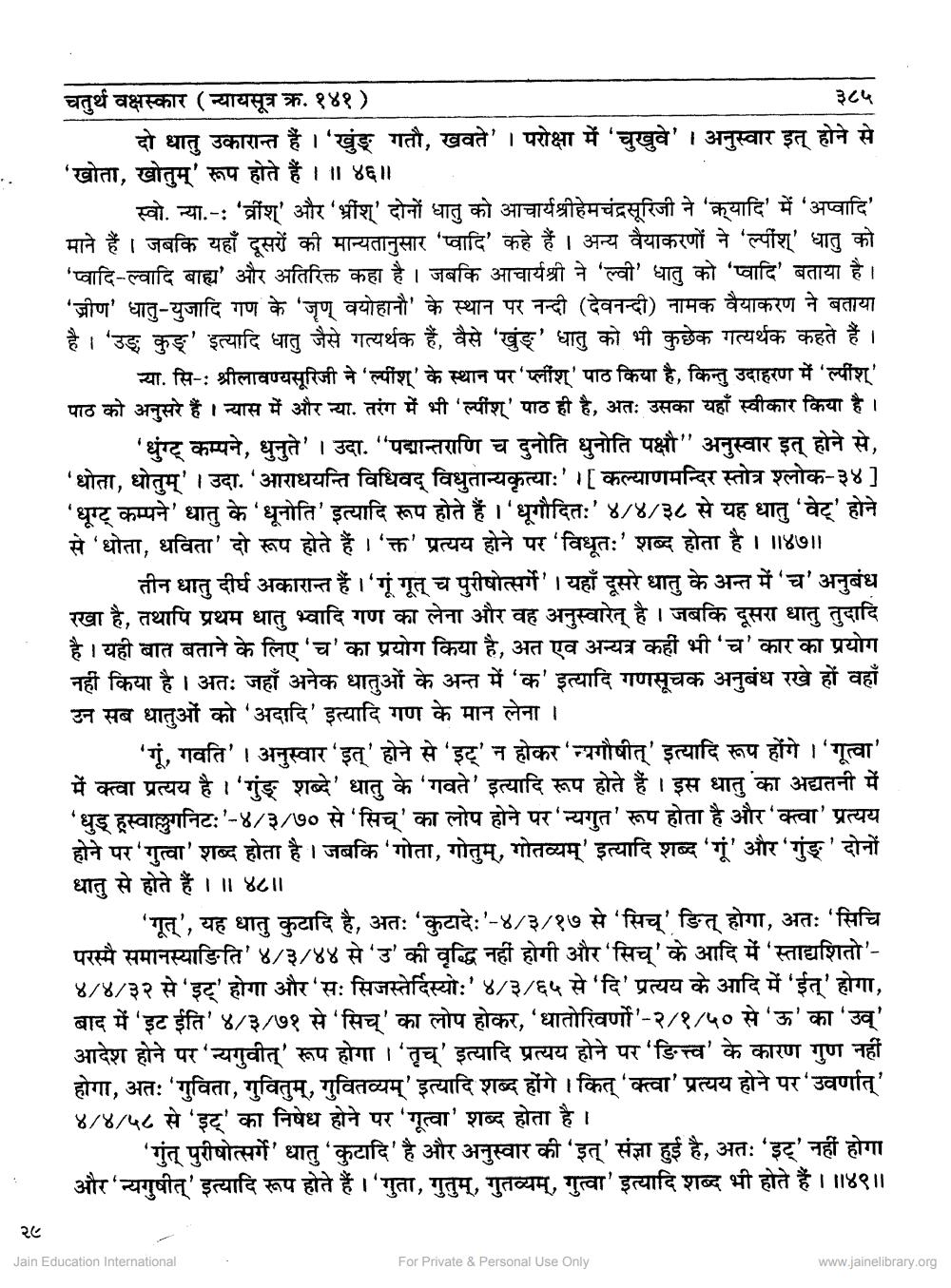________________
चतुर्थ वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. १४१)
३८५ दो धातु उकारान्त हैं । 'खुंङ् गतौ, खवते' । परीक्षा में 'चुखुवे' । अनुस्वार इत् होने से 'खोता, खोतुम्' रूप होते हैं । ॥ ४६॥
स्वो. न्या.-: 'वींश्' और 'श्रीश्' दोनों धातु को आचार्यश्रीहेमचंद्रसूरिजी ने 'क्यादि' में 'अप्वादि' माने हैं। जबकि यहाँ दूसरों की मान्यतानुसार 'प्वादि' कहे हैं । अन्य वैयाकरणों ने 'ल्पीश्' धातु को "प्वादि-ल्वादि बाह्य' और अतिरिक्त कहा है। जबकि आचार्यश्री ने 'ल्वी' धातु को 'प्वादि' बताया है। 'जीण' धातु-युजादि गण के 'जुण वयोहानौ' के स्थान पर नन्दी (देवनन्दी) नामक वैयाकरण ने बताया है । 'उङ् कुङ्' इत्यादि धातु जैसे गत्यर्थक हैं, वैसे 'लँङ्' धातु को भी कुछेक गत्यर्थक कहते हैं ।
न्या. सि-: श्रीलावण्यसूरिजी ने 'ल्पीश्' के स्थान पर 'प्लीश्' पाठ किया है, किन्तु उदाहरण में 'ल्पीश्' पाठ को अनुसरे हैं । न्यास में और न्या. तरंग में भी 'ल्पीश्' पाठ ही है, अतः उसका यहाँ स्वीकार किया है ।
'धुंग्ट् कम्पने, धुनुते' । उदा. "पद्मान्तराणि च दुनोति धुनोति पक्षौ" अनुस्वार इत् होने से, 'धोता, धोतुम्' । उदा. 'आराधयन्ति विधिवद् विधुतान्यकृत्याः' । [कल्याणमन्दिर स्तोत्र श्लोक-३४] 'धूग्ट् कम्पने' धातु के 'धूनोति' इत्यादि रूप होते हैं । 'धूगौदितः' ४/४/३८ से यह धातु 'वेट्' होने से 'धोता, धविता' दो रूप होते हैं । 'क्त' प्रत्यय होने पर 'विधूतः' शब्द होता है । ॥४७॥
तीन धातु दीर्घ अकारान्त हैं। 'गूंगूत् च पुरीषोत्सर्गे' । यहाँ दूसरे धातु के अन्त में 'च' अनुबंध रखा है, तथापि प्रथम धातु भ्वादि गण का लेना और वह अनुस्वारेत् है । जबकि दूसरा धातु तुदादि है। यही बात बताने के लिए 'च' का प्रयोग किया है, अत एव अन्यत्र कहीं भी 'च' कार का प्रयोग नहीं किया है । अतः जहाँ अनेक धातुओं के अन्त में 'क' इत्यादि गणसूचक अनुबंध रखे हों वहाँ उन सब धातुओं को 'अदादि' इत्यादि गण के मान लेना ।
_ 'गू, गवति' । अनुस्वार 'इत्' होने से 'इट्' न होकर 'न्यगौषीत्' इत्यादि रूप होंगे । 'गूत्वा' में क्त्वा प्रत्यय है । 'गुंङ् शब्दे' धातु के 'गवते' इत्यादि रूप होते हैं । इस धातु का अद्यतनी में 'धुड् हुस्वाल्लुगनिट:'-४/३/७० से 'सिच्' का लोप होने पर 'न्यगुत' रूप होता है और 'क्त्वा' प्रत्यय होने पर 'गुत्वा' शब्द होता है । जबकि 'गोता, गोतुम्, गोतव्यम्' इत्यादि शब्द 'गूं' और 'गुंङ्' दोनों धातु से होते हैं । ॥ ४८॥
'गूत्', यह धातु कुटादि है, अत: 'कुटादेः'-४/३/१७ से 'सिच्' ङित् होगा, अतः 'सिचि परस्मै समानस्याङिति' ४/३/४४ से 'उ' की वृद्धि नहीं होगी और 'सिच्' के आदि में 'स्ताद्यशितो'४/४/३२ से 'इट्' होगा और 'सः सिजस्तेर्दिस्योः ' ४/३/६५ से 'दि' प्रत्यय के आदि में 'ईत्' होगा, बाद में 'इट ईति' ४/३/७१ से 'सिच्' का लोप होकर, 'धातोरिवर्णो'-२/१/५० से 'ऊ' का 'उ' आदेश होने पर 'न्यगुवीत्' रूप होगा । 'तृच्' इत्यादि प्रत्यय होने पर 'ङित्त्व' के कारण गुण नहीं होगा, अतः 'गुविता, गुवितुम्, गुवितव्यम्' इत्यादि शब्द होंगे । कित् ‘क्त्वा' प्रत्यय होने पर 'उवर्णात्' ४/४/५८ से 'इट्' का निषेध होने पर 'गूत्वा' शब्द होता है ।
'गुंत् पुरीषोत्सर्गे' धातु 'कुटादि' है और अनुस्वार की 'इत्' संज्ञा हुई है, अतः 'इट्' नहीं होगा और 'न्यगुषीत्' इत्यादि रूप होते हैं । 'गुता, गुतुम्, गुतव्यम्, गुत्वा' इत्यादि शब्द भी होते हैं । ॥४९।।
૨૯ Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org