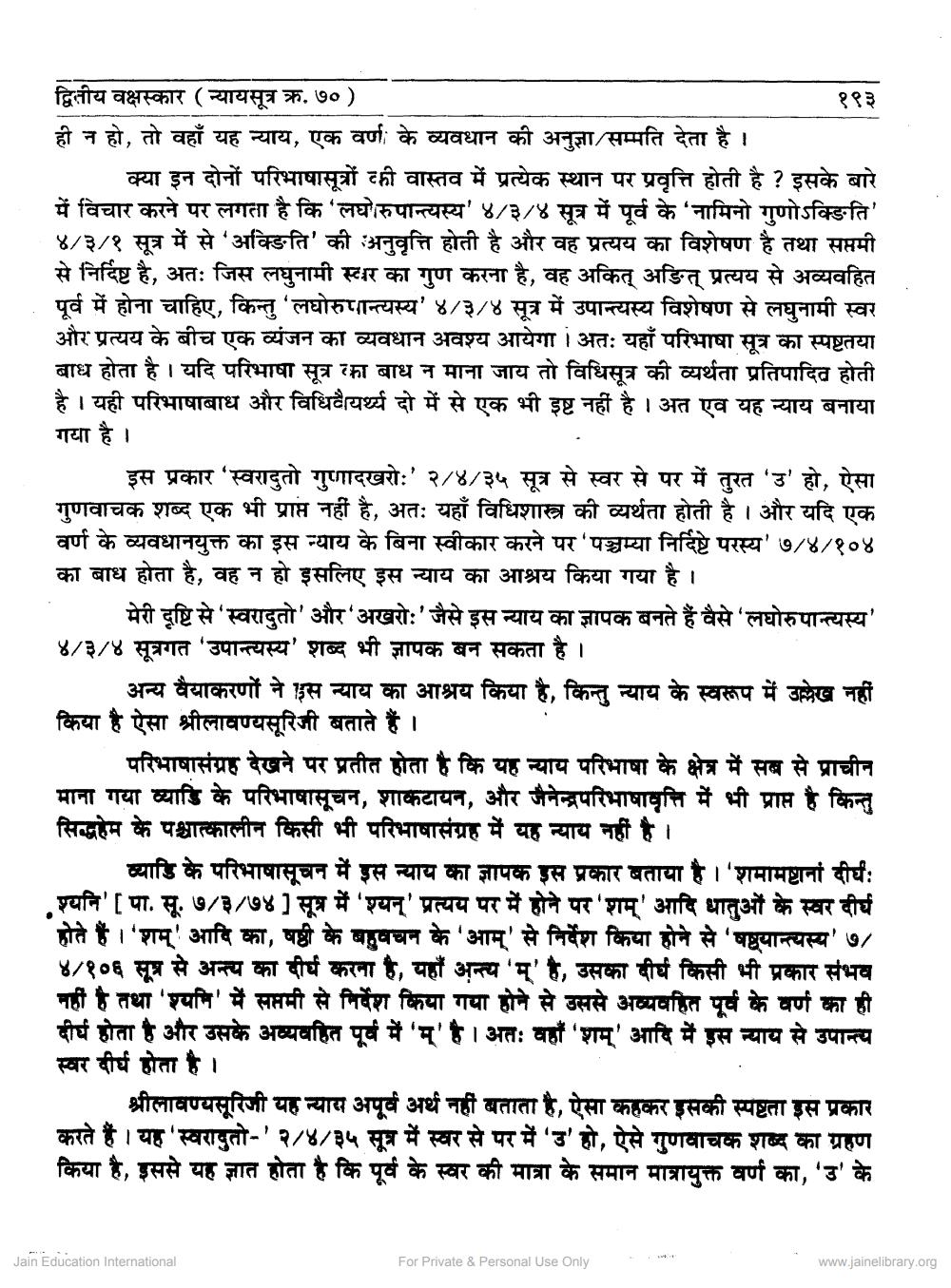________________
१९३
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ७०) ही न हो, तो वहाँ यह न्याय, एक वर्ण के व्यवधान की अनुज्ञा/सम्मति देता है ।
क्या इन दोनों परिभाषासूत्रों की वास्तव में प्रत्येक स्थान पर प्रवृत्ति होती है ? इसके बारे में विचार करने पर लगता है कि 'लघोरुपान्त्यस्य' ४/३/४ सूत्र में पूर्व के 'नामिनो गुणोऽक्ङिति' ४/३/१ सूत्र में से 'अक्ङिति' की अनुवृत्ति होती है और वह प्रत्यय का विशेषण है तथा सप्तमी से निर्दिष्ट है, अतः जिस लघुनामी स्वर का गुण करना है, वह अकित् अङित् प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए, किन्तु 'लघोरुपान्त्यस्य' ४/३/४ सूत्र में उपान्त्यस्य विशेषण से लघुनामी स्वर
और प्रत्यय के बीच एक व्यंजन का व्यवधान अवश्य आयेगा । अतः यहाँ परिभाषा सूत्र का स्पष्टतया बाध होता है। यदि परिभाषा सूत्र का बाध न माना जाय तो विधिसूत्र की व्यर्थता प्रतिपादित होती है । यही परिभाषाबाध और विधिवैयर्थ्य दो में से एक भी इष्ट नहीं है । अत एव यह न्याय बनाया गया है।
इस प्रकार 'स्वरादुतो गुणादखरोः' २/४/३५ सूत्र से स्वर से पर में तुरत 'उ' हो, ऐसा गुणवाचक शब्द एक भी प्राप्त नहीं है, अत: यहाँ विधिशास्त्र की व्यर्थता होती है। और यदि एक वर्ण के व्यवधानयुक्त का इस न्याय के बिना स्वीकार करने पर 'पञ्चम्या निर्दिष्टे परस्य' ७/४/१०४ का बाध होता है, वह न हो इसलिए इस न्याय का आश्रय किया गया है ।
मेरी दृष्टि से 'स्वरादुतो' और 'अखरोः' जैसे इस न्याय का ज्ञापक बनते हैं वैसे 'लघोरुपान्त्यस्य' ४/३/४ सूत्रगत 'उपान्त्यस्य' शब्द भी ज्ञापक बन सकता है ।
अन्य वैयाकरणों ने इस न्याय का आश्रय किया है, किन्तु न्याय के स्वरूप में उल्लेख नहीं किया है ऐसा श्रीलावण्यसूरिजी बताते हैं ।
परिभाषासंग्रह देखने पर प्रतीत होता है कि यह न्याय परिभाषा के क्षेत्र में सब से प्राचीन माना गया व्याडि के परिभाषासूचन, शाकटायन, और जैनेन्द्रपरिभाषावृत्ति में भी प्राप्त है किन्तु सिद्धहेम के पश्चात्कालीन किसी भी परिभाषासंग्रह में यह न्याय नहीं है।
व्याडि के परिभाषासूचन में इस न्याय का ज्ञापक इस प्रकार बताया है। 'शमामष्टानां दीर्घः .श्यनि' [ पा. सू. ७/३/७४ ] सूत्र में 'श्यन्' प्रत्यय पर में होने पर 'शम्' आदि धातुओं के स्वर दीर्घ होते हैं। 'शम्' आदि का, षष्ठी के बहुवचन के 'आम्' से निर्देश किया होने से 'षष्ठयान्त्यस्य' ७/ ४/१०६ सूत्र से अन्त्य का दीर्घ करना है, यहाँ अन्त्य 'म्' है, उसका वीर्घ किसी भी प्रकार संभव नहीं है तथा 'श्यनि' में सप्तमी से निर्देश किया गया होने से उससे अव्यवहित पूर्व के वर्ण का ही दीर्घ होता है और उसके अव्यवहित पूर्व में 'म्' है। अतः वहाँ 'शम्' आदि में इस न्याय से उपान्त्य स्वर दीर्घ होता है।
श्रीलावण्यसूरिजी यह न्याय अपूर्व अर्थ नहीं बताता है, ऐसा कहकर इसकी स्पष्टता इस प्रकार करते है । यह 'स्वरादुतो-' २/४/३५ सूत्र में स्वर से पर में 'उ' हो, ऐसे गुणवाचक शब्द का ग्रहण किया है, इससे यह ज्ञात होता है कि पूर्व के स्वर की मात्रा के समान मात्रायुक्त वर्ण का, 'उ' के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org