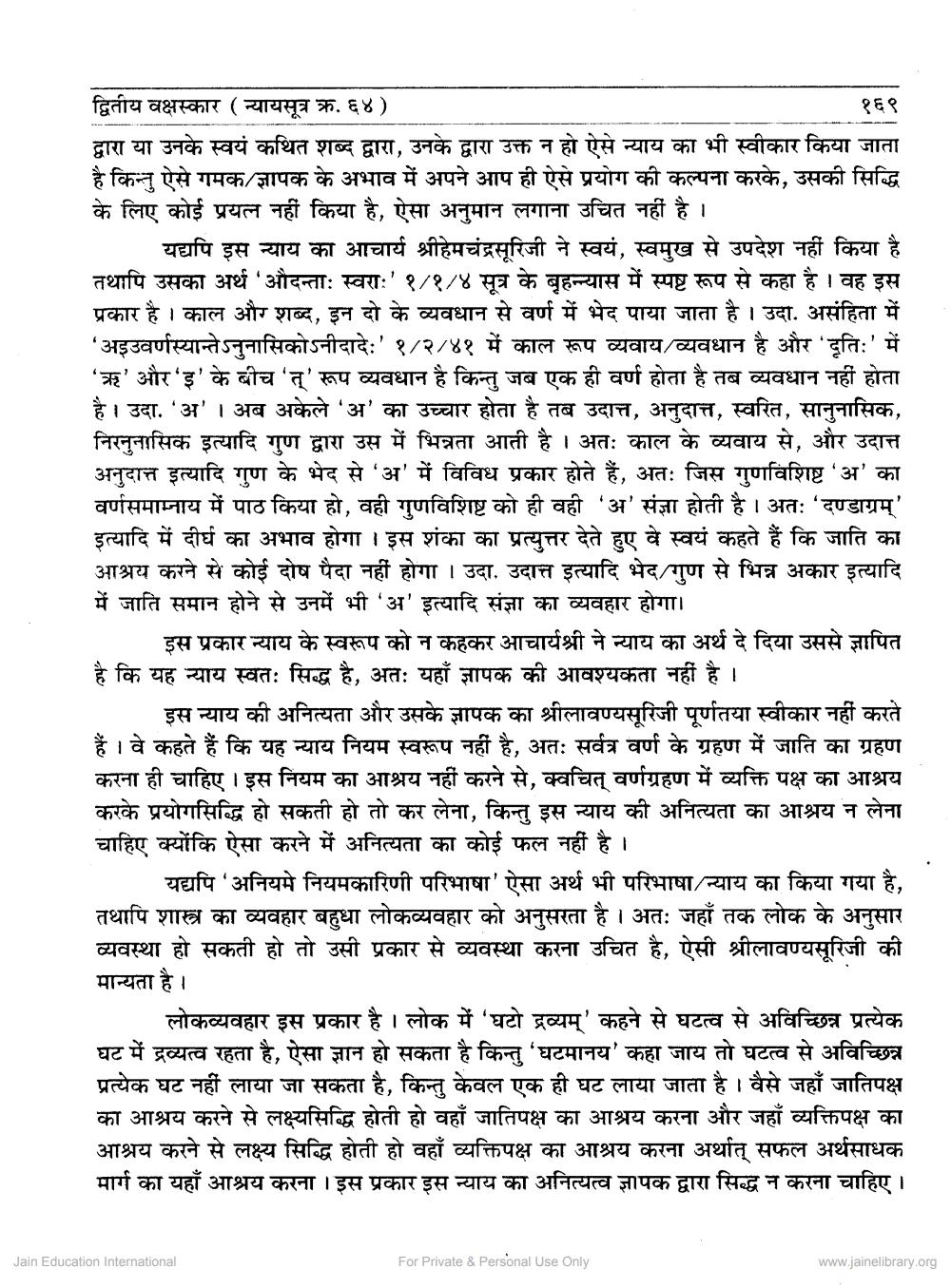________________
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. ६४)
१६९ द्वारा या उनके स्वयं कथित शब्द द्वारा, उनके द्वारा उक्त न हो ऐसे न्याय का भी स्वीकार किया जाता है किन्तु ऐसे गमक/ज्ञापक के अभाव में अपने आप ही ऐसे प्रयोग की कल्पना करके, उसकी सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है, ऐसा अनुमान लगाना उचित नहीं है ।
यद्यपि इस न्याय का आचार्य श्रीहेमचंद्रसूरिजी ने स्वयं, स्वमुख से उपदेश नहीं किया है तथापि उसका अर्थ 'औदन्ताः स्वराः' १/१/४ सूत्र के बृहन्न्यास में स्पष्ट रूप से कहा है । वह इस प्रकार है । काल और शब्द, इन दो के व्यवधान से वर्ण में भेद पाया जाता है। उदा. असंहिता में 'अइउवर्णस्यान्तेऽनुनासिकोऽनीदादेः' १/२/४१ में काल रूप व्यवाय/व्यवधान है और 'दृतिः' में 'ऋ' और 'इ' के बीच 'त्' रूप व्यवधान है किन्तु जब एक ही वर्ण होता है तब व्यवधान नहीं होता है। उदा. 'अ' । अब अकेले 'अ' का उच्चार होता है तब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक इत्यादि गुण द्वारा उस में भिन्नता आती है । अतः काल के व्यवाय से, और उदात्त अनुदात्त इत्यादि गुण के भेद से 'अ' में विविध प्रकार होते हैं, अत: जिस गुणविशिष्ट 'अ' का वर्णसमाम्नाय में पाठ किया हो, वही गुणविशिष्ट को ही वही 'अ' संज्ञा होती है। अत: ‘दण्डाग्रम्' इत्यादि में दीर्घ का अभाव होगा । इस शंका का प्रत्युत्तर देते हुए वे स्वयं कहते हैं कि जाति का आश्रय करने से कोई दोष पैदा नहीं होगा । उदा, उदात्त इत्यादि भेद/गुण से भिन्न अकार इत्यादि में जाति समान होने से उनमें भी 'अ' इत्यादि संज्ञा का व्यवहार होगा।
इस प्रकार न्याय के स्वरूप को न कहकर आचार्यश्री ने न्याय का अर्थ दे दिया उससे ज्ञापित है कि यह न्याय स्वतः सिद्ध है, अतः यहाँ ज्ञापक की आवश्यकता नहीं है ।
इस न्याय की अनित्यता और उसके ज्ञापक का श्रीलावण्यसूरिजी पूर्णतया स्वीकार नहीं करते हैं । वे कहते हैं कि यह न्याय नियम स्वरूप नहीं है, अतः सर्वत्र वर्ण के ग्रहण में जाति का ग्रहण करना ही चाहिए । इस नियम का आश्रय नहीं करने से, क्वचित् वर्णग्रहण में व्यक्ति पक्ष का आश्रय करके प्रयोगसिद्धि हो सकती हो तो कर लेना, किन्तु इस न्याय की अनित्यता का आश्रय न लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में अनित्यता का कोई फल नहीं है।
यद्यपि 'अनियमे नियमकारिणी परिभाषा' ऐसा अर्थ भी परिभाषा/न्याय का किया गया है, तथापि शास्त्र का व्यवहार बहुधा लोकव्यवहार को अनुसरता है। अत: जहाँ तक लोक के अनुसार व्यवस्था हो सकती हो तो उसी प्रकार से व्यवस्था करना उचित है, ऐसी श्रीलावण्यसूरिजी की मान्यता है।
लोकव्यवहार इस प्रकार है । लोक में 'घटो द्रव्यम्' कहने से घटत्व से अविच्छिन्न प्रत्येक घट में द्रव्यत्व रहता है, ऐसा ज्ञान हो सकता है किन्तु 'घटमानय' कहा जाय तो घटत्व से अविच्छिन्न प्रत्येक घट नहीं लाया जा सकता है, किन्तु केवल एक ही घट लाया जाता है। वैसे जहाँ जातिपक्ष का आश्रय करने से लक्ष्यसिद्धि होती हो वहाँ जातिपक्ष का आश्रय करना और जहाँ व्यक्तिपक्ष का आश्रय करने से लक्ष्य सिद्धि होती हो वहाँ व्यक्तिपक्ष का आश्रय करना अर्थात् सफल अर्थसाधक मार्ग का यहाँ आश्रय करना । इस प्रकार इस न्याय का अनित्यत्व ज्ञापक द्वारा सिद्ध न करना चाहिए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org