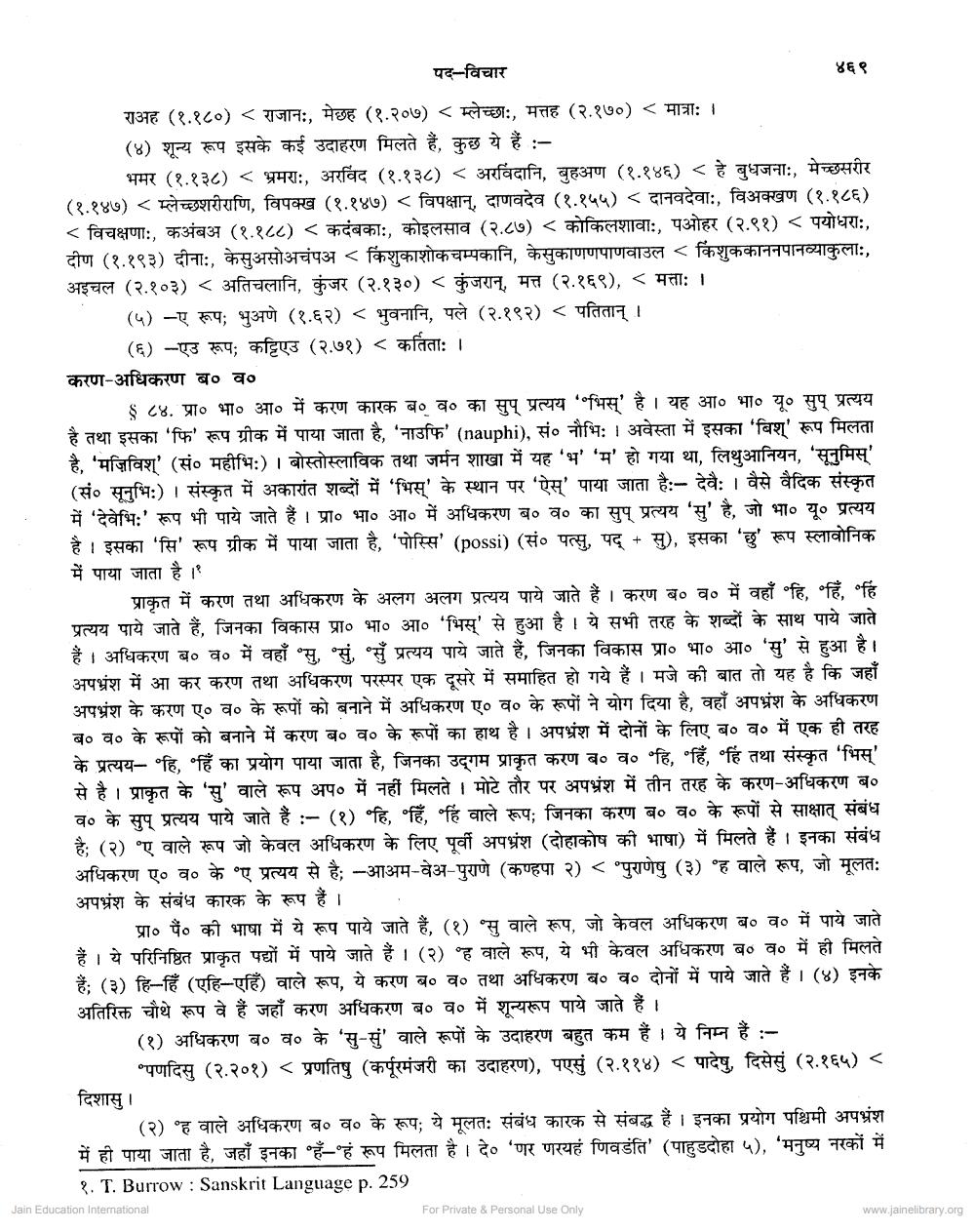________________
पद-विचार
४६९
राअह (१.१८०) < राजानः, मेछह (१.२०७) < म्लेच्छाः , मत्तह (२.१७०) < मात्राः । (४) शून्य रूप इसके कई उदाहरण मिलते हैं, कुछ ये हैं :
भमर (१.१३८) < भ्रमराः, अरविंद (१.१३८) < अरविंदानि, बुहअण (१.१४६) < हे बुधजनाः, मेच्छसरीर (१.१४७) < म्लेच्छशरीराणि, विपक्ख (१.१४७) < विपक्षान्, दाणवदेव (१.१५५) < दानवदेवाः, विअक्खण (१.१८६) < विचक्षणाः, कअंबअ (१.१८८) < कदंबकाः, कोइलसाव (२.८७) < कोकिलशावाः, पओहर (२.९१) < पयोधराः, दीण (१.१९३) दीनाः, केसुअसोअचंपअ < किंशुकाशोकचम्पकानि, केसुकाणणपाणवाउल < किंशुककाननपानव्याकुलाः, अइचल (२.१०३) < अतिचलानि, कुंजर (२.१३०) < कुंजरान्, मत्त (२.१६९), < मत्ताः ।
(५) -ए रूप; भुअणे (१.६२) < भुवनानि, पले (२.१९२) < पतितान् ।
(६) -एउ रूप; कट्टिएउ (२.७१) < कर्तिताः । करण-अधिकरण ब० व०
८४. प्रा० भा० आ० में करण कारक ब० व० का सुप् प्रत्यय "भिस्' है । यह आ० भा० यू. सुप् प्रत्यय है तथा इसका 'फि' रूप ग्रीक में पाया जाता है, 'नाउफि' (nauphi), सं० नौभिः । अवेस्ता में इसका 'बिश्' रूप मिलता है, 'मज़िविश्' (सं० महीभिः) । बोस्तोस्लाविक तथा जर्मन शाखा में यह 'भ' 'म' हो गया था, लिथुआनियन, 'सूनुमिस्' (सं० सूनुभिः) । संस्कृत में अकारांत शब्दों में 'भिस्' के स्थान पर 'ऐस्' पाया जाता है:-देवैः । वैसे वैदिक संस्कृत में 'देवेभिः' रूप भी पाये जाते हैं। प्रा० भा० आ० में अधिकरण ब० व० का सुप् प्रत्यय 'सु' है, जो भा० यू० प्रत्यय है। इसका 'सि' रूप ग्रीक में पाया जाता है, 'पोस्सि' (possi) (सं० पत्सु, पद् + सु), इसका 'छु' रूप स्लावोनिक में पाया जाता है ।
प्राकृत में करण तथा अधिकरण के अलग अलग प्रत्यय पाये जाते हैं। करण ब० व० में वहाँ हि, हिँ, हिं प्रत्यय पाये जाते हैं, जिनका विकास प्रा० भा० आ० 'भिस्' से हुआ है। ये सभी तरह के शब्दों के साथ पाये जाते हैं। अधिकरण ब० व० में वहाँ 'सु, सुं, सुँ प्रत्यय पाये जाते हैं, जिनका विकास प्रा० भा० आ० 'सु' से हुआ है। अपभ्रंश में आ कर करण तथा अधिकरण परस्पर एक दूसरे में समाहित हो गये हैं। मजे की बात तो यह है कि जहाँ अपभ्रंश के करण ए० व० के रूपों को बनाने में अधिकरण ए० व० के रूपों ने योग दिया है, वहाँ अपभ्रंश के अधिकरण ब० व० के रूपों को बनाने में करण ब० व० के रूपों का हाथ है । अपभ्रंश में दोनों के लिए ब० व० में एक ही तरह के प्रत्यय- हि, हिँ का प्रयोग पाया जाता है, जिनका उद्गम प्राकृत करण ब० व० “हि, हिँ, हिं तथा संस्कृत 'भिस्' से है। प्राकृत के 'सु' वाले रूप अप० में नहीं मिलते । मोटे तौर पर अपभ्रंश में तीन तरह के करण-अधिकरण ब० व० के सुप् प्रत्यय पाये जाते हैं :- (१) हि, हिँ, हिं वाले रूप; जिनका करण ब० व० के रूपों से साक्षात् संबंध है; (२) °ए वाले रूप जो केवल अधिकरण के लिए पूर्वी अपभ्रंश (दोहाकोष की भाषा) में मिलते हैं। इनका संबंध अधिकरण ए० व० के °ए प्रत्यय से है; -आअम-वेअ-पुराणे (कण्हपा २) < पुराणेषु (३) °ह वाले रूप, जो मूलतः अपभ्रंश के संबंध कारक के रूप हैं।
प्रा० .० की भाषा में ये रूप पाये जाते हैं, (१) सु वाले रूप, जो केवल अधिकरण ब० व० में पाये जाते हैं। ये परिनिष्ठित प्राकृत पद्यों में पाये जाते हैं । (२) "ह वाले रूप, ये भी केवल अधिकरण ब० व० में ही मिलते हैं; (३) हि-हिँ (एहि-एहिँ) वाले रूप, ये करण ब० व० तथा अधिकरण ब० व० दोनों में पाये जाते हैं । (४) इनके अतिरिक्त चौथे रूप वे हैं जहाँ करण अधिकरण ब० व० में शून्यरूप पाये जाते हैं।
(१) अधिकरण ब० व० के 'सु-सुं' वाले रूपों के उदाहरण बहुत कम हैं। ये निम्न हैं :
"पणदिसु (२.२०१) < प्रणतिषु (कर्पूरमंजरी का उदाहरण), पएसुं (२.११४) < पादेषु, दिसेसुं (२.१६५) < दिशासु।
(२) °ह वाले अधिकरण ब० व० के रूप; ये मूलतः संबंध कारक से संबद्ध हैं । इनका प्रयोग पश्चिमी अपभ्रंश में ही पाया जाता है, जहाँ इनका 'हँ-हं रूप मिलता है। दे० 'णर णरयहं णिवडंति' (पाहुडदोहा ५), 'मनुष्य नरकों में
१. T. Burrow : Sanskrit Language p. 259 Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org