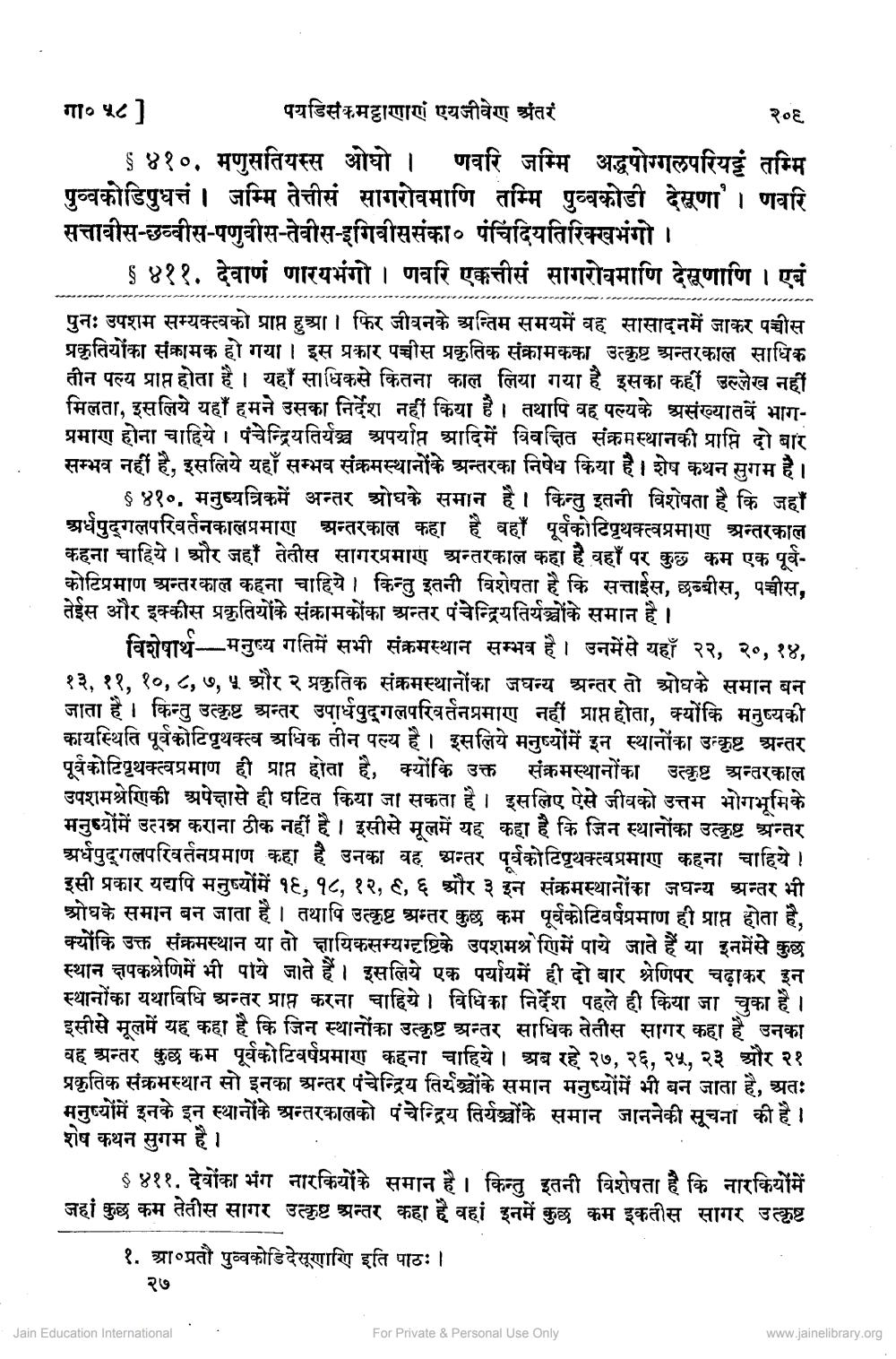________________
गा० ५८ ]
पयसिक मट्ठाणा एयजीवेण अंतरं
२०६
४१०. मणुसतियस्स ओघो । णवरि जम्मि अद्धपोग्गलपरियङ्कं तम्मि पुव्वको डिपुधत्तं । जम्मि तेत्तीसं सागरोवमाणि तम्मि पुव्वकोडी देखणा । णवरि सत्तावीस-छब्वीस- पणुवीस-तेवीस - इगिवीस संका० पंचिदियतिरिक्खभंगो ।
४११. देवाणं णारयभंगो । णवरि एकतीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । एवं
पुनः उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर जीवन के अन्तिम समयमें वह सासादनमें जाकर पच्चीस प्रकृतियोंका संक्रामक हो गया। इस प्रकार पच्चीस प्रकृतिक संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य प्राप्त होता है । यहाँ साधिकसे कितना काल लिया गया है इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, इसलिये यहाँ हमने उसका निर्देश नहीं किया है । तथापि वह पल्य के असंख्यातवें भागप्रमाण होना चाहिये | पंचेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्त आदिमें विवक्षित संक्रमस्थानकी प्राप्ति दो बार सम्भव नहीं है, इसलिये यहाँ सम्भव संक्रमस्थानोंके अन्तरका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है । ४१०. मनुष्यत्रिमें अन्तर प्रोघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ अर्धपुद्गल परिवर्तन कालप्रमाण अन्तरकाल कहा है वहाँ पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिये । और जहाँ तेतीस सागरप्रमाण अन्तरकाल कहा है वहाँ पर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्ताईस, छब्बीस, पच्चीस, तेईस और इक्कीस प्रकृतियोंके संक्रामकोंका अन्तर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों के समान है ।
विशेषार्थ – मनुष्य गतिमें सभी संक्रमस्थान सम्भव है । उनमें से यहाँ २२, २०, १४, १३, ११, १०, ८, ७, ५ और २ प्रकृतिक संक्रमस्थानोंका जघन्य अन्तर तो ओघ के समान बन जाता है । किन्तु उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मनुष्यकी काय स्थिति पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । इसलिये मनुष्यों में इन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्व कोटिपृथक्त्व प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि उक्त संक्रमस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपशमश्रेणिकी अपेक्षा से ही घटित किया जा सकता है। इसलिए ऐसे जीव को उत्तम भोगभूमिके मनुष्यों में उत्पन्न कराना ठीक नहीं है । इसीसे मूलमें यह कहा है कि जिन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है उनका वह अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण कहना चाहिये । इसी प्रकार यद्यपि मनुष्यों में १६, १८, १२, ६, ६ और ३ इन संक्रमस्थानोंका जघन्य अन्तर भी श्रोध के समान बन जाता है । तथापि उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिवर्षप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि उक्त संक्रमस्थान या तो क्षायिकसम्यग्दृष्टिके उपशमश्र णिमें पाये जाते हैं या इनमें से कुछ स्थान क्षपकश्रेणिमें भी पाये जाते हैं । इसलिये एक पर्यायमें ही दो बार श्रेणिपर चढ़ाकर इन स्थानोंका यथाविधि अन्तर प्राप्त करना चाहिये । विधिका निर्देश पहले ही किया जा चुका है इसीसे मूलमें यह कहा है कि जिन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है उनका वह अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिवर्षप्रमाण कहना चाहिये। अब रहे २७, २६, २५, २३ और २१ प्रकृतिक संक्रमस्थान सो इनका अन्तर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों के समान मनुष्यों में भी बन जाता है, अतः मनुष्योंमें इनके इन स्थानों के अन्तरकालको पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों के समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।
1
४११. देवोंका भंग नारकियों के समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि नारकियोंमें जहां कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर कहा है वहां इनमें कुछ कम इकतीस सागर उत्कृष्ट
१. प्रा० प्रतौ पुव्वकोडिदेसूणाणि इति पाठः ।
२७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org