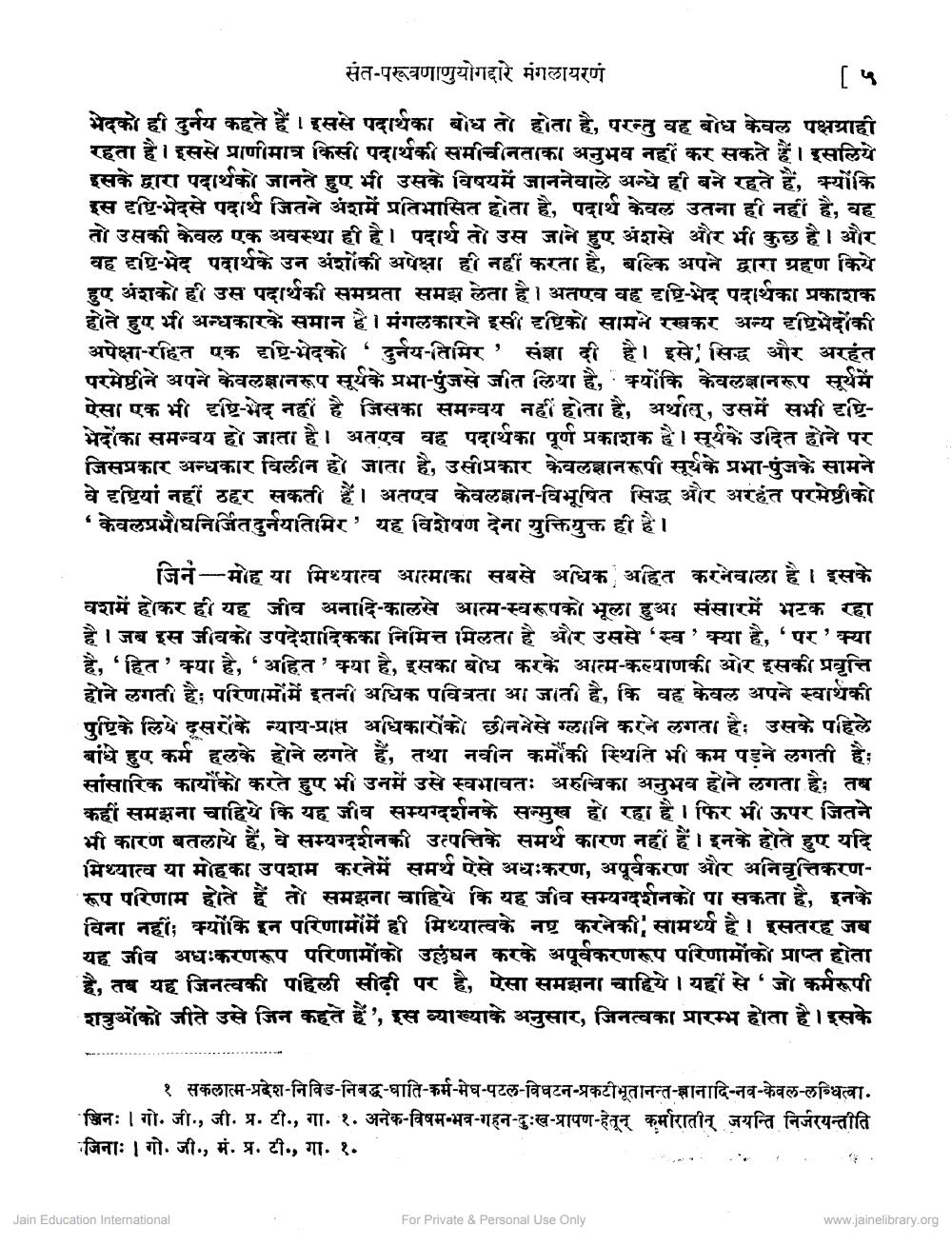________________
संत-परूवणाणुयोगद्दारे मंगलायरणं
[ ५
भेदको ही दुर्नय कहते हैं । इससे पदार्थका बोध तो होता है, परन्तु वह बोध केवल पक्षग्राही रहता है। इससे प्राणीमात्र किसी पदार्थकी समीचीनताका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिये इसके द्वारा पदार्थको जानते हुए भी उसके विषय में जाननेवाले अन्धे ही बने रहते हैं, क्योंकि इस दृष्टि-भेदले पदार्थ जितने अंशमें प्रतिभासित होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है, वह तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंशसे और भी कुछ है । और वह दृष्टि-भेद पदार्थके उन अंशों की अपेक्षा ही नहीं करता है, बल्कि अपने द्वारा ग्रहण किये हुए अंशको ही उस पदार्थकी समग्रता समझ लेता है । अतएव वह दृष्टि-भेद पदार्थका प्रकाशक होते हुए भी अन्धकारके समान है। मंगलकारने इसी दृष्टिको सामने रखकर अन्य दृष्टिभेदों की अपेक्षा-रहित एक दृष्टि-भेदको दुर्न संज्ञा दी है। इसे सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीने अपने केवलज्ञानरूप सूर्यके प्रभा-पुंजसे जीत लिया है, क्योंकि केवलज्ञानरूप सूर्य में ऐसा एक भी दृष्टि-भेद नहीं है जिसका समन्वय नहीं होता है, अर्थात्, उसमें सभी दृष्टिभेदों का समन्वय हो जाता है । अतएव वह पदार्थका पूर्ण प्रकाशक है। सूर्यके उदित होने पर जिसप्रकार अन्धकार विलीन हो जाता है, उसीप्रकार केवलज्ञानरूपी सूर्य के प्रभा-पुंजके सामने वे दृष्टियां नहीं ठहर सकती हैं। अतएव केवलज्ञान-विभूषित सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी को ' केवलप्रभौघनिर्जित दुर्नयतिमिर' यह विशेषण देना युक्तियुक्त ही है ।
"
9
जिनं – मोह या मिथ्यात्व आत्माका सबसे अधिक अहित करनेवाला है । इसके वशमें होकर ही यह जीव अनादि कालसे आत्म-स्वरूपको भूला हुआ संसारमें भटक रहा है । जब इस जीवको उपदेशादिकका निमित्त मिलता है और उससे 'स्व' क्या है, ' पर ' क्या है, 'हित' क्या है, 'अहित ' क्या है, इसका बोध करके आत्म-कल्याणकी ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है; परिणामों में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, कि वह केवल अपने स्वार्थकी पुष्टिके लिये दूसरोंके न्याय प्राप्त अधिकारोंको छीननेसे ग्लानि करने लगता है; उसके पहिले बांधे हुए : कर्म हलके होने लगते हैं, तथा नवीन कर्मों की स्थिति भी कम पड़ने लगती है: सांसारिक कार्योंको करते हुए भी उनमें उसे स्वभावतः अरुचिका अनुभव होने लगता है; तब कहीं समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनके सन्मुख हो रहा है । फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाये हैं, वे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं । इनके होते हुए यदि मिथ्यात्व या मोहका उपशम करनेमें समर्थ ऐसे अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनको पा सकता है, इनके विना नहीं; क्योंकि इन परिणामों में ही मिथ्यात्वके नष्ट करनेकी, सामर्थ्य है । इसतरह जब यह जीव अधःकरणरूप परिणामोंको उल्लंघन करके अपूर्वकरणरूप परिणामोंको प्राप्त होता है, तब यह जिनत्वकी पहिली सीढ़ी पर है, ऐसा समझना चाहिये । यहीं से ' जो कर्मरूपी शत्रुओं को जीते उसे जिन कहते हैं, इस व्याख्याके अनुसार, जिनत्वका प्रारम्भ होता है। इसके
१ सकलात्म- प्रदेश - निविड-निबद्ध-घाति-कर्म-मेघ- पटल-विघटन - प्रकटीभूतानन्त - ज्ञानादि - नव- केवल- लब्धित्वा. `जिनः । गो. जी., जी. प्र. टी., गा. १. अनेक विषम-भव - गहन -दुःख-प्रापण - हेतून् कुर्मारातीन् जयन्ति निर्जरयन्तीति जिनाः । गो. जी., मं. प्र. टी., गा. १.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org