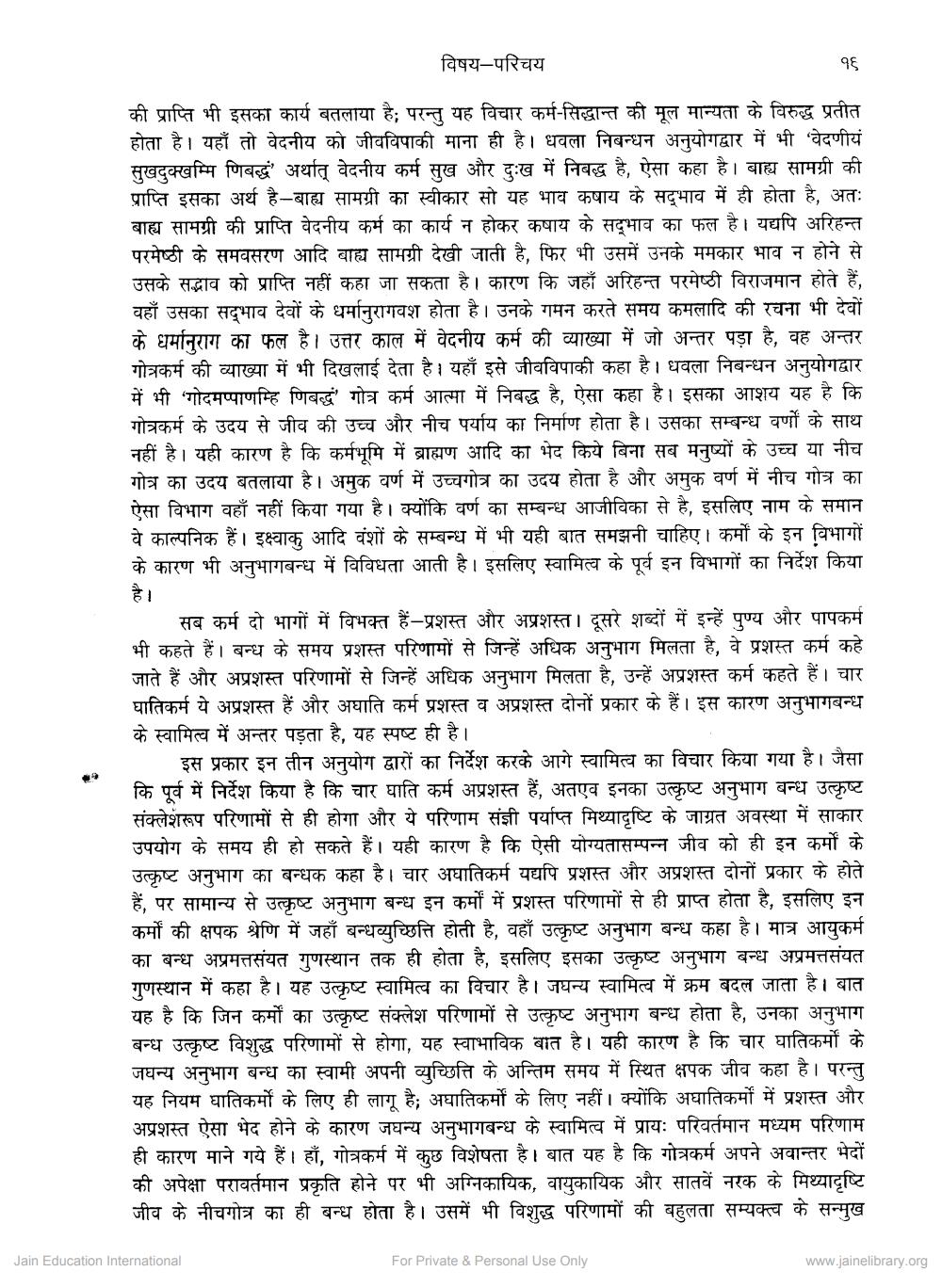________________
विषय-परिचय
की प्राप्ति भी इसका कार्य बतलाया है; परन्तु यह विचार कर्म-सिद्धान्त की मूल मान्यता के विरुद्ध प्रतीत होता है। यहाँ तो वेदनीय को जीवविपाकी माना ही है। धवला निबन्धन अनुयोगद्वार में भी 'वेदणीयं सुखदुक्खम्मिणिबद्धं' अर्थात् वेदनीय कर्म सुख और दुःख में निबद्ध है, ऐसा कहा है। बाह्य सामग्री की प्राप्ति इसका अर्थ है-बाह्य सामग्री का स्वीकार सो यह भाव कषाय के सद्भाव में ही होता है, अतः बाह्य सामग्री की प्राप्ति वेदनीय कर्म का कार्य न होकर कषाय के सद्भाव का फल है। यद्यपि अरिहन्त परमेष्ठी के समवसरण आदि बाह्य सामग्री देखी जाती है, फिर भी उसमें उनके ममकार भाव न होने से उसके सद्भाव को प्राप्ति नहीं कहा जा सकता है। कारण कि जहाँ अरिहन्त परमेष्ठी विराजमान होते हैं, वहाँ उसका सद्भाव देवों के धर्मानुरागवश होता है। उनके गमन करते समय कमलादि की रचना भी देवों के धर्मानुराग का फल है। उत्तर काल में वेदनीय कर्म की व्याख्या में जो अन्तर पड़ा है, वह अन्तर गोत्रकर्म की व्याख्या में भी दिखलाई देता है। यहाँ इसे जीवविपाकी कहा है। धवला निबन्धन अनुयोगद्वार में भी 'गोदमप्पाणम्हि णिबद्धं' गोत्र कर्म आत्मा में निबद्ध है, ऐसा कहा है। इसका आशय यह है कि गोत्रकर्म के उदय से जीव की उच्च और नीच पर्याय का निर्माण होता है। उसका सम्बन्ध वर्गों के साथ नहीं है। यही कारण है कि कर्मभूमि में ब्राह्मण आदि का भेद किये बिना सब मनुष्यों के उच्च या नीच गोत्र का उदय बतलाया है। अमुक वर्ण में उच्चगोत्र का उदय होता है और अमुक वर्ण में नीच गोत्र का ऐसा विभाग वहाँ नहीं किया गया है। क्योंकि वर्ण का सम्बन्ध आजीविका से है, इसलिए नाम के समान वे काल्पनिक हैं। इक्ष्वाकु आदि वंशों के सम्बन्ध में भी यही बात समझनी चाहिए। कर्मों के इन विभागों के कारण भी अनुभागबन्ध में विविधता आती है। इसलिए स्वामित्व के पूर्व इन विभागों का निर्देश किया
सब कर्म दो भागों में विभक्त हैं-प्रशस्त और अप्रशस्त। दूसरे शब्दों में इन्हें पूण्य और पापकर्म भी कहते हैं। बन्ध के समय प्रशस्त परिणामों से जिन्हें अधिक अनुभाग मिलता है, वे प्रशस्त कर्म कहे जाते हैं और अप्रशस्त परिणामों से जिन्हें अधिक अनुभाग मिलता है, उन्हें अप्रशस्त कर्म कहते हैं। चार घातिकर्म ये अप्रशस्त हैं और अघाति कर्म प्रशस्त व अप्रशस्त दोनों प्रकार के हैं। इस कारण अनुभागबन्ध के स्वामित्व में अन्तर पड़ता है, यह स्पष्ट ही है।
इस प्रकार इन तीन अनुयोग द्वारों का निर्देश करके आगे स्वामित्व का विचार किया गया है। जैसा कि पूर्व में निर्देश किया है कि चार घाति कर्म अप्रशस्त हैं, अतएव इनका उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामों से ही होगा और ये परिणाम संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि के जाग्रत अवस्था में साकार उपयोग के समय ही हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी योग्यतासम्पन्न जीव को ही इन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का बन्धक कहा है। चार अघातिकर्म यद्यपि प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के होते हैं, पर सामान्य से उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध इन कर्मों में प्रशस्त परिणामों से ही प्राप्त होता है, इसलिए इन कर्मों की क्षपक श्रेणि में जहाँ बन्धव्युच्छित्ति होती है, वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध कहा है। मात्र आयुकर्म का बन्ध अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए इसका उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में कहा है। यह उत्कृष्ट स्वामित्व का विचार है। जघन्य स्वामित्व में क्रम बदल जाता है। बात यह है कि जिन कर्मों का उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, उनका अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से होगा, यह स्वाभाविक बात है। यही कारण है कि चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभाग बन्ध का स्वामी अपनी व्युच्छित्ति के अन्तिम समय में स्थित क्षपक जीव कहा है। परन्तु यह नियम घातिकर्मों के लिए ही लागू है; अघातिकर्मों के लिए नहीं। क्योंकि अघातिकर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसा भेद होने के कारण जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामित्व में प्रायः परिवर्तमान मध्यम परिणाम ही कारण माने गये हैं। हाँ, गोत्रकर्म में कुछ विशेषता है। बात यह है कि गोत्रकर्म अपने अवान्तर भेदों की अपेक्षा परावर्तमान प्रकृति होने पर भी अग्निकायिक, वायुकायिक और सातवें नरक के मिथ्यादृष्टि जीव के नीचगोत्र का ही बन्ध होता है। उसमें भी विशुद्ध परिणामों की बहुलता सम्यक्त्व के सन्मुख
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org