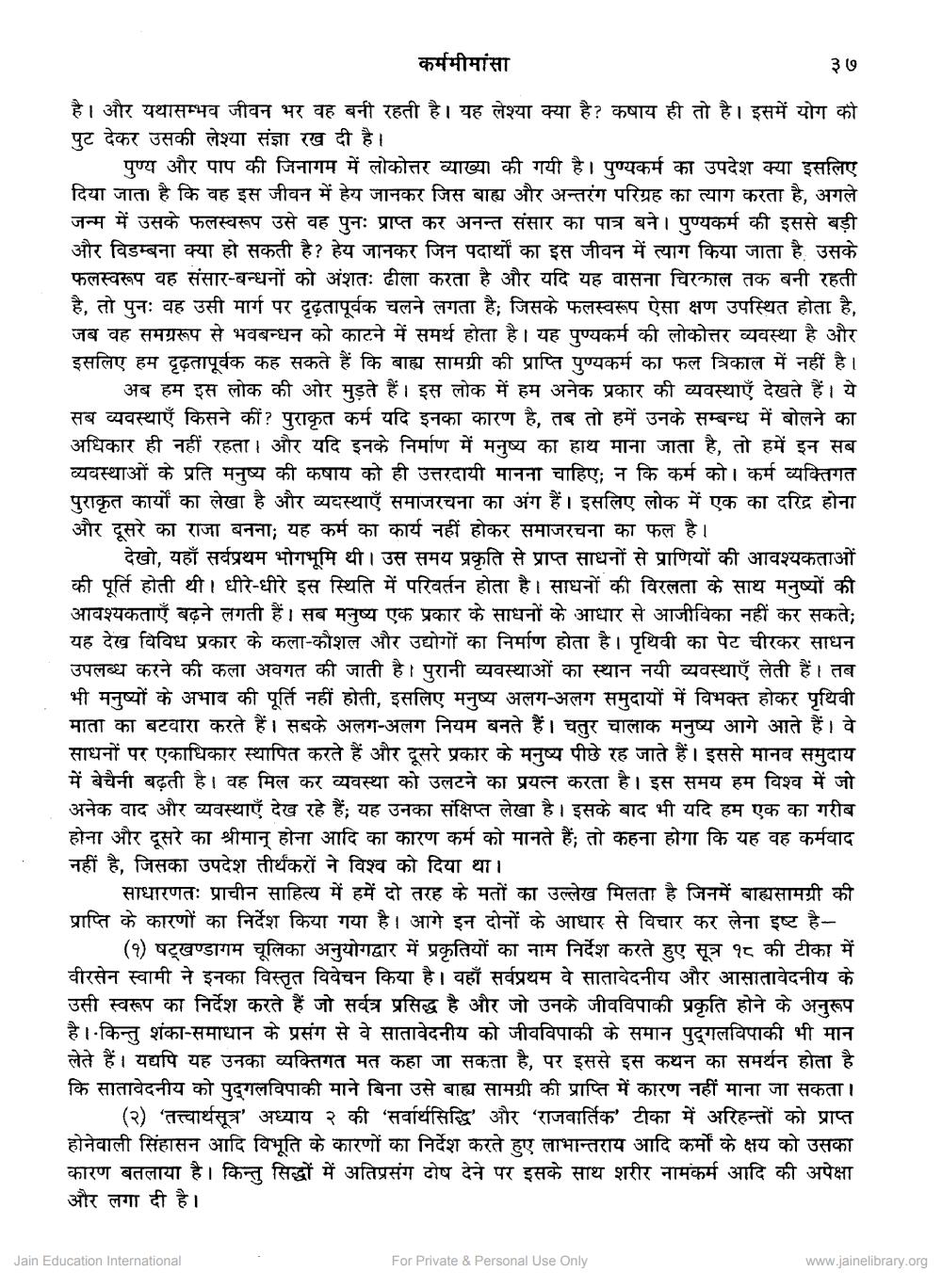________________
कर्ममीमांसा
३७
है। और यथासम्भव जीवन भर वह बनी रहती है। यह लेश्या क्या है? कषाय ही तो है। इसमें योग को पुट देकर उसकी लेश्या संज्ञा रख दी है।
पुण्य और पाप की जिनागम में लोकोत्तर व्याख्या की गयी है। पुण्यकर्म का उपदेश क्या इसलिए दिया जाता है कि वह इस जीवन में हेय जानकर जिस बाह्य और अन्तरंग परिग्रह का त्याग करता है, अगले जन्म में उसके फलस्वरूप उसे वह पुनः प्राप्त कर अनन्त संसार का पात्र बने। पुण्यकर्म की इससे बड़ी
और विडम्बना क्या हो सकती है? हेय जानकर जिन पदार्थों का इस जीवन में त्याग किया जाता है. उसके फलस्वरूप वह संसार-बन्धनों को अंशतः ढीला करता है और यदि यह वासना चिरकाल तक बनी रहती है, तो पुनः वह उसी मार्ग पर दृढ़ सापूर्वक चलने लगता है; जिसके फलस्वरूप ऐसा क्षण उपस्थित होता है, जब वह समग्ररूप से भवबन्धन को काटने में समर्थ होता है। यह पुण्यकर्म की लोकोत्तर व्यवस्था है और इसलिए हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि बाह्य सामग्री की प्राप्ति पुण्यकर्म का फल त्रिकाल में नहीं है।
__अब हम इस लोक की ओर मुड़ते हैं। इस लोक में हम अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ देखते हैं। ये सब व्यवस्थाएँ किसने की? पुराकृत कर्म यदि इनका कारण है, तब तो हमें उनके सम्बन्ध में बोलने का अधिकार ही नहीं रहता। और यदि इनके निर्माण में मनुष्य का हाथ माना जाता है, तो हमें इन सब व्यवस्थाओं के प्रति मनुष्य की कषाय को ही उत्तरदायी मानना चाहिए, न कि कर्म को। कर्म व्यकि पुराकृत कार्यों का लेखा है और व्यवस्थाएँ समाजरचना का अंग हैं। इसलिए लोक में एक का दरिद्र होना और दूसरे का राजा बनना; यह कर्म का कार्य नहीं होकर समाजरचना का फल है।
देखो, यहाँ सर्वप्रथम भोगभूमि थी। उस समय प्रकृति से प्राप्त साधनों से प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन होता है। साधनों की विरलता के साथ मनुष्यों की आवश्यकताएँ बढ़ने लगती हैं। सब मनुष्य एक प्रकार के साधनों के आधार से आजीविका नहीं कर सकते; यह देख विविध प्रकार के कला-कौशल और उद्योगों का निर्माण होता है। पृथिवी का पेट चीरकर साधन उपलब्ध करने की कला अवगत की जाती है। पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान नयी व्यवस्थाएँ लेती हैं। तब भी मनुष्यों के अभाव की पूर्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य अलग-अलग समुदायों में विभक्त होकर पृथिवी माता का बटवारा करते हैं। सबके अलग-अलग नियम बनते हैं। चतुर चालाक मनुष्य आगे आते हैं। वे साधनों पर एकाधिकार स्थापित करते हैं और दूसरे प्रकार के मनुष्य पीछे रह जाते हैं। इससे मानव समुदाय में बेचैनी बढ़ती है। वह मिल कर व्यवस्था को उलटने का प्रयत्न करता है। इस समय हम विश्व में जो अनेक वाद और व्यवस्थाएँ देख रहे हैं; यह उनका संक्षिप्त लेखा है। इसके बाद भी यदि हम एक का गरीब होना और दूसरे का श्रीमान् होना आदि का कारण कर्म को मानते हैं, तो कहना होगा कि यह वह कर्मवाद नहीं है, जिसका उपदेश तीर्थंकरों ने विश्व को दिया था।
साधारणतः प्राचीन साहित्य में हमें दो तरह के मतों का उल्लेख मिलता है जिनमें बाह्यसामग्री की प्राप्ति के कारणों का निर्देश किया गया है। आगे इन दोनों के आधार से विचार कर लेना इष्ट है
(१) षटखण्डागम चूलिका अनुयोगद्वार में प्रकृतियों का नाम निर्देश करते हुए सूत्र १८ की टीका में वीरसेन स्वामी ने इनका विस्तृत विवेचन किया है। वहाँ सर्वप्रथम वे सातावेदनीय और आसातावेदनीय के उसी स्वरूप का निर्देश करते हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो उनके जीवविपाकी प्रकृति होने के अनुरूप है। किन्तु शंका-समाधान के प्रसंग से वे सातावेदनीय को जीवविपाकी के समान पुद्गलविपाकी भी मान लेते हैं। यद्यपि यह उनका व्यक्तिगत मत कहा जा सकता है, पर इससे इस कथन का समर्थन है कि सातावेदनीय को पुद्गलविपाकी माने बिना उसे बाह्य सामग्री की प्राप्ति में कारण नहीं माना जा सकता।
(२) 'तत्त्वार्थसूत्र' अध्याय २ की 'सर्वार्थसिद्धि' और 'राजवार्तिक' टीका में अरिहन्तों को प्राप्त होनेवाली सिंहासन आदि विभूति के कारणों का निर्देश करते हुए लाभान्तराय आदि कर्मों के क्षय को उसका कारण बतलाया है। किन्तु सिद्धों में अतिप्रसंग दोष देने पर इसके साथ शरीर नामकर्म आदि की अपेक्षा और लगा दी है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org