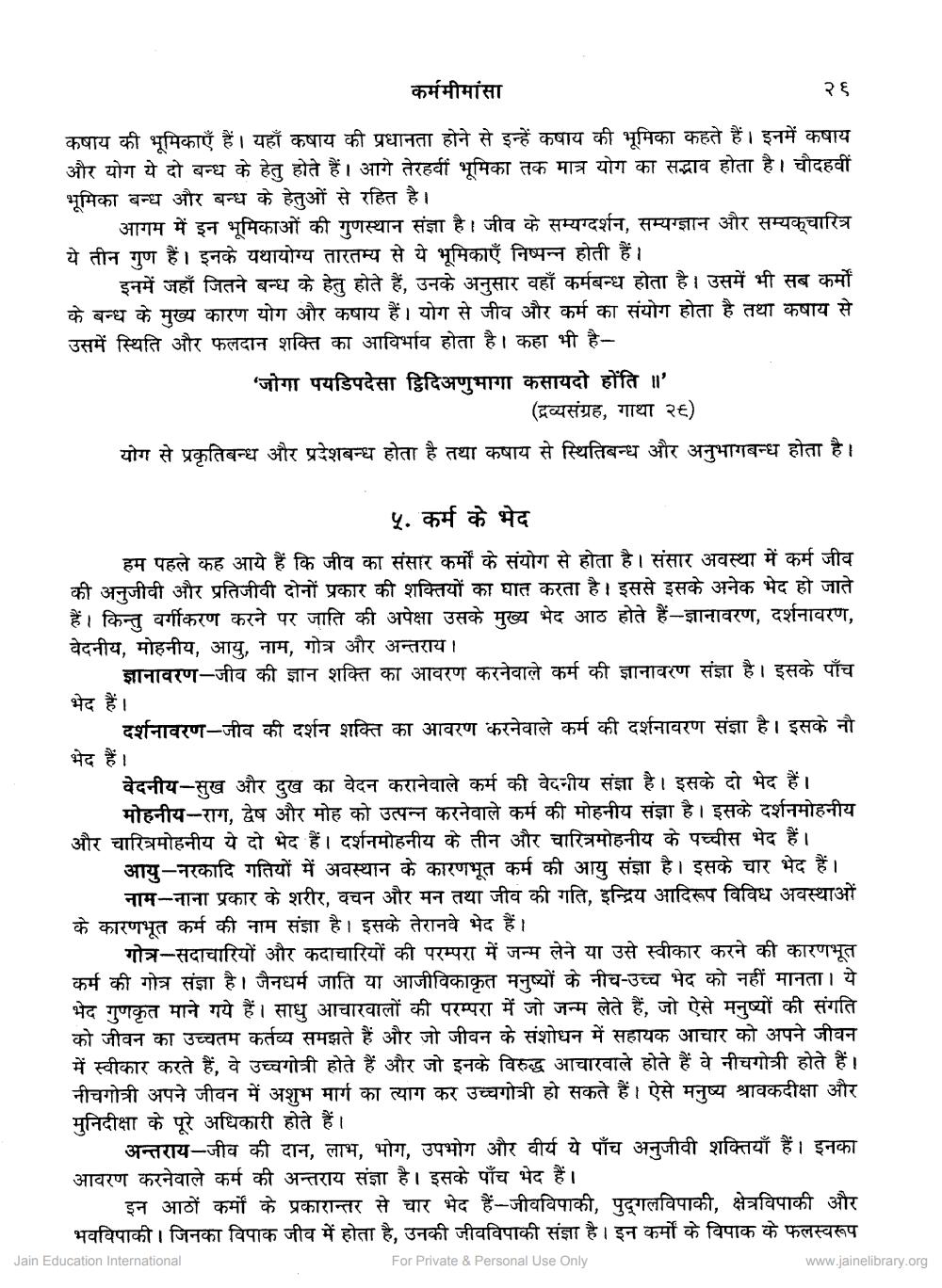________________
कर्ममीमांसा
२६
कषाय की भूमिकाएँ हैं । यहाँ कषाय की प्रधानता होने से इन्हें कषाय की भूमिका कहते हैं। इनमें कषाय और योग ये दो बन्ध के हेतु होते हैं। आगे तेरहवीं भूमिका तक मात्र योग का सद्भाव होता है। चौदहवीं भूमिका बन्ध और बन्ध के हेतुओं से रहित है ।
आगम में इन भूमिकाओं की गुणस्थान संज्ञा है । जीव के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीन गुण हैं । इनके यथायोग्य तारतम्य से ये भूमिकाएँ निष्पन्न होती हैं ।
इनमें जहाँ जितने बन्ध के हेतु होते हैं, उनके अनुसार वहाँ कर्मबन्ध होता है । उसमें भी सब कर्मों के बन्ध के मुख्य कारण योग और कषाय हैं। योग से जीव और कर्म का संयोग होता है तथा कषाय से उसमें स्थिति और फलदान शक्ति का आविर्भाव होता है। कहा भी है
'जोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ( द्रव्यसंग्रह, गाथा २६)
योग से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाय से स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध होता है।
५. कर्म के भेद
हम पहले कह आये हैं कि जीव का संसार कर्मों के संयोग से होता है। संसार अवस्था में कर्म जीव की अनुजीवी और प्रतिजीवी दोनों प्रकार की शक्तियों का घात करता है। इससे इसके अनेक भेद हो जाते हैं । किन्तु वर्गीकरण करने पर जाति की अपेक्षा उसके मुख्य भेद आठ होते हैं-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ।
ज्ञानावरण-जीव की ज्ञान शक्ति का आवरण करनेवाले कर्म की ज्ञानावरण संज्ञा है। इसके पाँच
दर्शनावरण-जीव की दर्शन शक्ति का आवरण करनेवाले कर्म की दर्शनावरण संज्ञा है। इसके नौ
वेदनीय-सुख और दुख का वेदन करानेवाले कर्म की वेदनीय संज्ञा है। इसके दो भेद हैं। मोहनीय - राग, द्वेष और मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्म की मोहनीय संज्ञा है। इसके दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दो भेद हैं। दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्रमोहनीय के पच्चीस भेद हैं।
भेद हैं।
भेद हैं।
आयु - नरकादि गतियों में अवस्थान के कारणभूत कर्म की आयु संज्ञा है। इसके चार भेद हैं । नाम - नाना प्रकार के शरीर, वचन और मन तथा जीव की गति, इन्द्रिय आदिरूप विविध अवस्थाओं के कारणभूत कर्म की नाम संज्ञा है। इसके तेरानवे भेद हैं।
गोत्र - सदाचारियों और कदाचारियों की परम्परा में जन्म लेने या उसे स्वीकार करने की कारणभूत कर्म की गोत्र संज्ञा | जैनधर्म जाति या आजीविकाकृत मनुष्यों के नीच उच्च भेद को नहीं मानता। ये भेद गुणकृत माने गये हैं । साधु आचारवालों की परम्परा में जो जन्म लेते हैं, जो ऐसे मनुष्यों की संगति को जीवन का उच्चतम कर्तव्य समझते हैं और जो जीवन के संशोधन में सहायक आचार को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उच्चगोत्री होते हैं और जो इनके विरुद्ध आचारवाले होते हैं वे नीचगोत्री होते हैं । नीचगोत्री अपने जीवन में अशुभ मार्ग का त्याग कर उच्चगोत्री हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य श्रावकदीक्षा और मुनिदीक्षा के पूरे अधिकारी होते हैं। 1
अन्तराय - जीव की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये पाँच अनुजीवी शक्तियाँ हैं । इनका आवरण करनेवाले कर्म की अन्तराय संज्ञा है। इसके पाँच भेद हैं ।
इन आठों कर्मों के प्रकारान्तर से चार भेद हैं- जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी, क्षेत्रविपाकी और भवविपाकी । जिनका विपाक जीव में होता है, उनकी जीवविपाकी संज्ञा है। इन कर्मों के विपाक के फलस्वरूप For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org