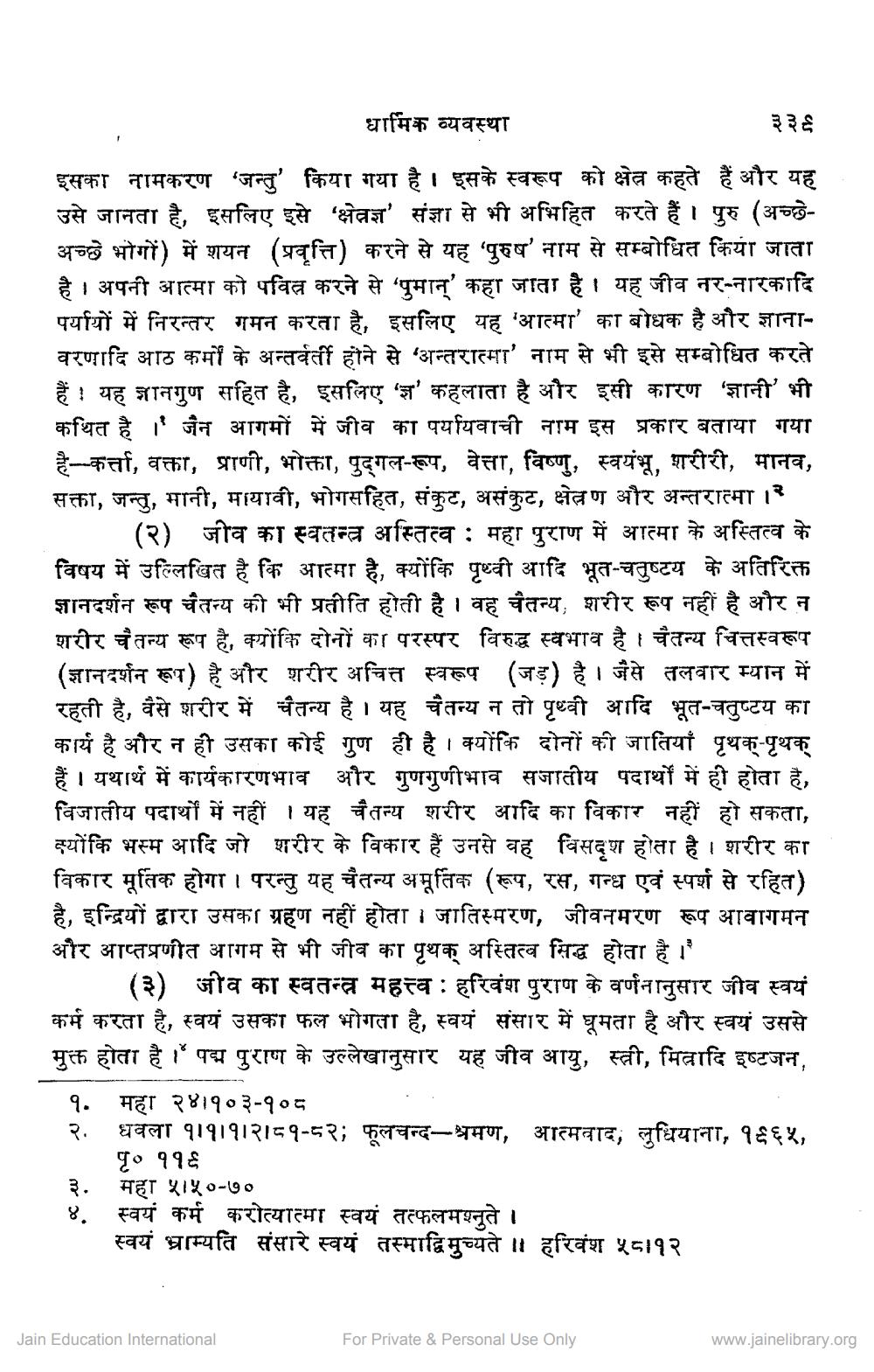________________
धार्मिक व्यवस्था इसका नामकरण 'जन्तु' किया गया है। इसके स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जानता है, इसलिए इसे 'क्षेत्रज्ञ' संज्ञा से भी अभिहित करते हैं । पुरु (अच्छेअच्छे भोगों) में शयन (प्रवृत्ति) करने से यह 'पुरुष' नाम से सम्बोधित किया जाता है। अपनी आत्मा को पवित्र करने से 'पुमान्' कहा जाता है। यह जीव नर-नारकादि पर्यायों में निरन्तर गमन करता है, इसलिए यह 'आत्मा' का बोधक है और ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के अन्तर्वर्ती होने से 'अन्तरात्मा' नाम से भी इसे सम्बोधित करते हैं ! यह ज्ञानगुण सहित है, इसलिए 'ज्ञ' कहलाता है और इसी कारण 'ज्ञानी' भी कथित है ।' जैन आगमों में जीव का पर्यायवाची नाम इस प्रकार बताया गया है-कर्ता, वक्ता, प्राणी, भोक्ता, पुद्गल-रूप, वेत्ता, विष्णु, स्वयंभू, शरीरी, मानव, सक्ता, जन्तु, मानी, मायावी, भोगसहित, संकुट, असंकुट, क्षेत्रण और अन्तरात्मा ।।
(२) जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व : महा पुराण में आत्मा के अस्तित्व के विषय में उल्लिखित है कि आत्मा है, क्योंकि पृथ्वी आदि भूत-चतुष्टय के अतिरिक्त ज्ञानदर्शन रूप चैतन्य की भी प्रतीति होती है । वह चैतन्य, शरीर रूप नहीं है और न शरीर चैतन्य रूप है, क्योंकि दोनों का परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। चैतन्य चित्तस्वरूप (ज्ञानदर्शन रूप) है और शरीर अचित्त स्वरूप (जड़) है । जैसे तलवार म्यान में रहती है, वैसे शरीर में चैतन्य है । यह चैतन्य न तो पृथ्वी आदि भूत-चतुष्टय का कार्य है और न ही उसका कोई गुण ही है । क्योंकि दोनों की जातियाँ पृथक्-पृथक् हैं । यथार्थ में कार्यकारणभाव और गुणगुणीभाव सजातीय पदार्थों में ही होता है, विजातीय पदार्थों में नहीं । यह चैतन्य शरीर आदि का विकार नहीं हो सकता, क्योंकि भस्म आदि जो शरीर के विकार हैं उनसे वह विसदृश होता है । शरीर का विकार मूर्तिक होगा। परन्तु यह चैतन्य अमूर्तिक (रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श से रहित) है, इन्द्रियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता । जातिस्मरण, जीवनमरण रूप आवागमन और आप्तप्रणीत आगम से भी जीव का पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है।
(३) जीव का स्वतन्त्र महत्त्व : हरिवंश पुराण के वर्णनानुसार जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में घूमता है और स्वयं उससे मुक्त होता है। पद्म पुराण के उल्लेखानुसार यह जीव आयु, स्त्री, मित्रादि इष्टजन, १. महा २४।१०३-१०८
धवला १।१।१।२।८१-८२; फूलचन्द-श्रमण, आत्मवाद, लुधियाना, १६६५,
पृ० ११६ ३. महा ५१५०-७० ४. स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते ।
स्वयं भ्राम्यति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥ हरिवंश ५८/१२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org