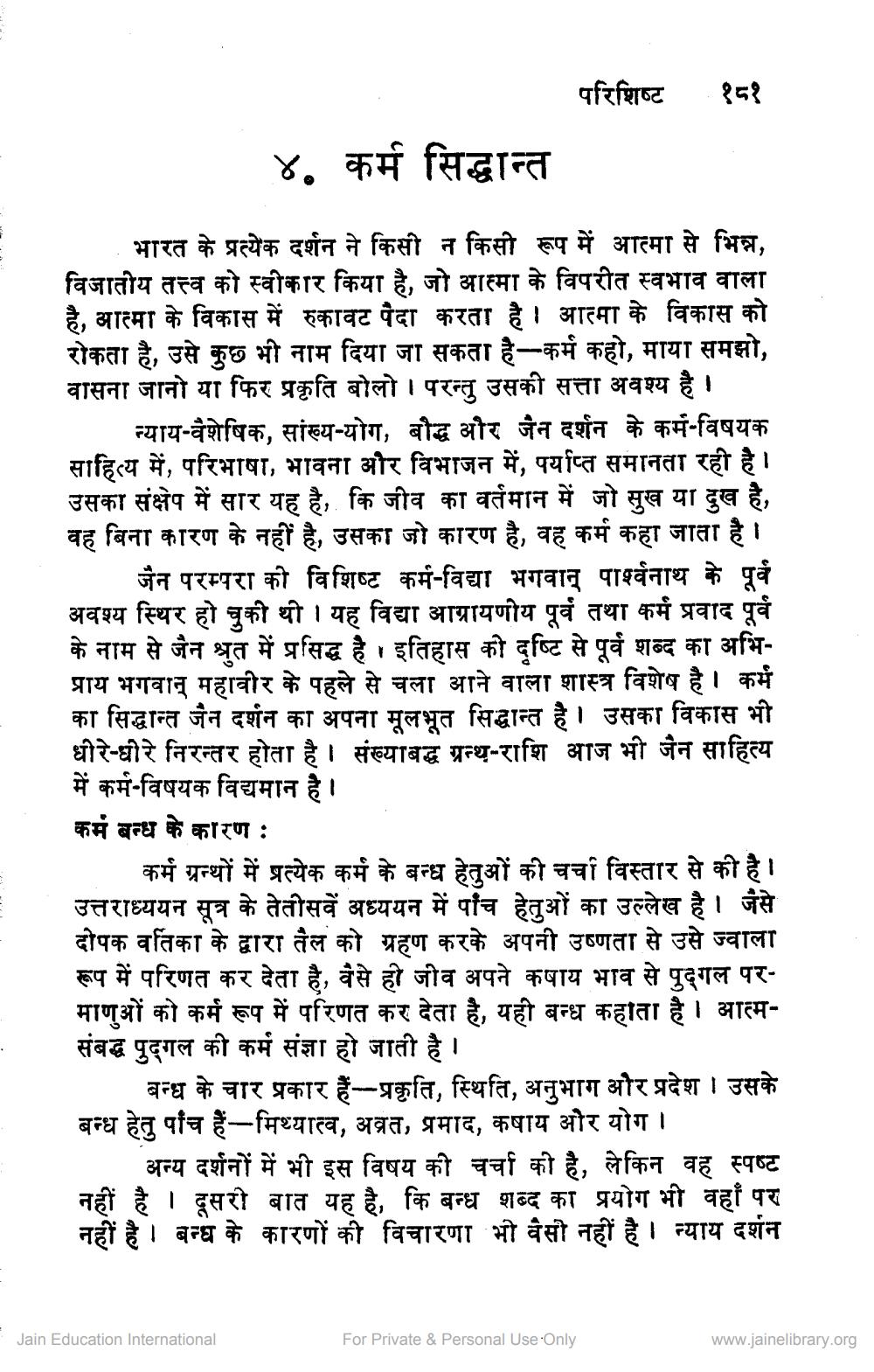________________
परिशिष्ट
१८१
४. कर्म सिद्धान्त
भारत के प्रत्येक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा से भिन्न, विजातीय तत्त्व को स्वीकार किया है, जो आस्मा के विपरीत स्वभाव वाला है, आत्मा के विकास में रुकावट पैदा करता है। आत्मा के विकास को रोकता है, उसे कुछ भी नाम दिया जा सकता है-कर्म कहो, माया समझो, वासना जानो या फिर प्रकृति बोलो । परन्तु उसकी सत्ता अवश्य है।
न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, बौद्ध और जैन दर्शन के कर्म-विषयक साहित्य में, परिभाषा, भावना और विभाजन में, पर्याप्त समानता रही है। उसका संक्षेप में सार यह है, कि जीव का वर्तमान में जो सुख या दुख है, वह बिना कारण के नहीं है, उसका जो कारण है, वह कर्म कहा जाता है।
___ जैन परम्परा की विशिष्ट कर्म-विद्या भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्व अवश्य स्थिर हो चुकी थी। यह विद्या आग्रायणीय पूर्व तथा कर्म प्रवाद पूर्व के नाम से जैन श्रुत में प्रसिद्ध है। इतिहास की दृष्टि से पूर्व शब्द का अभिप्राय भगवान् महावीर के पहले से चला आने वाला शास्त्र विशेष है। कर्म का सिद्धान्त जैन दर्शन का अपना मूलभूत सिद्धान्त है। उसका विकास भी धीरे-धीरे निरन्तर होता है। संख्याबद्ध ग्रन्थ-राशि आज भी जैन साहित्य में कर्म-विषयक विद्यमान है। कर्म बन्ध के कारण : ____ कर्म ग्रन्थों में प्रत्येक कर्म के बन्ध हेतुओं की चर्चा विस्तार से की है। उत्तराध्ययन सूत्र के तेतीसवें अध्ययन में पांच हेतुओं का उल्लेख है। जैसे दोपक वर्तिका के द्वारा तैल को ग्रहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है, वैसे ही जीव अपने कषाय भाव से पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में परिणत कर देता है, यही बन्ध कहाता है। आत्मसंबद्ध पुद्गल की कर्म संज्ञा हो जाती है ।
बन्ध के चार प्रकार हैं-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश । उसके बन्ध हेतु पांच हैं-मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग ।।
अन्य दर्शनों में भी इस विषय की चर्चा की है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि बन्ध शब्द का प्रयोग भी वहाँ पर नहीं है । बन्ध के कारणों की विचारणा भी वैसी नहीं है। न्याय दर्शन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org