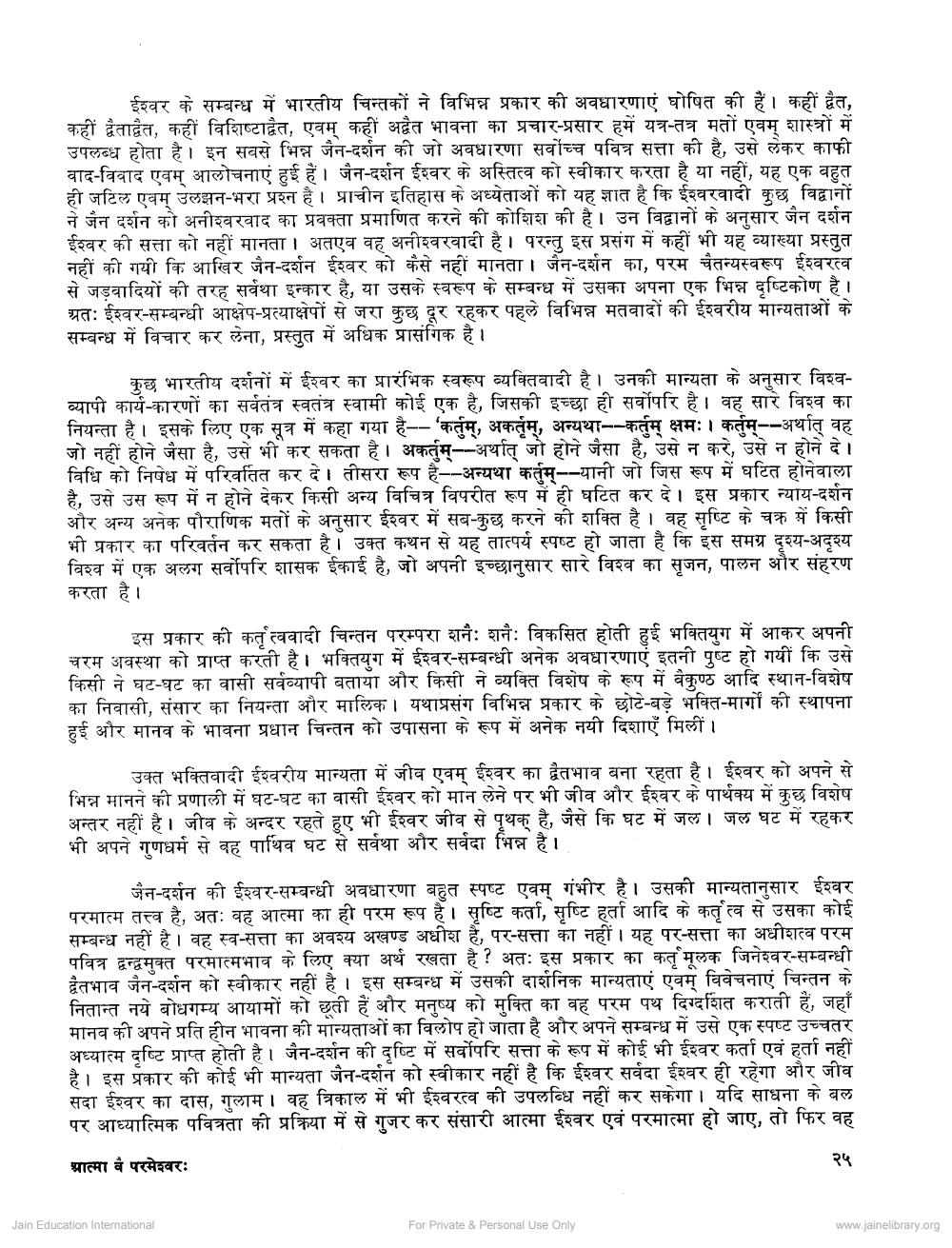________________
ईश्वर के सम्बन्ध में भारतीय चिन्तकों ने विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं घोषित की हैं। कहीं द्वैत, कहीं द्वैताद्वैत, कहीं विशिष्टाद्वैत, एवम् कहीं अद्वैत भावना का प्रचार-प्रसार हमें यत्र-तत्र मतों एवम् शास्त्रों में उपलब्ध होता है। इन सबसे भिन्न जैन-दर्शन की जो अवधारणा सर्वोच्च पवित्र सत्ता की है, उसे लेकर काफी वाद-विवाद एवम् आलोचनाएं हई हैं। जैन-दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है या नहीं, यह एक बहत ही जटिल एवम् उलझन-भरा प्रश्न है। प्राचीन इतिहास के अध्येताओं को यह ज्ञात है कि ईश्वरवादी कूछ विद्वानों ने जैन दर्शन को अनीश्वरवाद का प्रवक्ता प्रमाणित करने की कोशिश की है। उन विद्वानों के अनुसार जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। अतएव वह अनीश्वरवादी है। परन्तु इस प्रसंग में कहीं भी यह व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गयी कि आखिर जैन-दर्शन ईश्वर को कैसे नहीं मानता। जैन-दर्शन का, परम चैतन्यस्वरूप ईश्वरत्व से जड़वादियों की तरह सर्वथा इन्कार है, या उसके स्वरूप के सम्बन्ध में उसका अपना एक भिन्न दृष्टिकोण है। अतः ईश्वर-सम्बन्धी आक्षेप-प्रत्याक्षेपों से जरा कुछ दूर रहकर पहले विभिन्न मतवादों की ईश्वरीय मान्यताओं के सम्बन्ध में विचार कर लेना, प्रस्तुत में अधिक प्रासंगिक है।
कुछ भारतीय दर्शनों में ईश्वर का प्रारंभिक स्वरूप व्यक्तिवादी है। उनकी मान्यता के अनुसार विश्वव्यापी कार्य-कारणों का सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वामी कोई एक है, जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। वह सारे विश्व का नियन्ता है। इसके लिए एक सूत्र में कहा गया है-- 'कर्तुम्, अकर्तुम्, अन्यथा--कर्तुम् क्षमः। कर्तुम्--अर्थात् वह जो नहीं होने जैसा है, उसे भी कर सकता है। अकर्तुम्--अर्थात् जो होने जैसा है, उसे न करे, उसे न होने दे। विधि को निषेध में परिवर्तित कर दे। तीसरा रूप है--अन्यथा कर्तुम्--यानी जो जिस रूप में घटित होनेवाला है, उसे उस रूप में न होने देकर किसी अन्य विचित्र विपरीत रूप में ही घटित कर दे। इस प्रकार न्याय-दर्शन और अन्य अनेक पौराणिक मतों के अनुसार ईश्वर में सब-कुछ करने की शक्ति है। वह सृष्टि के चक्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। उक्त कथन से यह तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है कि इस समग्र दृश्य-अदृश्य विश्व में एक अलग सर्वोपरि शासक ईकाई है, जो अपनी इच्छानुसार सारे विश्व का सृजन, पालन और संहरण करता है।
इस प्रकार की कर्तृत्ववादी चिन्तन परम्परा शनैः शनैः विकसित होती हई भक्तियग में आकर अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करती है। भक्तियुग में ईश्वर-सम्बन्धी अनेक अवधारणाएं इतनी पुष्ट हो गयीं कि उसे किसी ने घट-घट का वासी सर्वव्यापी बताया और किसी ने व्यक्ति विशेष के रूप में वैकुण्ठ आदि स्थान-विशेष का निवासी, संसार का नियन्ता और मालिक। यथाप्रसंग विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े भक्ति-मार्गों की स्थापना हई और मानव के भावना प्रधान चिन्तन को उपासना के रूप में अनेक नयी दिशाएँ मिलीं।
उक्त भक्तिवादी ईश्वरीय मान्यता में जीव एवम् ईश्वर का द्वैतभाव बना रहता है। ईश्वर को अपने से भिन्न मानने की प्रणाली में घट-घट का वासी ईश्वर को मान लेने पर भी जीव और ईश्वर के पार्थक्य में कुछ विशेष अन्तर नहीं है। जीव के अन्दर रहते हुए भी ईश्वर जीव से पृथक् है, जैसे कि घट में जल। जल घट में रहकर भी अपने गुणधर्म से वह पार्थिव घट से सर्वथा और सर्वदा भिन्न है।
जैन-दर्शन की ईश्वर-सम्बन्धी अवधारणा बहुत स्पष्ट एवम् गंभीर है। उसकी मान्यतानुसार ईश्वर परमात्म तत्त्व है, अतः वह आत्मा का ही परम रूप है। सृष्टि कर्ता, सृष्टि हर्ता आदि के कर्तृत्व से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह स्व-सत्ता का अवश्य अखण्ड अधीश है, पर-सत्ता का नहीं। यह पर-सत्ता का अधीशत्व परम पवित्र द्वन्द्वमुक्त परमात्मभाव के लिए क्या अर्थ रखता है ? अतः इस प्रकार का कर्तृमूलक जिनेश्वर-सम्बन्धी द्वैतभाव जैन-दर्शन को स्वीकार नहीं है। इस सम्बन्ध में उसकी दार्शनिक मान्यताएं एवम् विवेचनाएं चिन्तन के नितान्त नये बोधगम्य आयामों को छती हैं और मनुष्य को मुक्ति का वह परम पथ दिग्दर्शित कराती हैं, जहाँ मानव की अपने प्रति हीन भावना की मान्यताओं का विलोप हो जाता है और अपने सम्बन्ध में उसे एक स्पष्ट उच्चतर अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होती है। जैन-दर्शन की दृष्टि में सर्वोपरि सत्ता के रूप में कोई भी ईश्वर कर्ता एवं हर्ता नहीं है। इस प्रकार की कोई भी मान्यता जैन-दर्शन को स्वीकार नहीं है कि ईश्वर सर्वदा ईश्वर ही रहेगा और जीव सदा ईश्वर का दास, गुलाम। वह त्रिकाल में भी ईश्वरत्व की उपलब्धि नहीं कर सकेगा। यदि साधना के बल पर आध्यात्मिक पवित्रता की प्रक्रिया में से गुजर कर संसारी आत्मा ईश्वर एवं परमात्मा हो जाए, तो फिर वह
प्रात्मा वै परमेश्वरः
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org