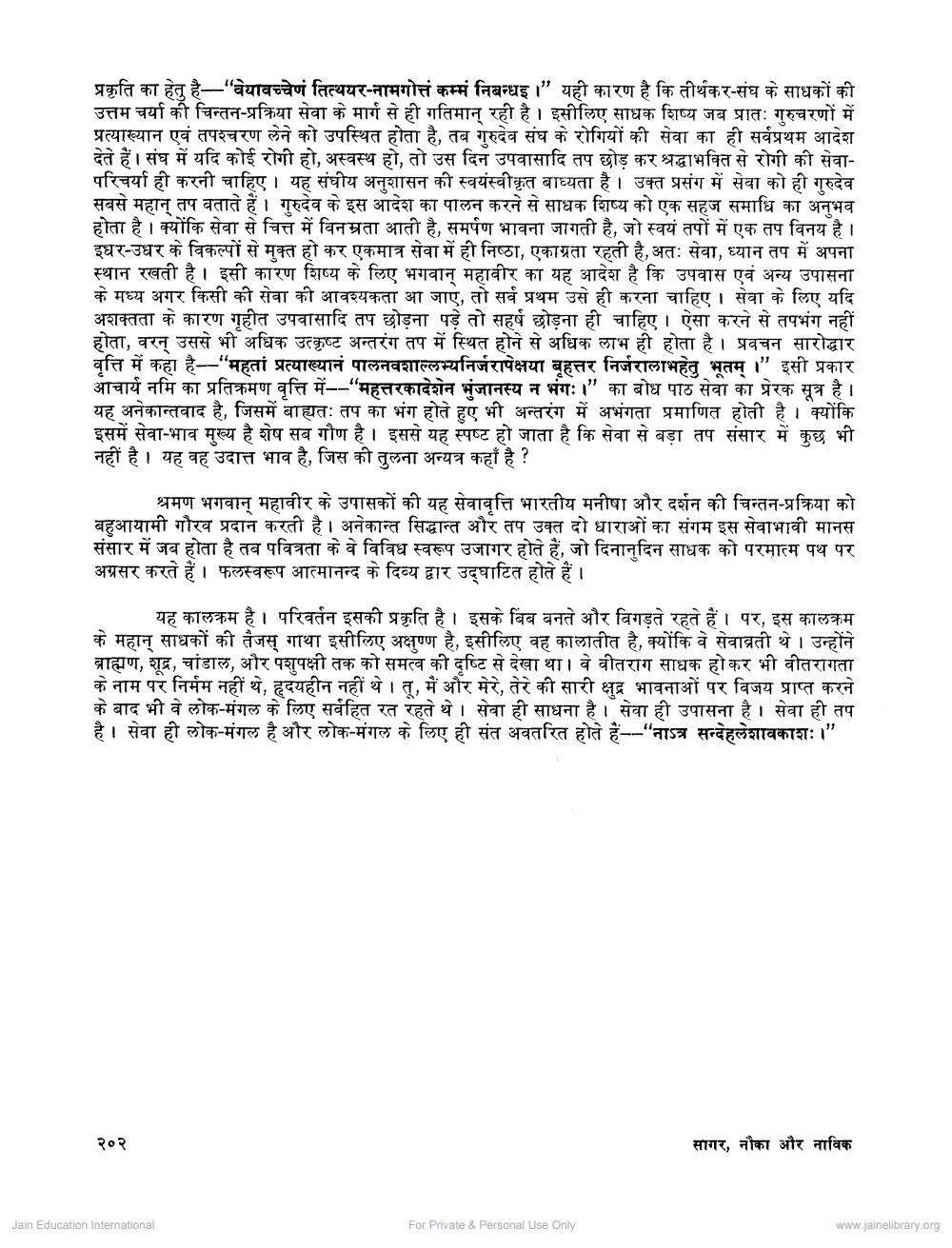________________
प्रकृति का हेतु है - "वेयावच्चेणं तित्थयर-नामगोत्तं कम्मं निबन्धइ ।” यही कारण है कि तीर्थंकर संघ के साधकों की उत्तमचर्या की चिन्तन प्रक्रिया सेवा के मार्ग से ही गतिमान् रही है । इसीलिए साधक शिष्य जब प्रातः गुरुचरणों में प्रत्याख्यान एवं तपश्चरण लेने को उपस्थित होता है, तब गुरुदेव संघ के रोगियों की सेवा का ही सर्वप्रथम आदेश देते हैं। संघ में यदि कोई रोगी हो, अस्वस्थ हो, तो उस दिन उपवासादि तप छोड़ कर श्रद्धाभक्ति से रोगी की सेवापरिचर्या ही करनी चाहिए। यह संघीय अनुशासन की स्वयंस्वीकृत बाध्यता है। उक्त प्रसंग में सेवा को ही गुरुदेव सबसे महान् तप बताते हैं। गुरुदेव के इस आदेश का पालन करने से साधक शिष्य को एक सहज समाधि का अनुभव होता है। क्योंकि सेवा से चित्त में विनम्रता आती है, समर्पण भावना जागती है, जो स्वयं तपों में एक तप विनय है । इधर-उधर के विकल्पों से मुक्त हो कर एकमात्र सेवा में ही निष्ठा, एकाग्रता रहती है, अतः सेवा, ध्यान तप में अपना स्थान रखती है । इसी कारण शिष्य के लिए भगवान् महावीर का यह आदेश है कि उपवास एवं अन्य उपासन के मध्य अगर किसी की सेवा की आवश्यकता आ जाए, तो सर्व प्रथम उसे ही करना चाहिए । सेवा के लिए यदि अशक्तता के कारण गृहीत उपवासादि तप छोड़ना पड़े तो सहर्ष छोड़ना ही चाहिए। ऐसा करने से तपभंग नहीं होता, वरन् उससे भी अधिक उत्कृष्ट अन्तरंग तप में स्थित होने से अधिक लाभ ही होता है। प्रवचन सारोद्धार वृत्ति में कहा है- " महतां प्रत्याख्यानं पालनवशाल्लभ्यनिर्जरापेक्षया बृहत्तर निर्जराला महेतु भूतम् ।" इसी प्रकार आचार्य नमि का प्रतिक्रमण वृत्ति में "महत्तरकादेशेन भुंजानस्य न भंगः " का बोध पाठ सेवा का प्रेरक सूत्र है। यह अनेकान्तवाद है, जिसमें बाह्यतः तप का भंग होते हुए भी अन्तरंग में अभंगता प्रमाणित होती है । क्योंकि इसमें सेवा भाव मुख्य है शेष सब गौण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सेवा से बड़ा तप संसार में कुछ भी नहीं है । यह वह उदात्त भाव है, जिस की तुलना अन्यत्र कहाँ है ?
श्रमण भगवान् महावीर के उपासकों की यह सेवावृत्ति भारतीय मनीषा और दर्शन की चिन्तन प्रक्रिया को बहुआयामी गौरव प्रदान करती है । अनेकान्त सिद्धान्त और तप उक्त दो धाराओं का संगम इस सेवाभावी मानस संसार में जब होता है तब पवित्रता के वे विविध स्वरूप उजागर होते हैं, जो दिनानुदिन साधक को परमात्म पथ पर अग्रसर करते हैं । फलस्वरूप आत्मानन्द के दिव्य द्वार उद्घाटित होते हैं ।
यह कालक्रम है । परिवर्तन इसकी प्रकृति है । इसके बिब बनते और बिगड़ते रहते हैं । पर इस कालक्रम के महान् साधकों की तेजस् गाथा इसीलिए अक्षुण्ण है, इसीलिए वह कालातीत है, क्योंकि वे सेवाव्रती थे। उन्होंने ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल और पशुपक्षी तक को समत्व की दृष्टि से देखा था। वे वीतराग साधक हो कर भी वीतरागता के नाम पर निर्मम नहीं थे, हृदयहीन नहीं थे । तू, मैं और मेरे, तेरे की सारी क्षुद्र भावनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी वे लोक-मंगल के लिए सर्वहित रत रहते थे। सेवा ही साधना है। सेवा ही उपासना है सेवा ही तप है। सेवा ही लोक-मंगल है और लोक-मंगल के लिए ही संत अवतरित होते है--" नात्र सन्देहलेशावकाशः ।"
२०२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
सागर, नौका और नाविक
www.jainelibrary.org.