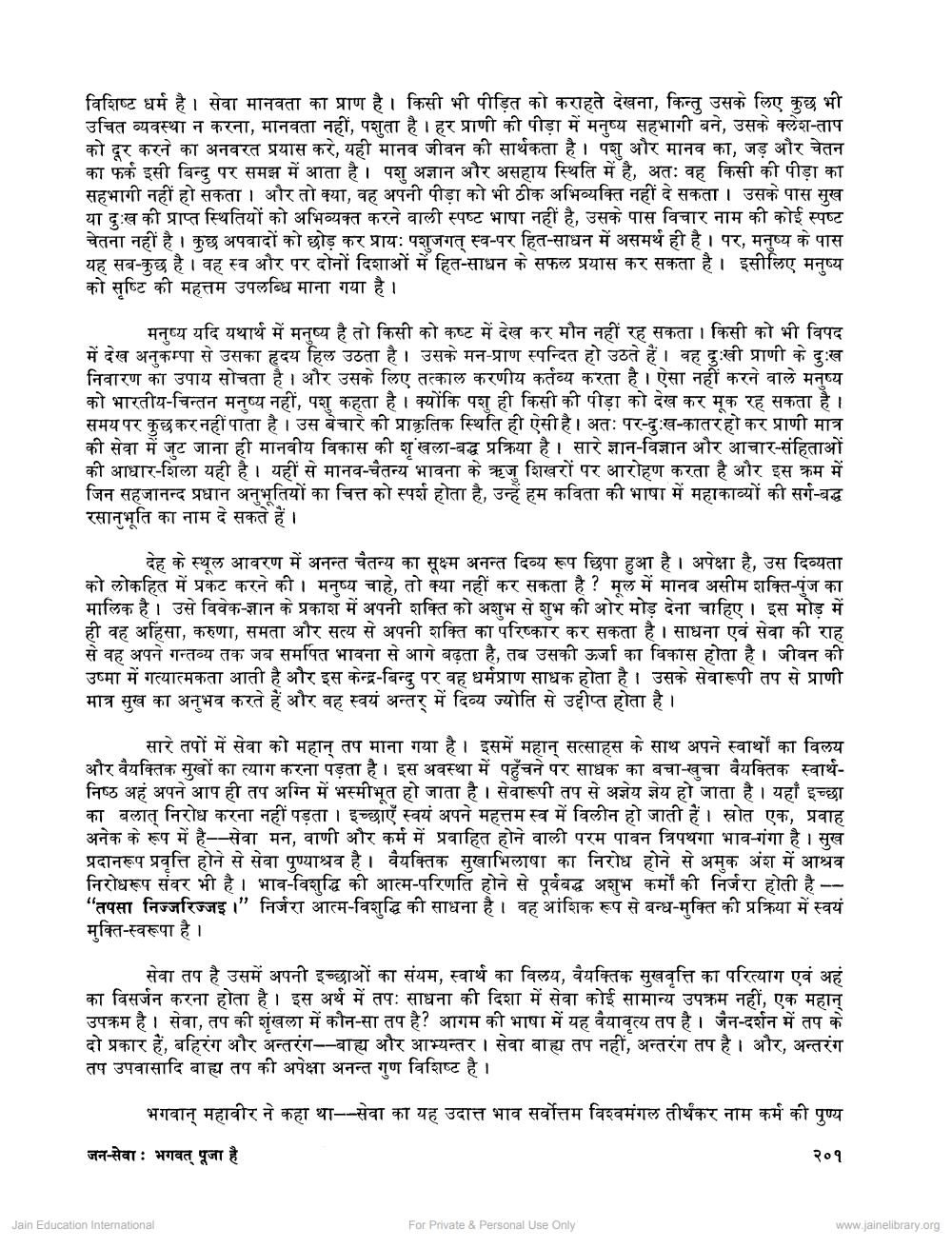________________
विशिष्ट धर्म है। सेवा मानवता का प्राण है। किसी भी पीडित को कराहते देखना, किन्तु उसके लिए कुछ भी उचित व्यवस्था न करना, मानवता नहीं, पशुता है। हर प्राणी की पीड़ा में मनुष्य सहभागी बने, उसके क्लेश-ताप को दूर करने का अनवरत प्रयास करे, यही मानव जीवन की सार्थकता है। पशु और मानव का, जड़ और चेतन का फर्क इसी बिन्दु पर समझ में आता है। पशु अज्ञान और असहाय स्थिति में है, अतः वह किसी की पीड़ा का सहभागी नहीं हो सकता। और तो क्या, वह अपनी पीड़ा को भी ठीक अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। उसके पास सुख या दुःख की प्राप्त स्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली स्पष्ट भाषा नहीं है, उसके पास विचार नाम की कोई स्पष्ट चेतना नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ कर प्रायः पशुजगत् स्व-पर हित-साधन में असमर्थ ही है। पर, मनुष्य के पास यह सब-कुछ है । वह स्व और पर दोनों दिशाओं में हित-साधन के सफल प्रयास कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को सष्टि की महत्तम उपलब्धि माना गया है।
मनष्य यदि यथार्थ में मनुष्य है तो किसी को कष्ट में देख कर मौन नहीं रह सकता। किसी को भी विपद में देख अनुकम्पा से उसका हृदय हिल उठता है। उसके मन-प्राण स्पन्दित हो उठते हैं। वह दुःखी प्राणी के दुःख निवारण का उपाय सोचता है। और उसके लिए तत्काल करणीय कर्तव्य करता है। ऐसा नहीं करने वाले मनुष्य को भारतीय-चिन्तन मनुष्य नहीं, पश कहता है। क्योंकि पशु ही किसी की पीड़ा को देख कर मक रह सकता है। समय पर कुछ कर नहीं पाता है। उस बेचारे की प्राकृतिक स्थिति ही ऐसी है। अतः पर-दुःख-कातर हो कर प्राणी मात्र की सेवा में जुट जाना ही मानवीय विकास की शखला-बद्ध प्रक्रिया है। सारे ज्ञान-विज्ञान और आचार-संहिताओं की आधारशिला यही है। यहीं से मानव-चैतन्य भावना के ऋज शिखरों पर आरोहण करता है और इस क्रम में जिन सहजानन्द प्रधान अनभतियों का चित्त को स्पर्श होता है, उन्हें हम कविता की भाषा में महाकाव्यों की सर्ग-बद्ध रसानुभूति का नाम दे सकते हैं।
देह के स्थूल आवरण में अनन्त चैतन्य का सूक्ष्म अनन्त दिव्य रूप छिपा हुआ है। अपेक्षा है, उस दिव्यता को लोकहित में प्रकट करने की। मनुष्य चाहे, तो क्या नहीं कर सकता है ? मूल में मानव असीम शक्ति-पुंज का मालिक है। उसे विवेक-ज्ञान के प्रकाश में अपनी शक्ति को अशुभ से शुभ की ओर मोड़ देना चाहिए। इस मोड़ में ही वह अहिंसा, करुणा, समता और सत्य से अपनी शक्ति का परिष्कार कर सकता है। साधना एवं सेवा की राह से वह अपने गन्तव्य तक जब समर्पित भावना से आगे बढ़ता है, तब उसकी ऊर्जा का विकास होता है। जीवन की उष्मा में गत्यात्मकता आती है और इस केन्द्र-बिन्दु पर वह धर्मप्राण साधक होता है। उसके सेवारूपी तप से प्राणी मात्र सुख का अनुभव करते हैं और वह स्वयं अन्तर में दिव्य ज्योति से उद्दीप्त होता है।
सारे तपों में सेवा को महान तप माना गया है। इसमें महान सत्साहस के साथ अपने स्वार्थों का विलय और वैयक्तिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। इस अवस्था में पहुँचने पर साधक का बचा-खुचा वैयक्तिक स्वार्थनिष्ठ अहं अपने आप ही तप अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है। सेवारूपी तप से अज्ञेय ज्ञेय हो जाता है। यहाँ इच्छा का बलात् निरोध करना नहीं पड़ता। इच्छाएँ स्वयं अपने महत्तम स्व में विलीन हो जाती हैं। स्रोत एक, प्रवाह अनेक के रूप में है--सेवा मन, वाणी और कर्म में प्रवाहित होने वाली परम पावन त्रिपथगा भाव-गंगा है। सुख प्रदानरूप प्रवृत्ति होने से सेवा पुण्याश्रव है। वैयक्तिक सुखाभिलाषा का निरोध होने से अमुक अंश में आश्रव निरोधरूप संवर भी है। भाव-विशुद्धि की आत्म-परिणति होने से पूर्वबद्ध अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है-- "तपसा निजरिज्जइ।" निर्जरा आत्म-विशुद्धि की साधना है। वह आंशिक रूप से बन्ध-मुक्ति की प्रक्रिया में स्वयं मुक्ति-स्वरूपा है।
सेवा तप है उसमें अपनी इच्छाओं का संयम, स्वार्थ का विलय, वैयक्तिक सुखवृत्ति का परित्याग एवं अहं का विसर्जन करना होता है। इस अर्थ में तपः साधना की दिशा में सेवा कोई सामान्य उपक्रम नहीं, एक महान् उपक्रम है। सेवा, तप की शृंखला में कौन-सा तप है? आगम की भाषा में यह वैयावृत्य तप है। जैन-दर्शन में तप के दो प्रकार हैं, बहिरंग और अन्तरंग--बाह्य और आभ्यन्तर । सेवा बाह्य तप नहीं, अन्तरंग तप है। और, अन्तरंग तप उपवासादि बाह्य तप की अपेक्षा अनन्त गुण विशिष्ट है।
भगवान महावीर ने कहा था--सेवा का यह उदात्त भाव सर्वोत्तम विश्वमंगल तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य
जन-सेवा : भगवत् पूजा है
२०१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org