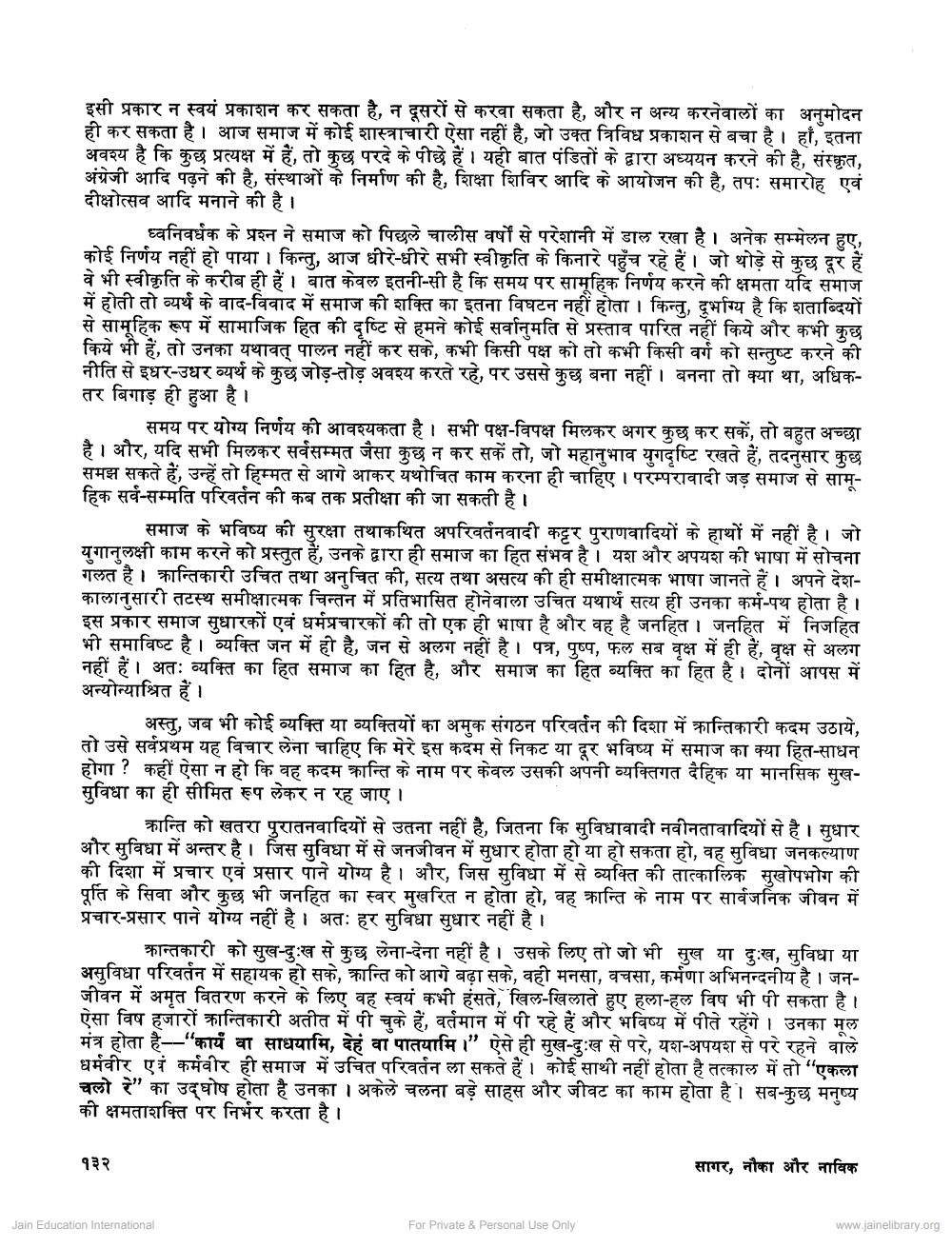________________
इसी प्रकार न स्वयं प्रकाशन कर सकता है, न दूसरों से करवा सकता है, और न अन्य करनेवालों का अनुमोदन ही कर सकता है । आज समाज में कोई शास्त्राचारी ऐसा नहीं है, जो उक्त त्रिविध प्रकाशन से बचा है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ प्रत्यक्ष में हैं, तो कुछ परदे के पीछे हैं । यही बात पंडितों के द्वारा अध्ययन करने की है, संस्कृत, अंग्रेजी आदि पढ़ने की है, संस्थाओं के निर्माण की है, शिक्षा शिविर आदि के आयोजन की है, तपः समारोह एवं दीक्षोत्सव आदि मनाने की है ।
ध्वनिवर्धक के प्रश्न ने समाज को पिछले चालीस वर्षों से परेशानी में डाल रखा है । अनेक सम्मेलन हुए, कोई निर्णय नहीं हो पाया । किन्तु, आज धीरे-धीरे सभी स्वीकृति के किनारे पहुँच रहे हैं। जो थोड़े से कुछ दूर हैं वे भी स्वीकृति के करीब ही हैं। बात केवल इतनी सी है कि समय पर सामूहिक निर्णय करने की क्षमता यदि समाज में होती तो व्यर्थ के वाद-विवाद में समाज की शक्ति का इतना विघटन नहीं होता । किन्तु, दुर्भाग्य है कि शताब्दियों से सामूहिक रूप में सामाजिक हित की दृष्टि से हमने कोई सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित नहीं किये और कभी कुछ किये भी हैं, तो उनका यथावत् पालन नहीं कर सके, कभी किसी पक्ष को तो कभी किसी वर्ग को सन्तुष्ट करने की नीति से इधर-उधर व्यर्थ के कुछ जोड़-तोड़ अवश्य करते रहे, पर उससे कुछ बना नहीं । बनना तो क्या था, अधिकतर बिगाड़ ही हुआ है ।
समय पर योग्य निर्णय की आवश्यकता है । सभी पक्ष-विपक्ष मिलकर अगर कुछ कर सकें, तो बहुत अच्छा है । और, यदि सभी मिलकर सर्वसम्मत जैसा कुछ न कर सकें तो, जो महानुभाव युगदृष्टि रखते हैं, तदनुसार कुछ समझ सकते हैं, उन्हें तो हिम्मत से आगे आकर यथोचित काम करना ही चाहिए । परम्परावादी जड़ समाज से सामूहिक सर्व सम्मति परिवर्तन की कब तक प्रतीक्षा की जा सकती है ।
I
समाज के भविष्य की सुरक्षा तथाकथित अपरिवर्तनवादी कट्टर पुराणवादियों के हाथों में नहीं है । जो युगानुलक्षी काम करने को प्रस्तुत हैं, उनके द्वारा ही समाज का हित संभव है । यश और अपयश की भाषा में सोचना गलत है । क्रान्तिकारी उचित तथा अनुचित की, सत्य तथा असत्य की ही समीक्षात्मक भाषा जानते हैं। अपने देशकालानुसारी तटस्थ समीक्षात्मक चिन्तन में प्रतिभासित होनेवाला उचित यथार्थ सत्य ही उनका कर्म-पथ होता है । इस प्रकार समाज सुधारकों एवं धर्मप्रचारकों की तो एक ही भाषा है और वह है जनहित । जनहित में निजहित भी समाविष्ट है । व्यक्ति जन में ही है, जन से अलग नहीं है । पत्र, पुष्प, फल सब वृक्ष में ही हैं, वृक्ष से अलग नहीं हैं । अतः व्यक्ति का हित समाज का हित है, और समाज का हित व्यक्ति का हित है। दोनों आपस में अन्योन्याश्रित हैं ।
अस्तु, जब भी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का अमुक संगठन परिवर्तन की दिशा में क्रान्तिकारी कदम उठाये, तो उसे सर्वप्रथम यह विचार लेना चाहिए कि मेरे इस कदम से निकट या दूर भविष्य में समाज का क्या हित साधन होगा ? कहीं ऐसा न हो कि वह कदम क्रान्ति के नाम पर केवल उसकी अपनी व्यक्तिगत दैहिक या मानसिक सुखसुविधा का ही सीमित रूप लेकर न रह जाए ।
क्रान्ति को खतरा पुरातनवादियों से उतना नहीं है, जितना कि सुविधावादी नवीनतावादियों से है । सुधार और सुविधा में अन्तर है । जिस सुविधा में से जनजीवन में सुधार होता हो या हो सकता हो, वह सुविधा जनकल्याण की दिशा में प्रचार एवं प्रसार पाने योग्य है । और जिस सुविधा में से व्यक्ति की तात्कालिक सुखोपभोग की पूर्ति के सिवा और कुछ भी जनहित का स्वर मुखरित न होता हो, वह क्रान्ति के नाम पर सार्वजनिक जीवन में प्रचार-प्रसार पाने योग्य नहीं है । अतः हर सुविधा सुधार नहीं है ।
कान्तकारी को सुख-दुःख से कुछ लेना-देना नहीं है। उसके लिए तो जो भी सुख या दुःख, सुविधा या असुविधा परिवर्तन में सहायक हो सके, क्रान्ति को आगे बढ़ा सके, वही मनसा, वचसा, कर्मणा अभिनन्दनीय है । जनजीवन में अमृत वितरण करने के लिए वह स्वयं कभी हंसते, खिल खिलाते हुए हलाहल विष भी पी सकता है । ऐसा विष हजारों क्रान्तिकारी अतीत में पी चुके हैं, वर्तमान में पी रहे हैं और भविष्य में पीते रहेंगे। उनका मूल मंत्र होता है - " कार्यं वा साधयामि, देहं वा पातयामि ।" ऐसे ही सुख-दुःख से परे, यश-अपयश से परे रहने वाले धर्मवीर एवं कर्मवीर ही समाज में उचित परिवर्तन ला सकते हैं । कोई साथी नहीं होता है तत्काल में तो "एकला चलो रे" का उद्घोष होता है उनका । अकेले चलना बड़े साहस और जीवट का काम होता है । सब-कुछ मनुष्य की क्षमताशक्ति पर निर्भर करता है ।
१३२
Jain Education International
For Private Personal Use Only
सागर, नौका और नाविक
www.jainelibrary.org