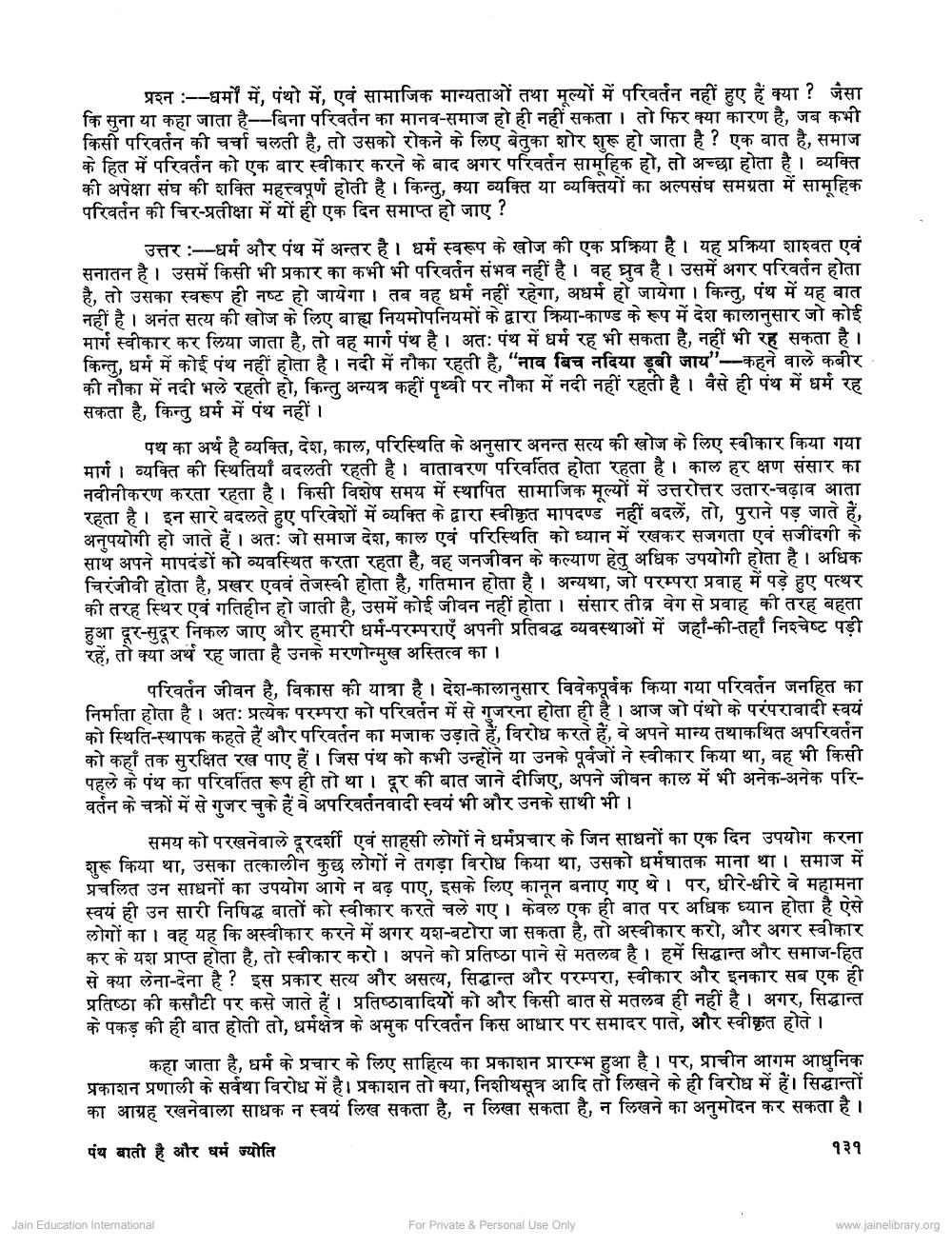________________
प्रश्न :--धर्मों में, पंथो में, एवं सामाजिक मान्यताओं तथा मूल्यों में परिवर्तन नहीं हुए हैं क्या? जैसा कि सुना या कहा जाता है-बिना परिवर्तन का मानव-समाज हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या कारण है, जब कभी किसी परिवर्तन की चर्चा चलती है, तो उसको रोकने के लिए बेतुका शोर शुरू हो जाता है ? एक बात है, समाज के हित में परिवर्तन को एक बार स्वीकार करने के बाद अगर परिवर्तन सामूहिक हो, तो अच्छा होता है। व्यक्ति की अपेक्षा संघ की शक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। किन्तु, क्या व्यक्ति या व्यक्तियों का अल्पसंघ समग्रता में सामूहिक परिवर्तन की चिर-प्रतीक्षा में यों ही एक दिन समाप्त हो जाए?
उत्तर :-धर्म और पंथ में अन्तर है। धर्म स्वरूप के खोज की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शाश्वत एवं सनातन है। उसमें किसी भी प्रकार का कभी भी परिवर्तन संभव नहीं है। वह ध्रुव है। उसमें अगर परिवर्तन होता है, तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जायेगा। तब वह धर्म नहीं रहेगा, अधर्म हो जायेगा। किन्तु, पंथ में यह बात नहीं है। अनंत सत्य की खोज के लिए बाह्य नियमोपनियमों के द्वारा क्रिया-काण्ड के रूप में देश कालानुसार जो कोई मार्ग स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह मार्ग पंथ है। अतः पंथ में धर्म रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। किन्तु, धर्म में कोई पंथ नहीं होता है। नदी में नौका रहती है, “नाव बिच नदिया डूबी जाय"-कहने वाले कबीर की नौका में नदी भले रहती हो, किन्तु अन्यत्र कहीं पृथ्वी पर नौका में नदी नहीं रहती है। वैसे ही पंथ में धर्म रह सकता है, किन्तु धर्म में पंथ नहीं।
पथ का अर्थ है व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अनन्त सत्य की खोज के लिए स्वीकार किया गया मार्ग । व्यक्ति की स्थितियाँ बदलती रहती है। वातावरण परिवर्तित होता रहता है। काल हर क्षण संसार का नवीनीकरण करता रहता है। किसी विशेष समय में स्थापित सामाजिक मूल्यों में उत्तरोत्तर उतार-चढ़ाव आता रहता है। इन सारे बदलते हुए परिवेशों में व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत मापदण्ड नहीं बदलें, तो, पुराने पड़ जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः जो समाज देश, काल एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर सजगता एवं सजींदगी के साथ अपने मापदंडों को व्यवस्थित करता रहता है, वह जनजीवन के कल्याण हेतु अधिक उपयोगी होता है। अधिक चिरंजीवी होता है, प्रखर एववं तेजस्वी होता है, गतिमान होता है। अन्यथा, जो परम्परा प्रवाह में पड़े हुए पत्थर की तरह स्थिर एवं गतिहीन हो जाती है, उसमें कोई जीवन नहीं होता। संसार तीव्र वेग से प्रवाह की तरह बहता हुआ दूर-सुदूर निकल जाए और हमारी धर्म-परम्पराएँ अपनी प्रतिबद्ध व्यवस्थाओं में जहाँ-की-तहाँ निश्चेष्ट पड़ी रहें, तो क्या अर्थ रह जाता है उनके मरणोन्मुख अस्तित्व का।
परिवर्तन जीवन है, विकास की यात्रा है। देश-कालानुसार विवेकपूर्वक किया गया परिवर्तन जनहित का निर्माता होता है। अतः प्रत्येक परम्परा को परिवर्तन में से गुजरना होता ही है। आज जो पंथो के परंपरावादी स्वयं को स्थिति-स्थापक कहते हैं और परिवर्तन का मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, वे अपने मान्य तथाकथित अपरिवर्तन को कहाँ तक सुरक्षित रख पाए हैं। जिस पंथ को कभी उन्होंने या उनके पूर्वजों ने स्वीकार किया था, वह भी किसी पहले के पंथ का परिवर्तित रूप ही तो था। दूर की बात जाने दीजिए, अपने जीवन काल में भी अनेक-अनेक परिवर्तन के चक्रों में से गुजर चुके हैं वे अपरिवर्तनवादी स्वयं भी और उनके साथी भी।
समय को परखनेवाले दूरदर्शी एवं साहसी लोगों ने धर्मप्रचार के जिन साधनों का एक दिन उपयोग करना शुरू किया था, उसका तत्कालीन कुछ लोगों ने तगड़ा विरोध किया था, उसको धर्मघातक माना था। समाज में प्रचलित उन साधनों का उपयोग आगे न बढ़ पाए, इसके लिए कानून बनाए गए थे। पर, धीरे-धीरे वे महामना स्वयं ही उन सारी निषिद्ध बातों को स्वीकार करते चले गए। केवल एक ही बात पर अधिक ध्यान होता है ऐसे लोगों का। वह यह कि अस्वीकार करने में अगर यश-बटोरा जा सकता है, तो अस्वीकार करो, और अगर स्वीकार कर के यश प्राप्त होता है, तो स्वीकार करो। अपने को प्रतिष्ठा पाने से मतलब है। हमें सिद्धान्त और समाज-हित से क्या लेना-देना है? इस प्रकार सत्य और असत्य, सिद्धान्त और परम्परा, स्वीकार और इनकार सब एक ही प्रतिष्ठा की कसौटी पर कसे जाते हैं। प्रतिष्ठावादियों को और किसी बात से मतलब ही नहीं है। अगर, सिद्धान्त के पकड़ की ही बात होती तो, धर्मक्षेत्र के अमुक परिवर्तन किस आधार पर समादर पाते, और स्वीकृत होते।
कहा जाता है, धर्म के प्रचार के लिए साहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है। पर, प्राचीन आगम आधुनिक प्रकाशन प्रणाली के सर्वथा विरोध में है। प्रकाशन तो क्या, निशीथसूत्र आदि तो लिखने के ही विरोध में हैं। सिद्धान्तों का आग्रह रखनेवाला साधक न स्वयं लिख सकता है, न लिखा सकता है, न लिखने का अनुमोदन कर सकता है।
पंथ बाती है और धर्म ज्योति
१३१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org