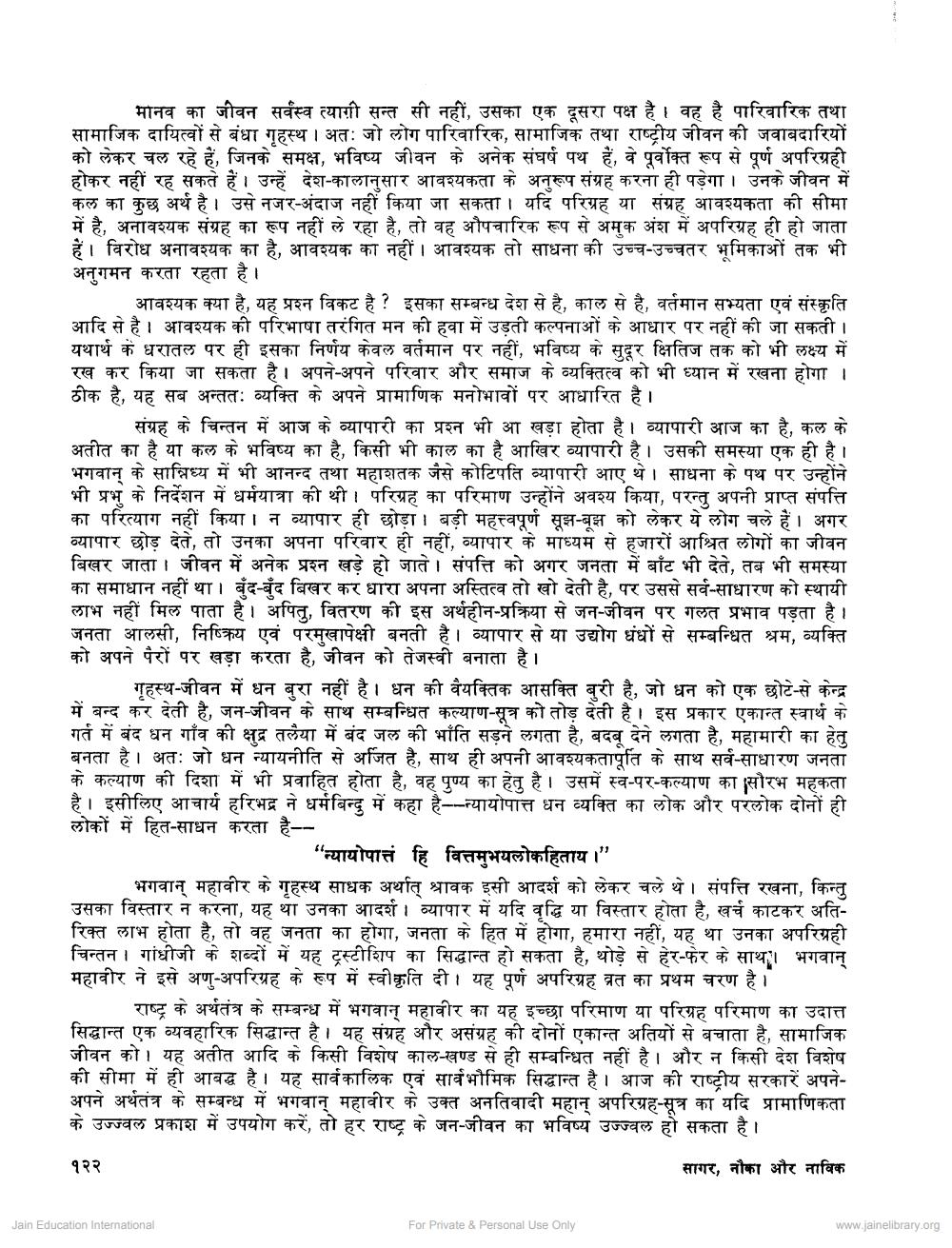________________
मानव का जीवन सर्वस्व त्यागी सन्त सी नहीं, उसका एक दूसरा पक्ष है। वह है पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों से बंधा गहस्थ । अतः जो लोग पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की जवाबदारियों को लेकर चल रहे हैं, जिनके समक्ष, भविष्य जीवन के अनेक संघर्ष पथ हैं, वे पूर्वोक्त रूप से पूर्ण अपरिग्रही होकर नहीं रह सकते हैं। उन्हें देश-कालानुसार आवश्यकता के अनुरूप संग्रह करना ही पड़ेगा। उनके जीवन में कल का कुछ अर्थ है। उसे नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता। यदि परिग्रह या संग्रह आवश्यकता की सीमा में है, अनावश्यक संग्रह का रूप नहीं ले रहा है, तो वह औपचारिक रूप से अमक अंश में अपरिग्रह ही हो जाता हैं। विरोध अनावश्यक का है, आवश्यक का नहीं। आवश्यक तो साधना की उच्च-उच्चतर भूमिकाओं तक भी अनुगमन करता रहता है।
आवश्यक क्या है, यह प्रश्न विकट है ? इसका सम्बन्ध देश से है, काल से है, वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति आदि से है। आवश्यक की परिभाषा तरंगित मन की हवा में उड़ती कल्पनाओं के आधार पर नहीं की जा सकती। यथार्थ के धरातल पर ही इसका निर्णय केवल वर्तमान पर नहीं, भविष्य के सुदूर क्षितिज तक को भी लक्ष्य में रख कर किया जा सकता है। अपने-अपने परिवार और समाज के व्यक्तित्व को भी ध्यान में रखना होगा । ठीक है, यह सब अन्तत: व्यक्ति के अपने प्रामाणिक मनोभावों पर आधारित है।
संग्रह के चिन्तन में आज के व्यापारी का प्रश्न भी आ खड़ा होता है। व्यापारी आज का है, कल के अतीत का है या कल के भविष्य का है, किसी भी काल का है आखिर व्यापारी है। उसकी समस्या एक ही है। भगवान् के सान्निध्य में भी आनन्द तथा महाशतक जैसे कोटिपति व्यापारी आए थे। साधना के पथ पर उन्होंने भी प्रभु के निर्देशन में धर्मयात्रा की थी। परिग्रह का परिमाण उन्होंने अवश्य किया, परन्तु अपनी प्राप्त संपत्ति का परित्याग नहीं किया। न व्यापार ही छोड़ा। बड़ी महत्त्वपूर्ण सूझ-बुझ को लेकर ये लोग चले हैं। अगर व्यापार छोड़ देते, तो उनका अपना परिवार ही नहीं, व्यापार के माध्यम से हजारों आश्रित लोगों का जीवन बिखर जाता। जीवन में अनेक प्रश्न खड़े हो जाते। संपत्ति को अगर जनता में बाँट भी देते, तब भी समस्या का समाधान नहीं था। बंद-बूंद बिखर कर धारा अपना अस्तित्व तो खो देती है, पर उससे सर्व-साधारण को स्थायी लाभ नहीं मिल पाता है। अपितु, वितरण की इस अर्थहीन-प्रक्रिया से जन-जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। जनता आलसी, निष्क्रिय एवं परमुखापेक्षी बनती है। व्यापार से या उद्योग धंधों से सम्बन्धित श्रम, व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करता है, जीवन को तेजस्वी बनाता है।
गृहस्थ-जीवन में धन बुरा नहीं है। धन की वैयक्तिक आसक्ति बुरी है, जो धन को एक छोटे-से केन्द्र में बन्द कर देती है, जन-जीवन के साथ सम्बन्धित कल्याण-सूत्र को तोड़ देती है। इस प्रकार एकान्त स्वार्थ के गर्त में बंद धन गाँव की क्षुद्र तलैया में बंद जल की भाँति सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, महामारी का हेतु बनता है। अत: जो धन न्यायनीति से अजित है, साथ ही अपनी आवश्यकतापूर्ति के साथ सर्व-साधारण जनता के कल्याण की दिशा में भी प्रवाहित होता है, वह पूण्य का हेतु है। उसमें स्व-पर-कल्याण का सौरभ महकता है। इसीलिए आचार्य हरिभद्र ने धर्मबिन्दु में कहा है--न्यायोपात्त धन व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों ही लोकों में हित-साधन करता है--
"न्यायोपात्तं हि वित्तमुभयलोकहिताय ।" भगवान महावीर के गृहस्थ साधक अर्थात् श्रावक इसी आदर्श को लेकर चले थे। संपत्ति रखना, किन्तु उसका विस्तार न करना, यह था उनका आदर्श। व्यापार में यदि वृद्धि या विस्तार होता है, खर्च काटकर अतिरिक्त लाभ होता है, तो वह जनता का होगा, जनता के हित में होगा, हमारा नहीं, यह था उनका अपरिग्रही चिन्तन। गांधीजी के शब्दों में यह ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त हो सकता है, थोड़े से हेर-फेर के साथ। भगवान् महावीर ने इसे अणु-अपरिग्रह के रूप में स्वीकृति दी। यह पूर्ण अपरिग्रह व्रत का प्रथम चरण है।
राष्ट्र के अर्थतंत्र के सम्बन्ध में भगवान महावीर का यह इच्छा परिमाण या परिग्रह परिमाण का उदात्त सिद्धान्त एक व्यवहारिक सिद्धान्त है। यह संग्रह और असंग्रह की दोनों एकान्त अतियों से बचाता है, सामाजिक जीवन को। यह अतीत आदि के किसी विशेष काल-खण्ड से ही सम्बन्धित नहीं है। और न किसी देश विशेष की सीमा में ही आबद्ध है। यह सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक सिद्धान्त है। आज की राष्ट्रीय सरकारें अपनेअपने अर्थतंत्र के सम्बन्ध में भगवान महावीर के उक्त अनतिवादी महान अपरिग्रह-सूत्र का यदि प्रामाणिकता के उज्ज्वल प्रकाश में उपयोग करें, तो हर राष्ट्र के जन-जीवन का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।
बनता है। अ. गांव की क्षुद्र तला साथ सम्बन्धित वैयक्तिक आसक्ति
१२२
सागर, नौका और नाविक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org