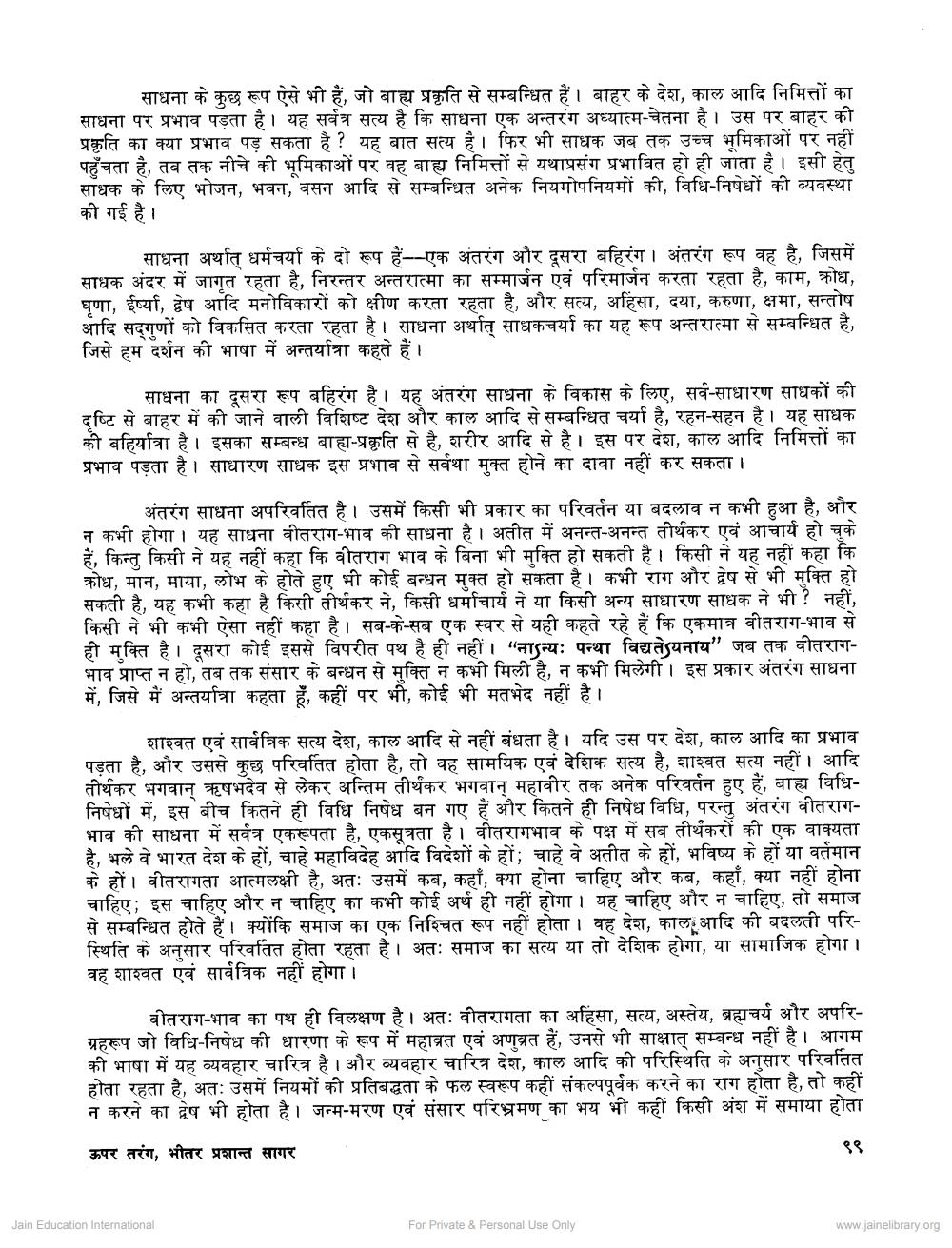________________
साधना के कुछ रूप ऐसे भी हैं, जो बाह्य प्रकृति से सम्बन्धित हैं। बाहर के देश, काल आदि निमित्तों का साधना पर प्रभाव पड़ता है । यह सर्वत्र सत्य है कि साधना एक अन्तरंग अध्यात्म चेतना है । उस पर बाहर की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह बात सत्य है। फिर भी साधक जब तक उच्च भूमिकाओं पर नहीं पहुँचता है, तब तक नीचे की भूमिकाओं पर वह बाह्य निमित्तों से यथाप्रसंग प्रभावित हो ही जाता है। इसी हेतु साधक के लिए भोजन, भवन, वसन आदि से सम्बन्धित अनेक नियमोपनियमों की विधि-निषेधों की व्यवस्था की गई है।
,
साधना अर्थात् धर्मचर्या के दो रूप हैं--एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग अंतरंग रूप वह है, जिसमें साधक अंदर में जागृत रहता है, निरन्तर अन्तरात्मा का सम्मार्जन एवं परिमार्जन करता रहता है, काम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकारों को क्षीण करता रहता है, और सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा, सन्तोष आदि सद्गुणों को विकसित करता रहता है। साधना अर्थात् साधकचर्या का यह रूप अन्तरात्मा से सम्बन्धित है, जिसे हम दर्शन की भाषा में अन्तर्यात्रा कहते हैं ।
साधना का दूसरा रूप बहिरंग है। यह अंतरंग साधना के विकास के लिए, सर्व साधारण साधकों की दृष्टि से बाहर में की जाने वाली विशिष्ट देश और काल आदि से सम्बन्धित चर्या है, रहन-सहन है। यह साधक की बहिर्यात्रा है । इसका सम्बन्ध बाह्य - प्रकृति से है, शरीर आदि से है । इस पर देश, काल आदि निमित्तों का प्रभाव पड़ता है । साधारण साधक इस प्रभाव से सर्वथा मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता ।
अंतरंग साधना अपरिवर्तित है । उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव न कभी हुआ है, और न कभी होगा। यह साधना वीतराग-भाव की साधना है। अतीत में अनन्त अनन्त तीर्थंकर एवं आचार्य हो चुके हैं, किन्तु किसी ने यह नहीं कहा कि वीतराग भाव के बिना भी मुक्ति हो सकती है। किसी ने यह नहीं कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ के होते हुए भी कोई बन्धन मुक्त हो सकता है। कभी राग और द्वेष से भी मुक्ति हो सकती है, यह कभी कहा है किसी तीर्थंकर ने, किसी धर्माचार्य ने या किसी अन्य साधारण साधक ने भी ? नहीं, किसी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा है। सब-के-सब एक स्वर से यही कहते रहे हैं कि एकमात्र वीतराग-भाव से ही मुक्ति है दूसरा कोई इससे विपरीत पथ है ही नहीं "नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" जब तक वीतरागभाव प्राप्त न हो, तब तक संसार के बन्धन से मुक्ति न कभी मिली है, न कभी मिलेगी। इस प्रकार अंतरंग साधना में, जिसे में अन्तर्यात्रा कहता हूँ, कहीं पर भी कोई भी मतभेद नहीं है।
शाश्वत एवं सार्वत्रिक सत्य देश, काल आदि से नहीं बंधता है । यदि उस पर देश, काल आदि का प्रभाव पड़ता है, और उससे कुछ परिवर्तित होता है, तो वह सामयिक एवं देशिक सत्य है, शाश्वत सत्य नहीं आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर तक अनेक परिवर्तन हुए हैं, बाह्य विधिनिषेधों में इस बीच कितने ही विधि निषेध बन गए हैं और कितने ही निषेध विधि, परन्तु अंतरंग वीतरागभाव की साधना में सर्वत्र एकरूपता है, एकसूत्रता है। वीतरागभाव के पक्ष में सब तीर्थंकरों की एक वाक्यता है, भले वे भारत देश के हों, चाहे महाविदेह आदि विदेशों के हों; चाहे वे अतीत के हों, भविष्य के हों या वर्तमान के हों। वीतरागता आत्मलक्षी है, अतः उसमें कब, कहां, क्या होना चाहिए और कब, कहाँ, क्या नहीं होना चाहिए; इस चाहिए और न चाहिए का कभी कोई अर्थ ही नहीं होगा। यह चाहिए और न चाहिए, तो समाज से सम्बन्धित होते हैं क्योंकि समाज का एक निश्चित रूप नहीं होता। वह देश, काल आदि की बदलती परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अतः समाज का सत्य या तो देशिक होगा, या सामाजिक होगा। वह शाश्वत एवं सार्वत्रिक नहीं होगा।
वीतराग-भाव का पथ ही विलक्षण है। अतः वीतरागता का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप जो विधि-निषेध की धारणा के रूप में महाव्रत एवं अणुव्रत हैं, उनसे भी साक्षात् सम्बन्ध नहीं है आगम की भाषा में यह व्यवहार चारित्र है और व्यवहार चारित्र देश, काल आदि की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, अतः उसमें नियमों की प्रतिबद्धता के फल स्वरूप कहीं संकल्पपूर्वक करने का राग होता है, तो कहीं न करने का द्वेष भी होता है । जन्म-मरण एवं संसार परिभ्रमण का भय भी कहीं किसी अंश में समाया होता ऊपर तरंग, भीतर प्रशान्त सागर
९९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.