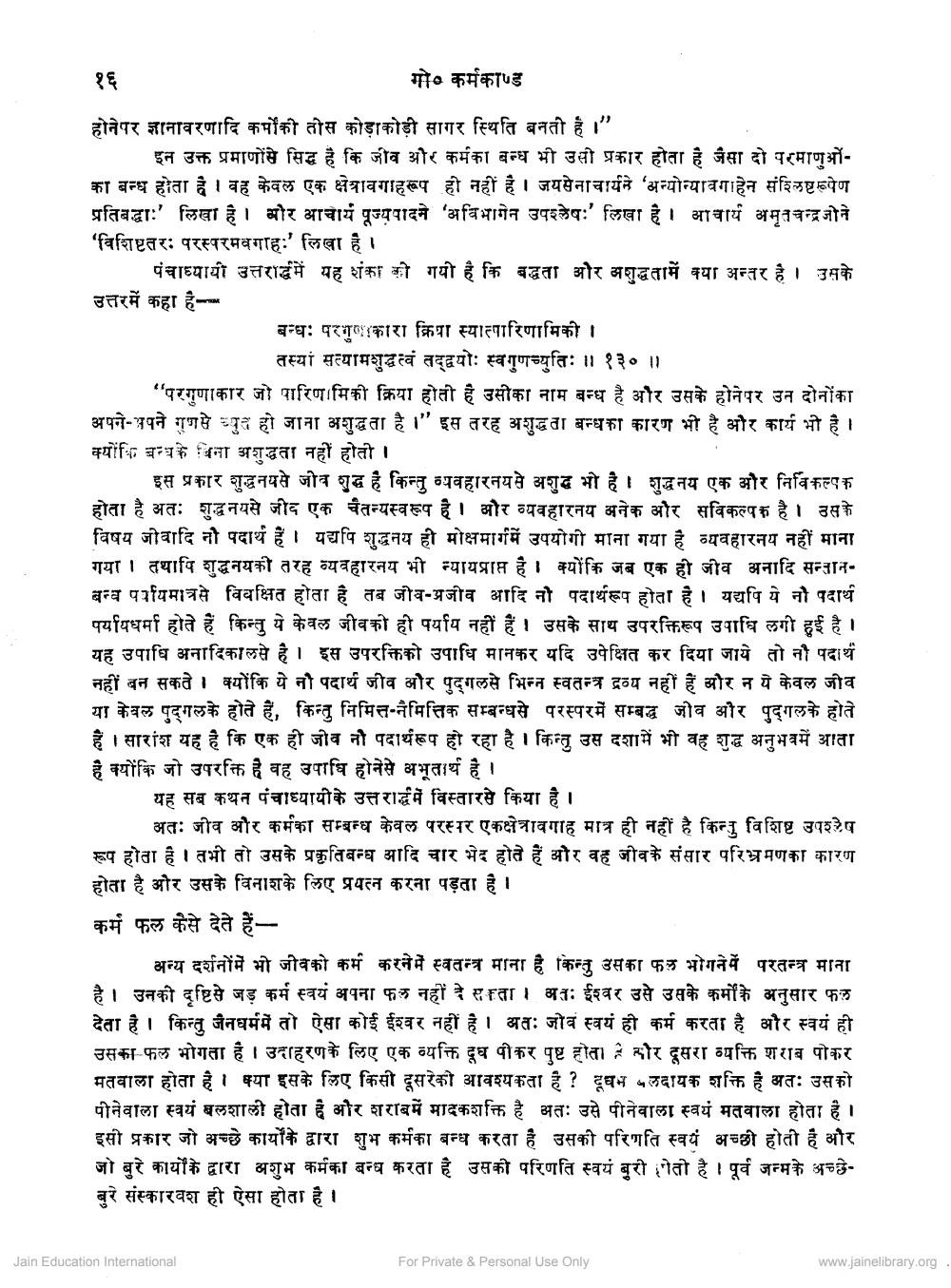________________
गो० कर्मकाण्ड
होने पर ज्ञानावरणादि कर्मोंकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति बनती है।"
इन उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि जीव और कर्मका बन्ध भी उसी प्रकार होता है जैसा दो परमाणुओंका बन्ध होता है। वह केवल एक क्षेत्रावगाहरूप ही नहीं है । जयसेनाचार्यने 'अन्योन्यावगाहेन संश्लिष्टरूपेण प्रतिबद्धाः' लिखा है। और आचार्य पूज्यपादने 'अविभागेन उपश्लेषः' लिखा है। आचार्य अमतचन्द्र जोने 'विशिष्टतरः परस्परमवगाहः' लिखा है।
पंचाध्यायी उत्तरार्द्ध में यह शंका की गयी है कि बद्धता और अशुद्धतामें क्या अन्तर है। उसके उत्तरमें कहा है
बन्धः परगुणाकारा क्रिया स्यात्पारिणामिकी ।
तस्यां सत्यामशुद्धत्वं तद्वयोः स्वगुणच्युतिः ॥ १३० ॥ "परगुणाकार जो पारिणामिकी क्रिया होती है उसीका नाम बन्ध है और उसके होने पर उन दोनोंका अपने-अपने गुण से च्युत हो जाना अशुद्धता है।" इस तरह अशुद्धता बन्धका कारण भी है और कार्य भी है। क्योंकि बन्ध के बिना अशुद्धता नहीं होती।
इस प्रकार शुद्धनयसे जीव शुद्ध है किन्तु व्यवहारनयसे अशुद्ध भो है। शुद्ध नय एक और निर्विकल्पक होता है अतः शुद्ध नयसे जीद एक चैतन्यस्वरूप है। और व्यवहारनय अनेक और सविकल्पक है। उसके विषय जीवादि नौ पदार्थ है। यद्यपि शुद्धनय ही मोक्षमार्गमें उपयोगी माना गया है व्यवहारनय नहीं माना गया । तथापि शुद्धनयकी तरह व्यवहारनय भी न्यायप्राप्त है। क्योंकि जब एक ही जीव अनादि सन्तानबन्ध पर्यायमात्रसे विवक्षित होता है तब जीव-अजीव आदि नौ पदार्थरूप होता है। यद्यपि ये नौ पदार्थ पर्यायधर्मा होते हैं किन्तु ये केवल जीवको ही पर्याय नहीं हैं। उसके साथ उपरक्तिरूप उपाधि लगी हुई है । यह उपाधि अनादिकालसे है। इस उपरक्तिको उपाधि मानकर यदि उपेक्षित कर दिया जाये तो नौ पदार्थ नहीं बन सकते। क्योंकि ये नौ पदार्थ जीव और पुद्गलसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं और न ये केवल जीव या केवल पुद्गलके होते हैं, किन्तु निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धसे परस्परमें सम्बद्ध जीव और पुद्गलके होते है । सारांश यह है कि एक ही जीव नौ पदार्थरूप हो रहा है। किन्तु उस दशा में भी वह शुद्ध अनुभवमें आता है क्योंकि जो उपरक्ति है वह उपाधि होनेसे अभूतार्थ है।
यह सब कथन पंचाध्यायीके उत्तरार्द्ध में विस्तारसे किया है।
अतः जीव और कर्मका सम्बन्ध केवल परस्सर एकक्षेत्रावगाह मात्र ही नहीं है किन्तु विशिष्ट उपश्रेष रूप होता है। तभी तो उसके प्रकृतिबन्ध आदि चार भेद होते हैं और वह जीवके संसार परिभ्रमणका कारण होता है और उसके विनाशके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कर्म फल कैसे देते हैं
अन्य दर्शनों में भी जीवको कर्म करने में स्वतन्त्र माना है किन्तु उसका फल भोगने में परतन्त्र माना है। उनकी दृष्टि से जड़ कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे साता। अतः ईश्वर उसे उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। किन्तु जैनधर्ममें तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है । अतः जोव स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है । उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दूध पीकर पुष्ट होता है और दूसरा व्यक्ति शराब पीकर मतवाला होता है। क्या इसके लिए किसी दूसरेको आवश्यकता है ? दूधभ लदायक शक्ति है अतः उसको पीनेवाला स्वयं बलशाली होता है और शराबमें मादकशक्ति है अतः उसे पीनेवाला स्वयं मतवाला होता है । इसी प्रकार जो अच्छे कार्योंके द्वारा शुभ कर्मका बन्ध करता है उसकी परिणति स्वयं अच्छी होती है और जो बुरे कार्यों के द्वारा अशुभ कर्मका बन्ध करता है उसकी परिणति स्वयं बरी तो है। पूर्व जन्म के अच्छेबुरे संस्कारवश ही ऐसा होता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org .