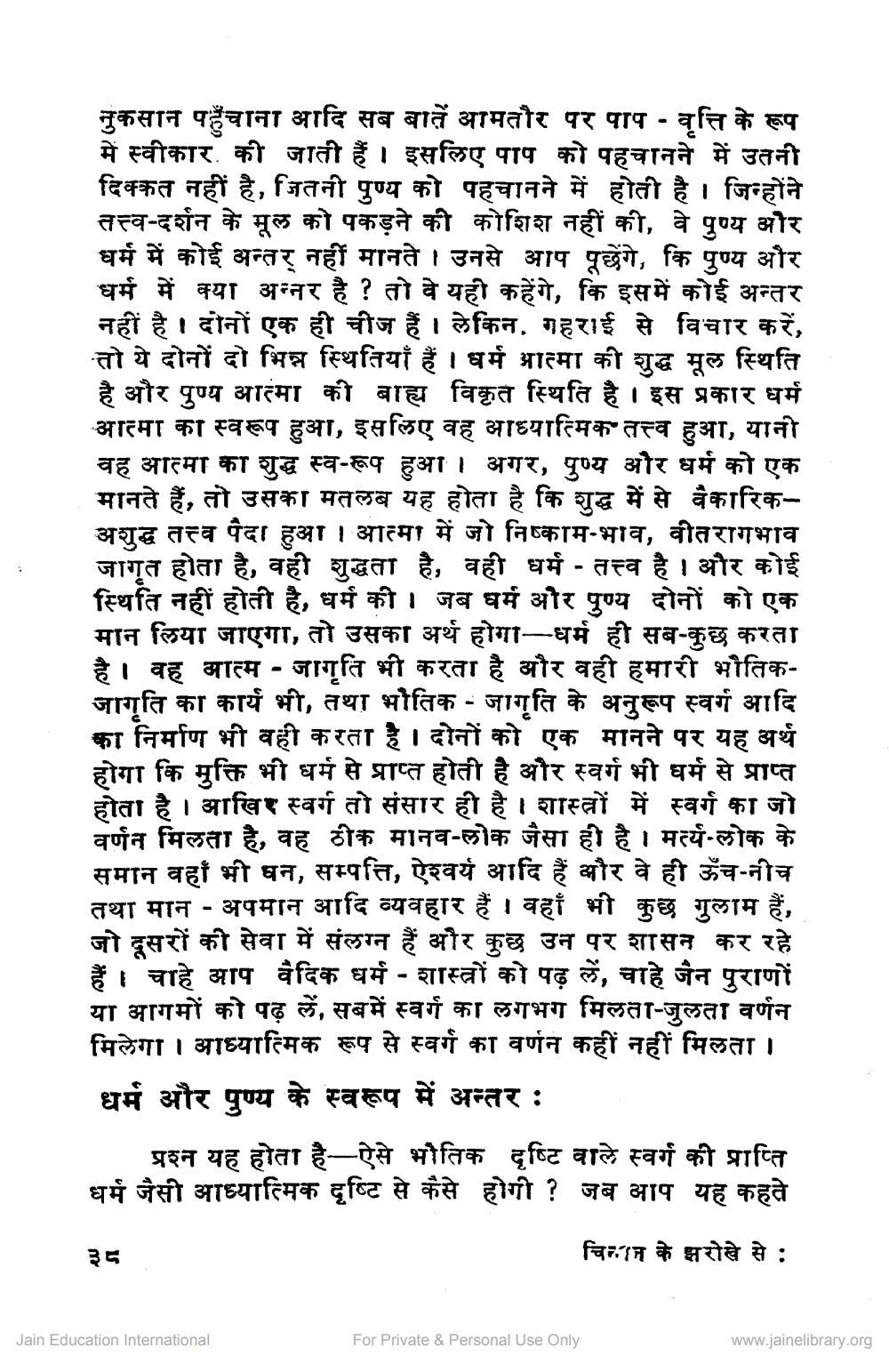________________
नुकसान पहुँचाना आदि सब बातें आमतौर पर पाप - वृत्ति के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इसलिए पाप को पहचानने में उतनी दिक्कत नहीं है, जितनी पुण्य को पहचानने में होती है। जिन्होंने तत्त्व-दर्शन के मूल को पकड़ने की कोशिश नहीं की, वे पुण्य और धर्म में कोई अन्तर नहीं मानते। उनसे आप पूछेगे, कि पुण्य और धर्म में क्या अन्नर है ? तो वे यही कहेंगे, कि इसमें कोई अन्तर नहीं है। दोनों एक ही चीज हैं । लेकिन, गहराई से विचार करें, तो ये दोनों दो भिन्न स्थितियाँ हैं । धर्म आत्मा की शुद्ध मूल स्थिति है और पुण्य आत्मा की बाह्य विकृत स्थिति है । इस प्रकार धर्म आत्मा का स्वरूप हुआ, इसलिए वह आध्यात्मिक तत्त्व हुआ, यानी वह आत्मा का शुद्ध स्व-रूप हुआ। अगर, पुण्य और धर्म को एक मानते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि शुद्ध में से वैकारिकअशुद्ध तत्त्व पैदा हुआ। आत्मा में जो निष्काम-भाव, वीतरागभाव जागृत होता है, वही शुद्धता है, वही धर्म - तत्त्व है । और कोई स्थिति नहीं होती है, धर्म की। जब धर्म और पुण्य दोनों को एक मान लिया जाएगा, तो उसका अर्थ होगा-धर्म ही सब-कुछ करता है। वह आत्म - जागृति भी करता है और वही हमारी भौतिकजागति का कार्य भी, तथा भौतिक - जागति के अनुरूप स्वर्ग आदि का निर्माण भी वही करता है। दोनों को एक मानने पर यह अर्थ होगा कि मुक्ति भी धर्म से प्राप्त होती है और स्वर्ग भी धर्म से प्राप्त होता है। आखिर स्वर्ग तो संसार ही है। शास्त्रों में स्वर्ग का जो वर्णन मिलता है, वह ठीक मानव-लोक जैसा ही है। मर्त्य-लोक के समान वहाँ भी धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि हैं और वे ही ऊँच-नीच तथा मान - अपमान आदि व्यवहार हैं । वहाँ भी कुछ गुलाम हैं, जो दूसरों की सेवा में संलग्न हैं और कुछ उन पर शासन कर रहे हैं। चाहे आप वैदिक धर्म - शास्त्रों को पढ़ लें, चाहे जैन पुराणों या आगमों को पढ़ लें, सबमें स्वर्ग का लगभग मिलता-जुलता वर्णन मिलेगा। आध्यात्मिक रूप से स्वर्ग का वर्णन कहीं नहीं मिलता। धर्म और पुण्य के स्वरूप में अन्तर :
प्रश्न यह होता है-ऐसे भौतिक दृष्टि वाले स्वर्ग की प्राप्ति धर्म जैसी आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे होगी ? जब आप यह कहते
चिनान के झरोखे से :
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org