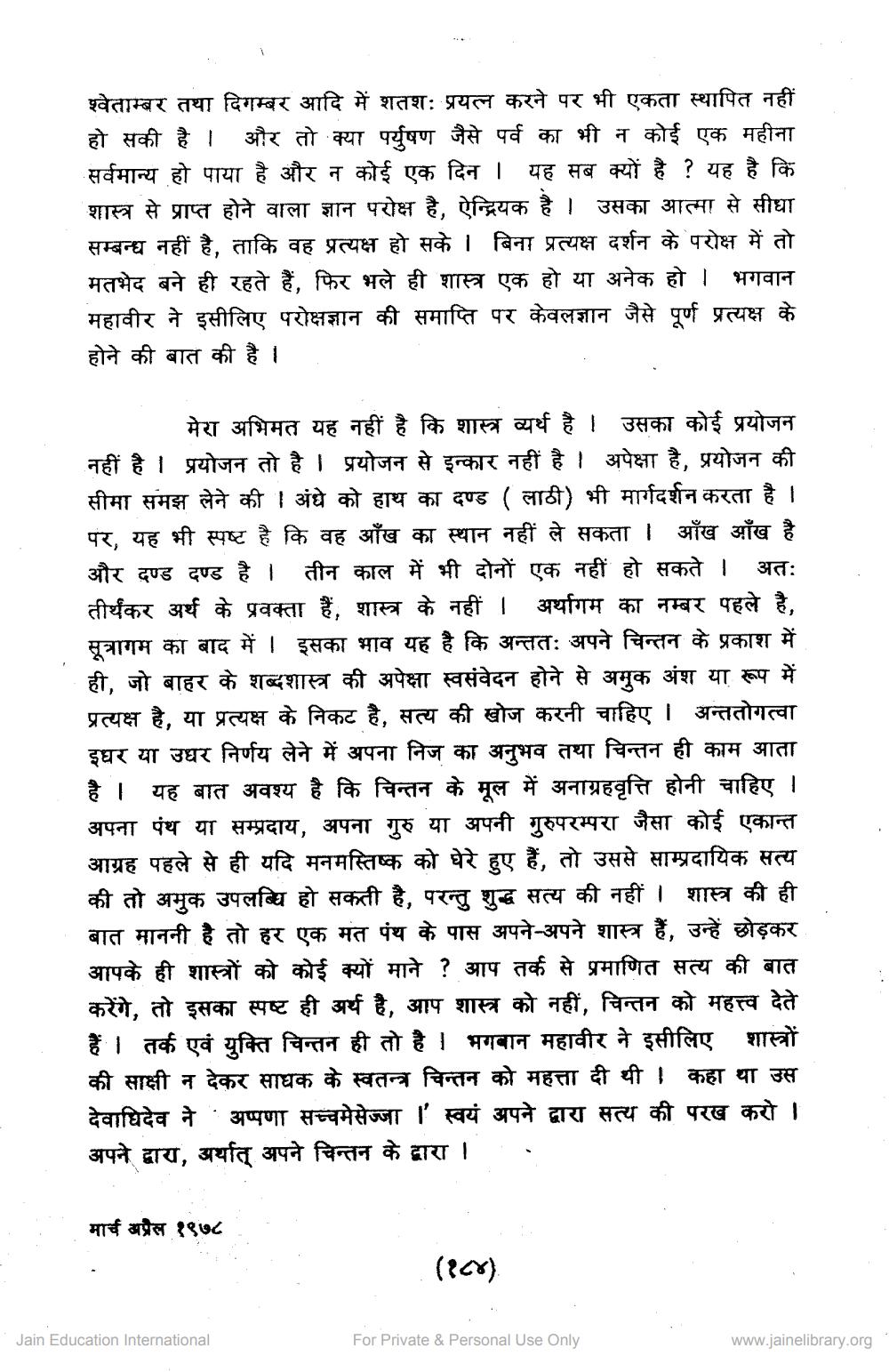________________
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर आदि में शतश: प्रयत्न करने पर भी एकता स्थापित नहीं हो सकी है । और तो क्या पर्युषण जैसे पर्व का भी न कोई एक महीना सर्वमान्य हो पाया है और न कोई एक दिन । यह सब क्यों है ? यह है कि शास्त्र से प्राप्त होने वाला ज्ञान परोक्ष है, ऐन्द्रियक है । उसका आत्मा से सीधा सम्बन्ध नहीं है, ताकि वह प्रत्यक्ष हो सके । बिना प्रत्यक्ष दर्शन के परोक्ष में तो मतभेद बने ही रहते हैं, फिर भले ही शास्त्र एक हो या अनेक हो । भगवान महावीर ने इसीलिए परोक्षज्ञान की समाप्ति पर केवलज्ञान जैसे पूर्ण प्रत्यक्ष के होने की बात की है ।
मेरा अभिमत यह नहीं है कि शास्त्र व्यर्थ है
।
उसका कोई प्रयोजन अपेक्षा है, प्रयोजन की
नहीं है । प्रयोजन तो है । प्रयोजन से इन्कार नहीं है । सीमा समझ लेने की । अंधे को हाथ का दण्ड ( लाठी) भी मार्गदर्शन करता है । पर, यह भी स्पष्ट है कि वह आँख का स्थान नहीं ले सकता । आँख आँख है और दण्ड दण्ड है । तीन काल में भी दोनों एक नहीं हो सकते । अतः तीर्थंकर अर्थ के प्रवक्ता हैं, शास्त्र के नहीं । अर्थागम का नम्बर पहले है, सूत्रागम का बाद में । इसका भाव यह है कि अन्ततः अपने चिन्तन के प्रकाश में ही, जो बाहर के शब्दशास्त्र की अपेक्षा स्वसंवेदन होने से अमुक अंश या रूप में प्रत्यक्ष है, या प्रत्यक्ष के निकट है, सत्य की खोज करनी चाहिए । अन्ततोगत्वा इधर या उधर निर्णय लेने में अपना निज का अनुभव तथा चिन्तन ही काम आता है । यह बात अवश्य है कि चिन्तन के मूल में अनाग्रहवृत्ति होनी चाहिए । अपना पंथ या सम्प्रदाय, अपना गुरु या अपनी गुरुपरम्परा जैसा कोई एकान्त आग्रह पहले से ही यदि मनमस्तिष्क को घेरे हुए हैं, तो उससे साम्प्रदायिक सत्य की तो अमुक उपलब्धि हो सकती है, परन्तु शुद्ध सत्य की नहीं । शास्त्र की ही बात माननी है तो हर एक मत पंथ के पास अपने-अपने शास्त्र हैं, उन्हें छोड़कर आपके ही शास्त्रों को कोई क्यों माने ? आप तर्क से प्रमाणित सत्य की बात करेंगे, तो इसका स्पष्ट ही अर्थ है, आप शास्त्र को नहीं, चिन्तन को महत्त्व देते हैं । तर्क एवं युक्ति चिन्तन ही तो है । भगवान महावीर ने इसीलिए शास्त्रों की साक्षी न देकर साधक के स्वतन्त्र चिन्तन को महत्ता दी थी । कहा था उस देवाधिदेव ने अप्पणा सच्चमेसेज्जा ।' स्वयं अपने द्वारा सत्य की
परख करो ।
अपने द्वारा, अर्थात् अपने चिन्तन के द्वारा |
मार्च अप्रैल १९७८
Jain Education International
(१८४)
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org