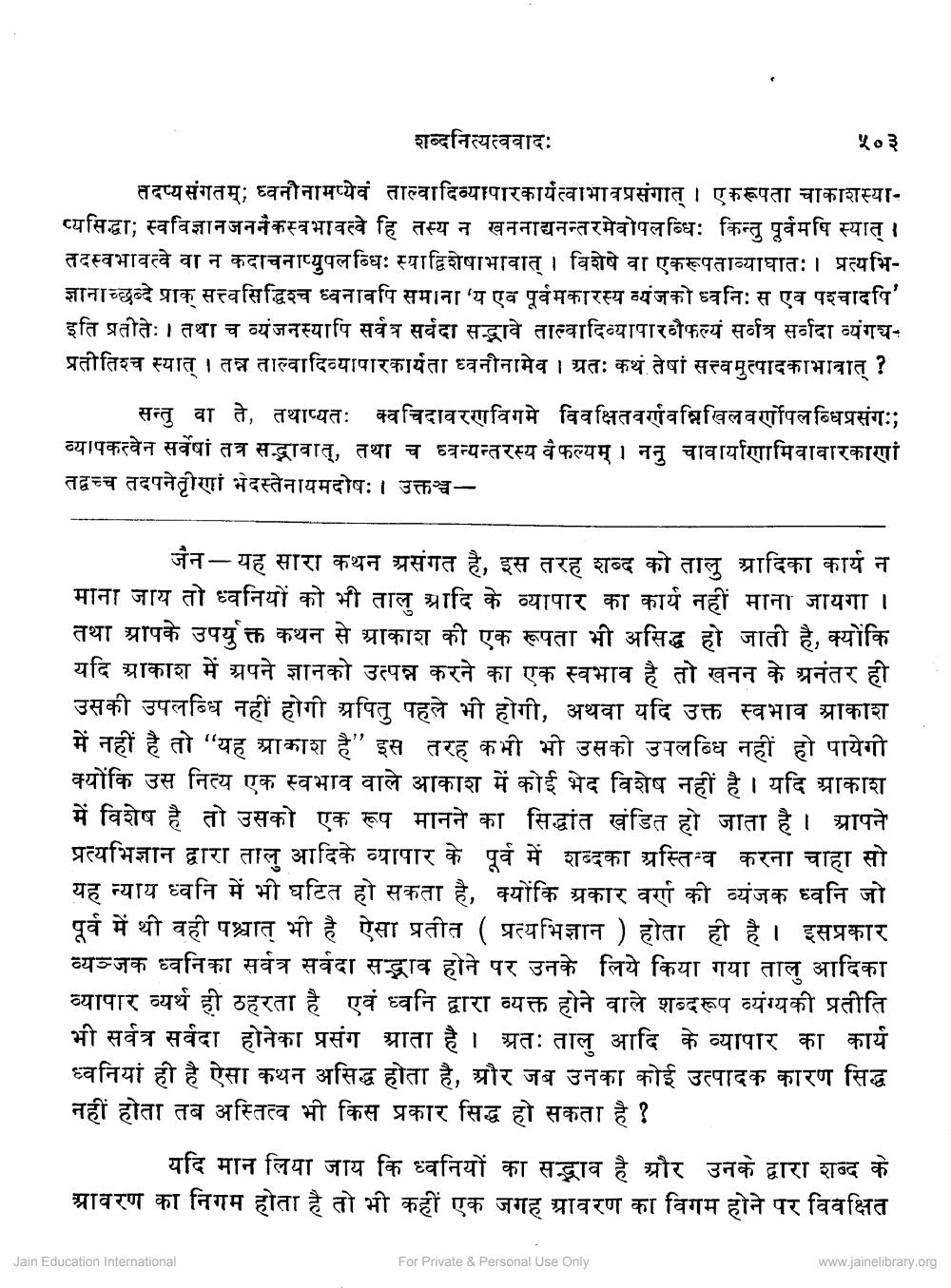________________
शब्दनित्यत्ववादः
५०३
तदप्यसंगतम्; ध्वनीनामप्येवं ताल्वादिव्यापारकार्यत्वाभावप्रसंगात् । एकरूपता चाकाशस्याप्यसिद्धा; स्वविज्ञानजननै कस्वभावत्वे हि तस्य न खननाद्यनन्तरमेवोपलब्धिः किन्तु पूर्वमपि स्यात् । तदस्वभावत्वे वा न कदाचनाप्युपलब्धिः स्याद्विशेषाभावात् । विशेषे वा एकरूपताव्याघातः । प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दे प्राक् सत्त्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना 'य एवं पूर्वमकारस्य व्यंजको ध्वनिः स एव पश्चादपि' इति प्रतीतेः । तथा च व्यंजनस्यापि सर्वत्र सर्वदा सद्भावे ताल्वादिव्यापारमैफल्यं सर्वत्र सर्वदा व्यंगयप्रतीतिश्च स्यात् । तन्न ताल्वादिव्यापारकार्यता ध्वनीनामेव । अतः कथं तेषां सत्त्वमुत्पादकाभावात् ?
सन्तु वा ते, तथाप्यतः क्वचिदावरणविगमे विवक्षितवर्णवनिखिल वर्णोपलब्धिप्रसंगः; व्यापकत्वेन सर्वेषां तत्र सद्भावात्, तथा च ध्वन्यन्तरस्य वैफल्यम् । ननु चावार्यारणामिवावारकाणां तद्वच्च तदपनेतीणां भेदस्तेनायमदोषः। उक्तञ्च
जैन- यह सारा कथन असंगत है, इस तरह शब्द को तालु आदिका कार्य न माना जाय तो ध्वनियों को भी तालु आदि के व्यापार का कार्य नहीं माना जायगा । तथा आपके उपर्युक्त कथन से आकाश की एक रूपता भी असिद्ध हो जाती है, क्योंकि यदि आकाश में अपने ज्ञानको उत्पन्न करने का एक स्वभाव है तो खनन के अनंतर ही उसकी उपलब्धि नहीं होगी अपितु पहले भी होगी, अथवा यदि उक्त स्वभाव आकाश में नहीं है तो “यह आकाश है" इस तरह कभी भी उसको उपलब्धि नहीं हो पायेगी क्योंकि उस नित्य एक स्वभाव वाले आकाश में कोई भेद विशेष नहीं है। यदि आकाश में विशेष है तो उसको एक रूप मानने का सिद्धांत खंडित हो जाता है। आपने प्रत्यभिज्ञान द्वारा तालु आदिके व्यापार के पूर्व में शब्दका अस्तित्व करना चाहा सो यह न्याय ध्वनि में भी घटित हो सकता है, क्योंकि प्रकार वर्ण की व्यंजक ध्वनि जो पूर्व में थी वही पश्चात् भी है ऐसा प्रतीत ( प्रत्यभिज्ञान ) होता ही है। इसप्रकार व्यञ्जक ध्वनिका सर्वत्र सर्वदा सद्भाव होने पर उनके लिये किया गया तालु आदिका व्यापार व्यर्थ ही ठहरता है एवं ध्वनि द्वारा व्यक्त होने वाले शब्दरूप व्यंग्य की प्रतीति भी सर्वत्र सर्वदा होनेका प्रसंग आता है। अतः तालु आदि के व्यापार का कार्य ध्वनियां ही है ऐसा कथन असिद्ध होता है, और जब उनका कोई उत्पादक कारण सिद्ध नहीं होता तब अस्तित्व भी किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ?
यदि मान लिया जाय कि ध्वनियों का सद्भाव है और उनके द्वारा शब्द के आवरण का निगम होता है तो भी कहीं एक जगह प्रावरण का विगम होने पर विवक्षित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org