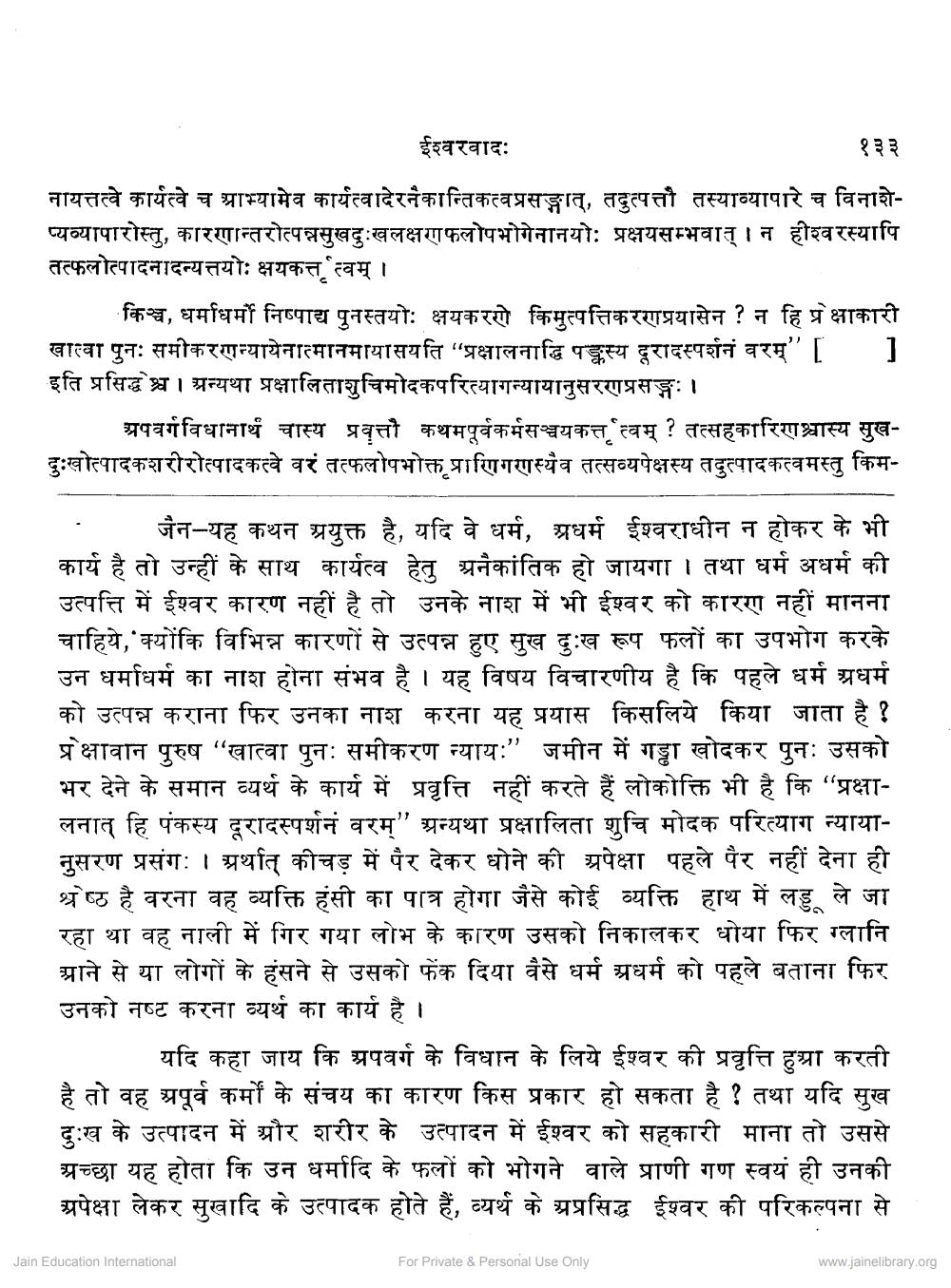________________
ईश्वरवादः नायत्तत्वे कार्यत्वे च प्राभ्यामेव कार्यत्वादेरनैकान्तिकत्वप्रसङ्गात्, तदुत्पत्तौ तस्याव्यापारे च विनाशेप्यव्यापारोस्तु, कारणान्तरोत्पन्नसुखदुःखलक्षण फलोपभोगेनानयोः प्रक्षयसम्भवात् । न हीश्वरस्यापि तत्फलोत्पादनादन्यत्तयोः क्षयकत्त त्वम् ।
किञ्च, धर्माधर्मों निष्पाद्य पुनस्तयोः क्षयकरणे किमुत्पत्तिकरणप्रयासेन ? न हि प्रेक्षाकारी खात्वा पुनः समीकरणन्यायेनात्मानमायासयति "प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' [ ] इति प्रसिद्धश्च । अन्यथा प्रक्षालिताशुचिमोदकपरित्यागन्यायानुसरणप्रसङ्गः।।
अपवर्गविधानार्थं चास्य प्रवृत्तौ कथमपूर्वकर्मसञ्चयकत्त त्वम् ? तत्सहकारिणश्चास्य सुखदुःखोत्पादकशरीरोत्पादकत्वे वरं तत्फलोपभोक्त प्राणिगणस्यैव तत्सव्यपेक्षस्य तदुत्पादकत्वमस्तु किम
- जैन-यह कथन अयुक्त है, यदि वे धर्म, अधर्म ईश्वराधीन न होकर के भी कार्य है तो उन्हीं के साथ कार्यत्व हेतु अनैकांतिक हो जायगा । तथा धर्म अधर्म की उत्पत्ति में ईश्वर कारण नहीं है तो उनके नाश में भी ईश्वर को कारण नहीं मानना चाहिये, क्योंकि विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए सुख दुःख रूप फलों का उपभोग करके उन धर्माधर्म का नाश होना संभव है । यह विषय विचारणीय है कि पहले धर्म अधर्म को उत्पन्न कराना फिर उनका नाश करना यह प्रयास किसलिये किया जाता है ? प्रक्षावान पुरुष "खात्वा पुन: समीकरण न्यायः' जमीन में गड्ढा खोदकर पुनः उसको भर देने के समान व्यर्थ के कार्य में प्रवृत्ति नहीं करते हैं लोकोक्ति भी है कि "प्रक्षालनात् हि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्" अन्यथा प्रक्षालिता शुचि मोदक परित्याग न्यायानुसरण प्रसंगः । अर्थात् कीचड़ में पैर देकर धोने की अपेक्षा पहले पैर नहीं देना ही श्रेष्ठ है वरना वह व्यक्ति हंसी का पात्र होगा जैसे कोई व्यक्ति हाथ में लड्डु ले जा रहा था वह नाली में गिर गया लोभ के कारण उसको निकालकर धोया फिर ग्लानि आने से या लोगों के हंसने से उसको फेंक दिया वैसे धर्म अधर्म को पहले बताना फिर उनको नष्ट करना व्यर्थ का कार्य है।
यदि कहा जाय कि अपवर्ग के विधान के लिये ईश्वर की प्रवृत्ति हुया करती है तो वह अपूर्व कर्मों के संचय का कारण किस प्रकार हो सकता है ? तथा यदि सुख दुःख के उत्पादन में और शरीर के उत्पादन में ईश्वर को सहकारी माना तो उससे अच्छा यह होता कि उन धर्मादि के फलों को भोगने वाले प्राणी गण स्वयं ही उनकी अपेक्षा लेकर सुखादि के उत्पादक होते हैं, व्यर्थ के अप्रसिद्ध ईश्वर की परिकल्पना से
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org