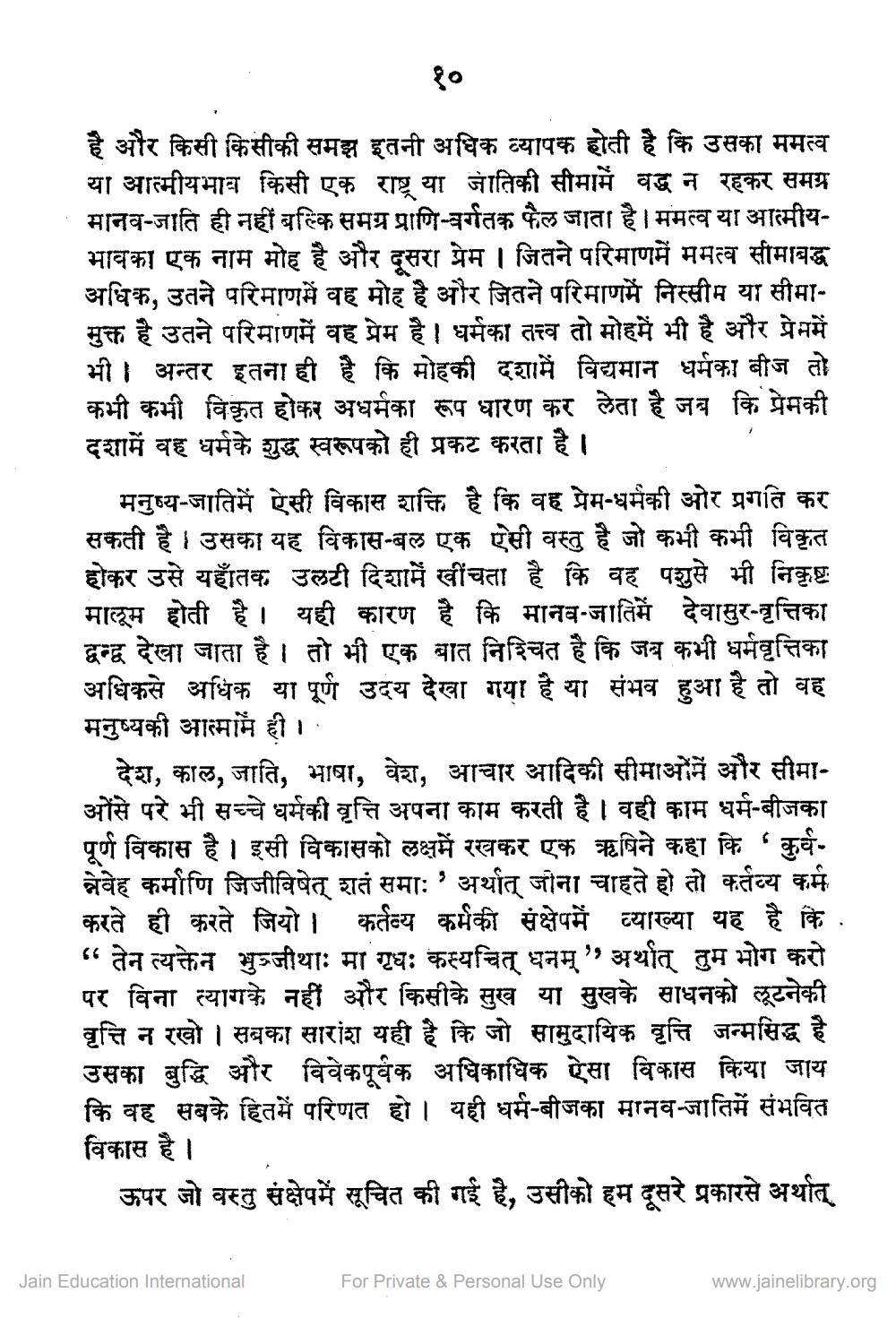________________
१०
है और किसी किसीकी समझ इतनी अधिक व्यापक होती है कि उसका ममत्व या आत्मीयभाव किसी एक राष्ट्र या जातिकी सीमामें वद्ध न रहकर समग्र मानव जाति ही नहीं बल्कि समग्र प्राणि-वर्गतक फैल जाता है। ममत्व या आत्मीयभावका एक नाम मोह है और दूसरा प्रेम । जितने परिमाणमें ममत्व सीमाबद्ध 1 अधिक, उतने परिमाण में वह मोह है और जितने परिमाणमें निस्सीम या सीमामुक्त है उतने परिमाणमें वह प्रेम है । धर्मका तत्त्व तो मोहमें भी है और प्रेममें भी । अन्तर इतना ही है कि मोहकी दशा में विद्यमान धर्मका बीज तो कभी कभी विकृत होकर अधर्मका रूप धारण कर लेता है जब कि प्रेमकी दशामें वह धर्मके शुद्ध स्वरूपको ही प्रकट करता है ।
मनुष्य जाति में ऐसी विकास शक्ति है कि वह प्रेम-धर्मकी ओर प्रगति कर सकती है । उसका यह विकास-बल एक ऐसी वस्तु है जो कभी कभी विकृत होकर उसे यहाँतक उलटी दिशामें खींचता है कि वह पशुसे भी निकृष्ट मालूम होती है । यही कारण है कि मानव जातिमें देवासुर-वृत्तिका द्वन्द्व देखा जाता है । तो भी एक बात निश्चित है कि जब कभी धर्मवृत्तिका अधिक से अधिक या पूर्ण उदय देखा गया है या संभव हुआ है तो वह मनुष्यकी आत्मा ही ।
देश, काल, जाति, भाषा, वेश, आचार आदिकी सीमाओंमें और सीमाओंसे परे भी सच्चे धर्मकी वृत्ति अपना काम करती है । वही काम धर्म - बीजका पूर्ण विकास है । इसी विकासको लक्षमें रखकर एक ऋषिने कहा कि ' कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ' अर्थात् जोना चाहते हो तो कर्तव्य कर्म करते ही करते जियो । कर्तव्य कर्मकी संक्षेपमें व्याख्या यह है कि " तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम् " अर्थात् तुम भोग करो पर विना त्यागके नहीं और किसीके सुख या सुखके साधनको लूटनेकी वृत्ति न रखो । सबका सारांश यही है कि जो सामुदायिक वृत्ति जन्मसिद्ध है उसका बुद्धि और विवेकपूर्वक अधिकाधिक ऐसा विकास किया जाय कि वह सबके हित में परिणत हो । यही धर्म - बीजका मानव जातिमें संभवित विकास है ।
ऊपर जो वस्तु संक्षेपमें सूचित की गई है, उसीको हम दूसरे प्रकारसे अर्थात्
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org