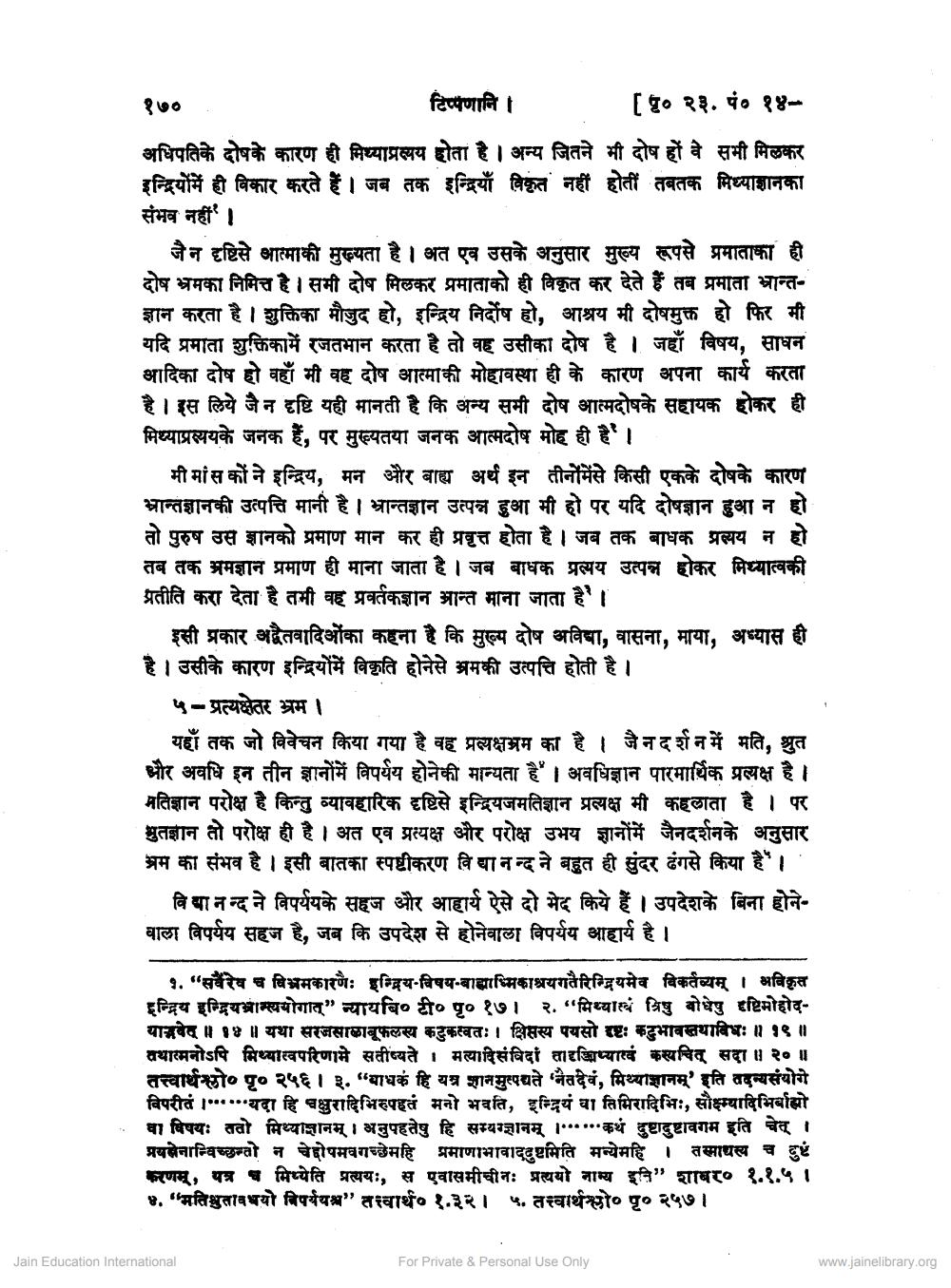________________
१७०
टिप्पणानि ।
[पृ० २३. पं० १४अधिपतिके दोषके कारण ही मिथ्याप्रत्यय होता है। अन्य जितने भी दोष हों वे सभी मिलकर इन्द्रियोंमें ही विकार करते हैं। जब तक इन्द्रियाँ विकृत नहीं होती तबतक मिथ्याज्ञानका संभव नहीं।
जैन दृष्टिसे आत्माकी मुख्यता है । अत एव उसके अनुसार मुख्य रूपसे प्रमाताका ही दोष भ्रमका निमित्त है । समी दोष मिलकर प्रमाताको ही विकृत कर देते हैं तब प्रमाता भ्रान्तज्ञान करता है । शुक्तिका मौजुद हो, इन्द्रिय निर्दोष हो, आश्रय मी दोषमुक्त हो फिर मी यदि प्रमाता शुक्तिकामें रजतमान करता है तो वह उसीका दोष है । जहाँ विषय, साधन आदिका दोष हो वहाँ भी वह दोष आत्माकी मोहावस्था ही के कारण अपना कार्य करता है । इस लिये जैन दृष्टि यही मानती है कि अन्य समी दोष आत्मदोषके सहायक होकर ही मिथ्याप्रत्ययके जनक हैं, पर मुख्यतया जनक आत्मदोष मोह ही है ।
मी मांस कों ने इन्द्रिय, मन और बाह्य अर्थ इन तीनोंमेंसे किसी एकके दोषके कारण भ्रान्तज्ञानकी उत्पत्ति मानी है । भ्रान्तज्ञान उत्पन्न हुआ मी हो पर यदि दोषज्ञान हुआ न हो तो पुरुष उस ज्ञानको प्रमाण मान कर ही प्रवृत्त होता है। जब तक बाधक प्रत्यय न हो तब तक अमज्ञान प्रमाण ही माना जाता है । जब बाधक प्रत्यय उत्पन्न होकर मिथ्यात्वकी प्रतीति करा देता है तमी वह प्रवर्तकज्ञान प्रान्त माना जाता है।
इसी प्रकार अद्वैतवादिओंका कहना है कि मुख्य दोष अविद्या, वासना, माया, अभ्यास ही है । उसीके कारण इन्द्रियों में विकृति होनेसे अमकी उत्पत्ति होती है ।
५- प्रत्यक्षेतर भ्रम। यहाँ तक जो विवेचन किया गया है वह प्रत्यक्षश्रम का है । जैन दर्शन में मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंमें विपर्यय होनेकी मान्यता है । अवधिज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। मतिज्ञान परोक्ष है किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे इन्द्रियजमतिज्ञान प्रत्यक्ष मी कहलाता है । पर भुतज्ञान तो परोक्ष ही है । अत एव प्रत्यक्ष और परोक्ष उभय ज्ञानोंमें जैनदर्शनके अनुसार भ्रम का संभव है । इसी बातका स्पष्टीकरण वि यानन्द ने बहुत ही सुंदर ढंगसे किया है।
विधा नन्द ने विपर्ययके सहज और आहार्य ऐसे दो भेद किये हैं। उपदेशके बिना होनेवाला विपर्यय सहज है, जब कि उपदेश से होनेवाला विपर्यय आहार्य है।
१. "सवैरेव च विभ्रमकारणैः इन्द्रिय-विषय-बाह्माध्मिकाश्रयगतैरिन्द्रियमेव विकर्तव्यम् । अविकृत इन्द्रिय इन्द्रियनान्स्ययोगात्" न्यायबि० टी० पृ०१७। २. "मिथ्यात्वं त्रिषु बोधेषु दृष्टिमोहोदयानवेत् ॥ १४ ॥ यथा सरजसाकाबूफलस्य कटुकस्वतः। क्षितस्य पयसो बटः कटुभावस्तथाविधः ॥ १९॥ तथारमनोऽपि मिथ्यास्वपरिणामे सतीप्यते । मत्यादिसंविदां तादृचिभ्यावं कस्यचित् सदा ॥२०॥ तत्त्वार्थश्लो० पृ०२५६ । ३. "याधकं हि यत्र ज्ञानमुत्पद्यते 'नैतदेवं, मिथ्याज्ञानम्' इति तदन्यसंयोगे
विपरीतं ..."यदा हि चक्षुरादिभिरूपहतं मनो भवति, इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सौम्यादिभिर्बाझो .. वा विषयः ततो मिथ्याज्ञानम् । अनुपहतेषु हि सम्यग्ज्ञानम् ।.......कथं दुष्टादुष्टावगम इति चेत् ।
प्रयलेनान्विच्छन्तो न चेहोषमवगच्छेमहि प्रमाणाभावाददुष्टमिति मन्येमहि । तमाघस्य च दुष्टं करणम् , पत्र व मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययो नाम्य इनि" शाबर० १.१.५ । १. "मतिश्रुतावश्चयो विपर्ययन" तत्वार्थ० १.३२। ५. तत्त्वार्थश्लो० पृ०२५७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org