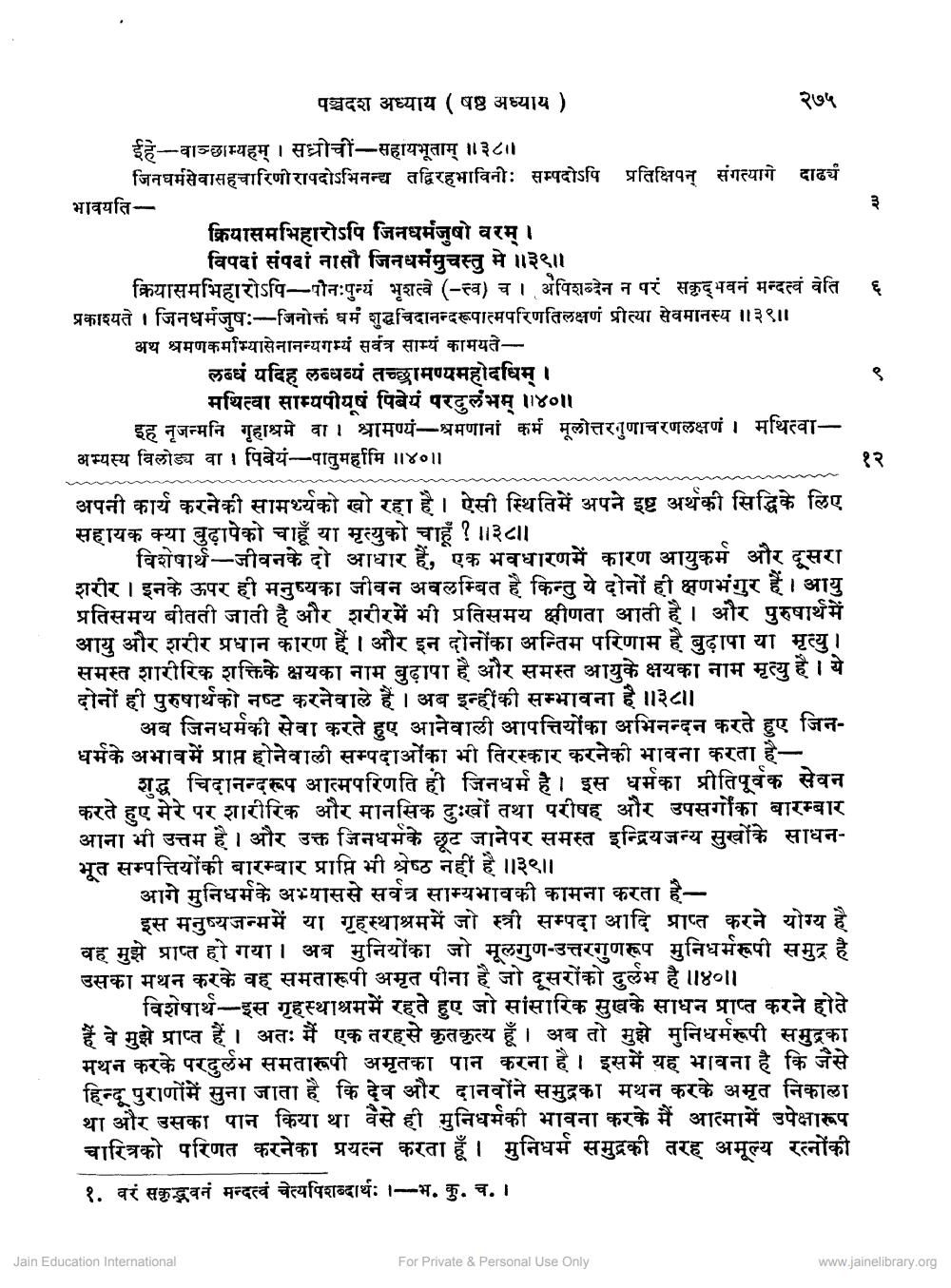________________
पञ्चदश अध्याय ( षष्ठ अध्याय )
ईहे - वाञ्छाम्यहम् । सधीचीं -सहायभूताम् ॥ ३८ ॥
जिनधर्म सेवा सहचारिणीरापदोऽभिनन्द्य तद्विरहभाविनीः सम्पदोऽपि प्रतिक्षिपन् संगत्यागे दाढर्य भावयति -
२७५
क्रियासमभिहारोऽपि जिनधर्मजुषो वरम् । विपदां संपदां नासौ जिनधर्ममुचस्तु मे ॥३९॥ क्रियासमभिहारोऽपि - पौनःपुन्यं भृशत्वे (त्व) च । अपिशब्देन न परं सकृद्भवनं मन्दत्वं वेति प्रकाश्यते | जिनधर्मजुषः - जिनोक्तं धर्मं शुद्धचिदानन्दरूपात्मपरिणतिलक्षणं प्रीत्या सेवमानस्य ॥ ३९ ॥ अथ श्रमणकर्माभ्यासेनानन्यगभ्यं सर्वत्र साम्यं कामयते—
६
लब्धं यदि लब्धव्यं तच्छ्रामण्यमहोदधिम् । मथित्वा साम्यपीयूषं पिबेयं परदुर्लभम् ॥ ४० ॥
इह नृजन्मनि गृहाश्रमे वा । श्रामण्यं श्रमणानां कर्म मूलोत्तरगुणाचरणलक्षणं । मथित्वा - अभ्यस्य विलोड्य वा । पिबेयं -- पातुमहमि ॥४०॥
Jain Education International
अपनी कार्य करने की सामर्थ्यको खो रहा है । ऐसी स्थिति में अपने इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिए सहायक क्या बुढ़ापेको चाहूँ या मृत्युको चाहूँ ? ||३८||
विशेषार्थ - जीवनके दो आधार हैं, एक भवधारणमें कारण आयुकर्म और दूसरा शरीर । इनके ऊपर ही मनुष्यका जीवन अवलम्बित है किन्तु ये दोनों ही क्षणभंगुर हैं । आयु प्रतिसमय बीतती जाती है और शरीर में भी प्रतिसमय क्षीणता आती है । और पुरुषार्थ में आयु और शरीर प्रधान कारण हैं । और इन दोनोंका अन्तिम परिणाम है बुढ़ापा या मृत्यु | समस्त शारीरिक शक्तिके क्षयका नाम बुढ़ापा है और समस्त आयुके क्षयका नाम मृत्यु है । ये दोनों ही पुरुषार्थको नष्ट करनेवाले हैं । अब इन्हींकी सम्भावना है ॥३८॥
अब जिनधर्मकी सेवा करते हुए आनेवाली आपत्तियोंका अभिनन्दन करते हुए जिनधर्मके अभाव में प्राप्त होनेवाली सम्पदाओंका भी तिरस्कार करनेकी भावना करता है -
शुद्ध चिदानन्दरूप आत्मपरिणति ही जिनधर्म है। इस धर्मका प्रीतिपूर्वक सेवन करते हुए मेरे पर शारीरिक और मानसिक दुःखों तथा परीषह और उपसर्गोंका बारम्बार आना भी उत्तम है । और उक्त जिनधर्मके छूट जानेपर समस्त इन्द्रियजन्य सुखोंके साधनभूत सम्पत्तियों की बारम्बार प्राप्ति भी श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३९ ॥
आगे मुनिधर्म के अभ्यास से सर्वत्र साम्यभावकी कामना करता है -
इस मनुष्यजन्म में या गृहस्थाश्रम में जो स्त्री सम्पदा आदि प्राप्त करने योग्य है वह मुझे प्राप्त हो गया । अब मुनियोंका जो मूलगुण- उत्तरगुणरूप मुनिधर्मरूपी समुद्र है उसका मथन करके वह समतारूपी अमृत पीना है जो दूसरोंको दुर्लभ है ॥४०॥
विशेषार्थ - - इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो सांसारिक सुखके साधन प्राप्त करने होते हैं वे मुझे प्राप्त हैं । अतः मैं एक तरह से कृतकृत्य हूँ । अब तो मुझे मुनिधर्मरूपी समुद्रका मथन करके परदुर्लभ समतारूपी अमृतका पान करना है । इसमें यह भावना है कि जैसे हिन्दू पुराणोंमें सुना जाता है कि देव और दानवोंने समुद्रका मथन करके अमृत निकाला था और उसका पान किया था वैसे ही मुनिधर्मकी भावना करके मैं आत्मामें उपेक्षारूप चारित्रको परिणत करनेका प्रयत्न करता हूँ | मुनिधर्म समुद्रकी तरह अमूल्य रत्नोंकी १. वरं सकृद्भवनं मन्दत्वं चेत्यपिशब्दार्थः । भ. कु. च. ।
For Private & Personal Use Only
३
१२
www.jainelibrary.org