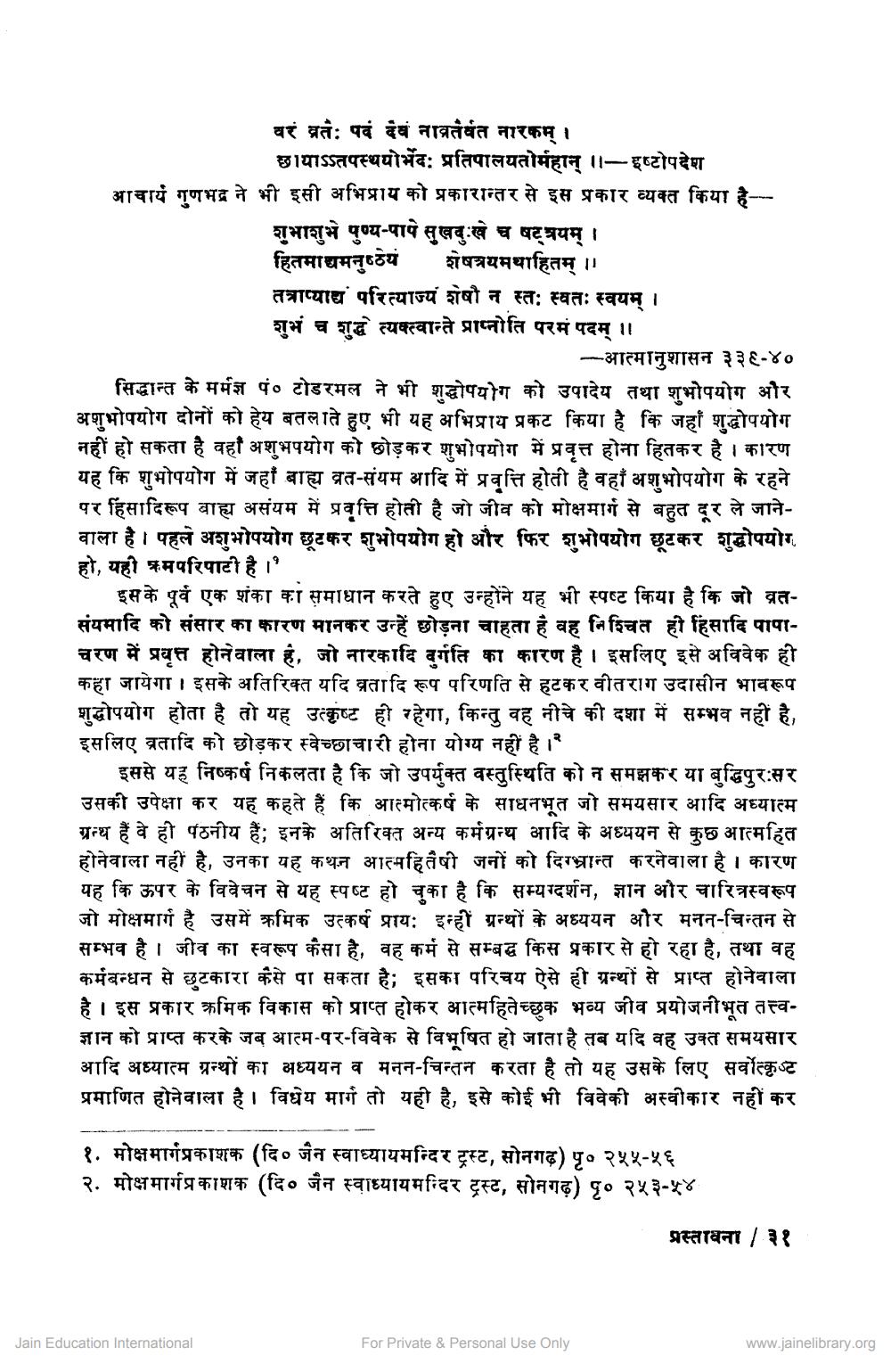________________
वरं व्रतः पदं देवं नावतर्वत नारकम् ।
छायाऽऽतपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ।। - इष्टोपदेश आचार्य गुणभद्र ने भी इसी अभिप्राय को प्रकारान्तर से इस प्रकार व्यक्त किया है---
शुभाशुभे पुण्य-पापे सुखदुःखे च षट्त्रयम् । हितमाधमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम् ।। तत्राप्याद्य परित्याज्यं शेषौ न स्त: स्वतः स्वयम् । शुभं च शुद्ध त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ।।
-आत्मानुशासन ३३६-४० सिद्धान्त के मर्मज्ञ पं० टोडरमल ने भी शुद्धोपयोग को उपादेय तथा शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को हेय बतलाते हुए भी यह अभिप्राय प्रकट किया है कि जहाँ शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है वहाँ अशुभपयोग को छोड़ कर शुभोपयोग में प्रवृत्त होना हितकर है । कारण यह कि शुभोपयोग में जहाँ बाह्य व्रत-संयम आदि में प्रवृत्ति होती है वहाँ अशुभोपयोग के रहने पर हिंसादिरूप बाह्य असंयम में प्रवृत्ति होती है जो जीव को मोक्षमार्ग से बहुत दूर ले जानेवाला है। पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो और फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग, हो, यही क्रमपरिपाटी है।'
इस के पूर्व एक शंका का समाधान करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो व्रतसंयमादि को संसार का कारण मानकर उन्हें छोड़ना चाहता है वह निश्चित ही हिंसादि पापाचरण में प्रवृत्त होने वाला है, जो नारकादि वर्गति का कारण है । इसलिए इसे अविवेक ही कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि व्रतादि रूप परिणति से हटकर वीतराग उदासीन भावरूप शुद्धोपयोग होता है तो यह उत्कृष्ट ही रहेगा, किन्तु वह नीचे की दशा में सम्भव नहीं है, इसलिए व्रतादि को छोड़कर स्वेच्छाचारी होना योग्य नहीं है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो उपर्युक्त वस्तुस्थिति को न समझकर या बुद्धिपुरःसर उसकी उपेक्षा कर यह कहते हैं कि आत्मोत्कर्ष के साधनभूत जो समयसार आदि अध्यात्म ग्रन्थ हैं वे ही पठनीय हैं; इनके अतिरिक्त अन्य कर्मग्रन्थ आदि के अध्ययन से कुछ आत्महित होनेवाला नहीं है, उनका यह कथन आत्महितैषी जनों को दिग्भ्रान्त करनेवाला है। कारण यह कि ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रस्वरूप जो मोक्षमार्ग है उसमें क्रमिक उत्कर्ष प्रायः इन्हीं ग्रन्थों के अध्ययन और मनन-चिन्तन से सम्भव है। जीव का स्वरूप कैसा है, वह कर्म से सम्बद्ध किस प्रकार से हो रहा है, तथा वह कर्मबन्धन से छटकारा कैसे पा सकता है। इसका परिचय ऐसे ही ग्रन्थों से प्राप्त होनेवाला है । इस प्रकार क्रमिक विकास को प्राप्त होकर आत्महितेच्छुक भव्य जीव प्रयोजनीभूत तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके जब आत्म-पर-विवेक से विभूषित हो जाता है तब यदि वह उक्त समयसार आदि अध्यात्म ग्रन्थों का अध्ययन व मनन-चिन्तन करता है तो यह उसके लिए सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित होने वाला है। विधेय मार्ग तो यही है, इसे कोई भी विवेकी अस्वीकार नहीं कर
१. मोक्षमार्गप्रकाशक (दि० जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़) पृ० २५५-५६ २. मोक्षमार्गप्रकाशक (दि० जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़) पृ० २५३-५४
प्रस्तावना | ३१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org