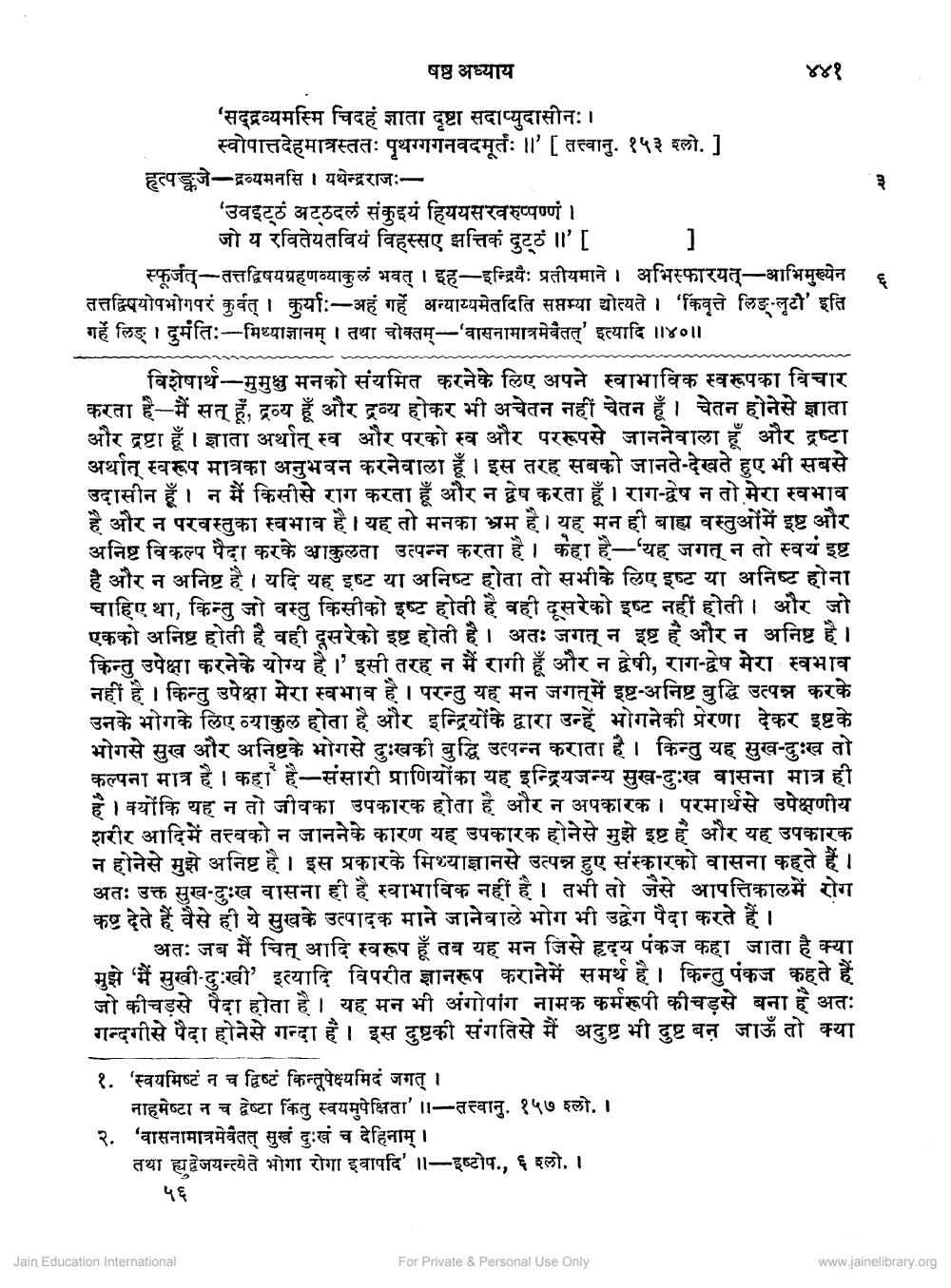________________
षष्ठ अध्याय
४४१
'सद्व्यमस्मि चिदहं ज्ञाता दृष्टा सदाप्युदासीनः ।
स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः पृथग्गगनवदमूर्तः ॥' [ तत्त्वानु. १५३ श्लो. ] हृत्पङ्कजे-द्रव्यमनसि । यथेन्द्रराजः
'उवइट्ठ अठदलं संकुइयं हिययसरवरुप्पण्णं ।
जो य रवितेयतवियं विहस्सए झत्तिकं दुट्ठ ॥ [ ] स्फूर्जत्-तत्तद्विषयग्रहणव्याकुलं भवत् । इह-इन्द्रियैः प्रतीयमाने । अभिस्फारयत्-आभिमुख्येन ६ तत्तद्विषयोपभोगपरं कुर्वत् । कुर्या:-अहं गहें अन्याय्यमेतदिति सप्तम्या द्योत्यते । “किंवृत्ते लिङ्-लुटौ' इति गहें लिङ् । दुर्मतिः-मिथ्याज्ञानम् । तथा चोक्तम्-'वासनामात्रमेवैतत्' इत्यादि ॥४०॥
विशेषार्थ-मुमुक्षु मनको संयमित करने के लिए अपने स्वाभाविक स्वरूपका विचार करता है-मैं सत् हूँ, द्रव्य हूँ और द्रव्य होकर भी अचेतन नहीं चेतन हूँ। चेतन होनेसे ज्ञाता और द्रष्टा हूँ । ज्ञाता अर्थात् स्व और परको स्व और पररूपसे जाननेवाला हूँ और द्रष्टा अर्थात् स्वरूप मात्रका अनुभवन करनेवाला हूँ। इस तरह सबको जानते-देखते हुए भी सबसे उदासीन हूँ। न मैं किसीसे राग करता हूँ और न द्वेष करता हूँ। राग-द्वेष न तो मेरा स्वभाव है और न परवस्तुका स्वभाव है। यह तो मनका भ्रम है। यह मन ही बाह्य वस्तुओंमें इष्ट और अनिष्ट विकल्प पैदा करके आकुलता उत्पन्न करता है। कहा है-'यह जगत् न तो स्वयं इष्ट है और न अनिष्ट है। यदि यह इष्ट या अनिष्ट होता तो सभीके लिए इष्ट या अनिष्ट होना चाहिए था, किन्तु जो वस्तु किसीको इष्ट होती है वही दूसरेको इष्ट नहीं होती। और जो एकको अनिष्ट होती है वही दूसरेको इष्ट होती है। अतः जगत् न इष्ट है और न अनिष्ट है। किन्तु उपेक्षा करनेके योग्य है।' इसी तरह न मैं रागी हूँ और न द्वेषी, राग-द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। किन्तु उपेक्षा मेरा स्वभाव है। परन्तु यह मन जगत्में इष्ट-निष्ट बुद्धि उत्पन्न करके उनके भोगके लिए व्याकुल होता है और इन्द्रियों के द्वारा उन्हें भोगनेकी प्रेरणा देकर इष्टके भोगसे सुख और अनिष्टके भोगसे दुःखकी बुद्धि उत्पन्न कराता है। किन्तु यह सुख-दुःख तो कल्पना मात्र है । कहा है-संसारी प्राणियोंका यह इन्द्रियजन्य सुख-दुःख वासना मात्र ही है। क्योंकि यह न तो जीवका उपकारक होता है और न अपकारक । परमार्थसे उपेक्षणीय शरीर आदिमें तत्त्वको न जाननेके कारण यह उपकारक होनेसे मुझे इष्ट है और यह उपकारक न होनेसे मुझे अनिष्ट है। इस प्रकारके मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारको वासना कहते हैं। अतः उक्त सुख-दुःख वासना ही है स्वाभाविक नहीं है। तभी तो जैसे आपत्तिकालमें रोग कर देते हैं वैसे ही ये सुखके उत्पादक माने जानेवाले भोग भी उद्वेग पैदा करते हैं।
अतः जब मैं चित् आदि स्वरूप हूँ तब यह मन जिसे हृदय पंकज कहा जाता है क्या मुझे 'मैं सुखी-दुःखी' इत्यादि विपरीत ज्ञानरूप कराने में समर्थ है। किन्तु पंकज कहते हैं जो कीचड़से पैदा होता है। यह मन भी अंगोपांग नामक कर्मरूपी कीचड़से बना है अतः गन्दगीसे पैदा होनेसे गन्दा है। इस दुष्टकी संगतिसे मैं अदुष्ट भी दुष्ट बन जाऊँ तो क्या
१. 'स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तपेक्ष्यमिदं जगत् ।
नाहमेष्टा न च द्वेष्टा किंतु स्वयमुपेक्षिता' ।।-तत्त्वानु. १५७ श्लो. । २. 'वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् ।।
तथा ह्यद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि' ।-इष्टोप., ६ श्लो. ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org