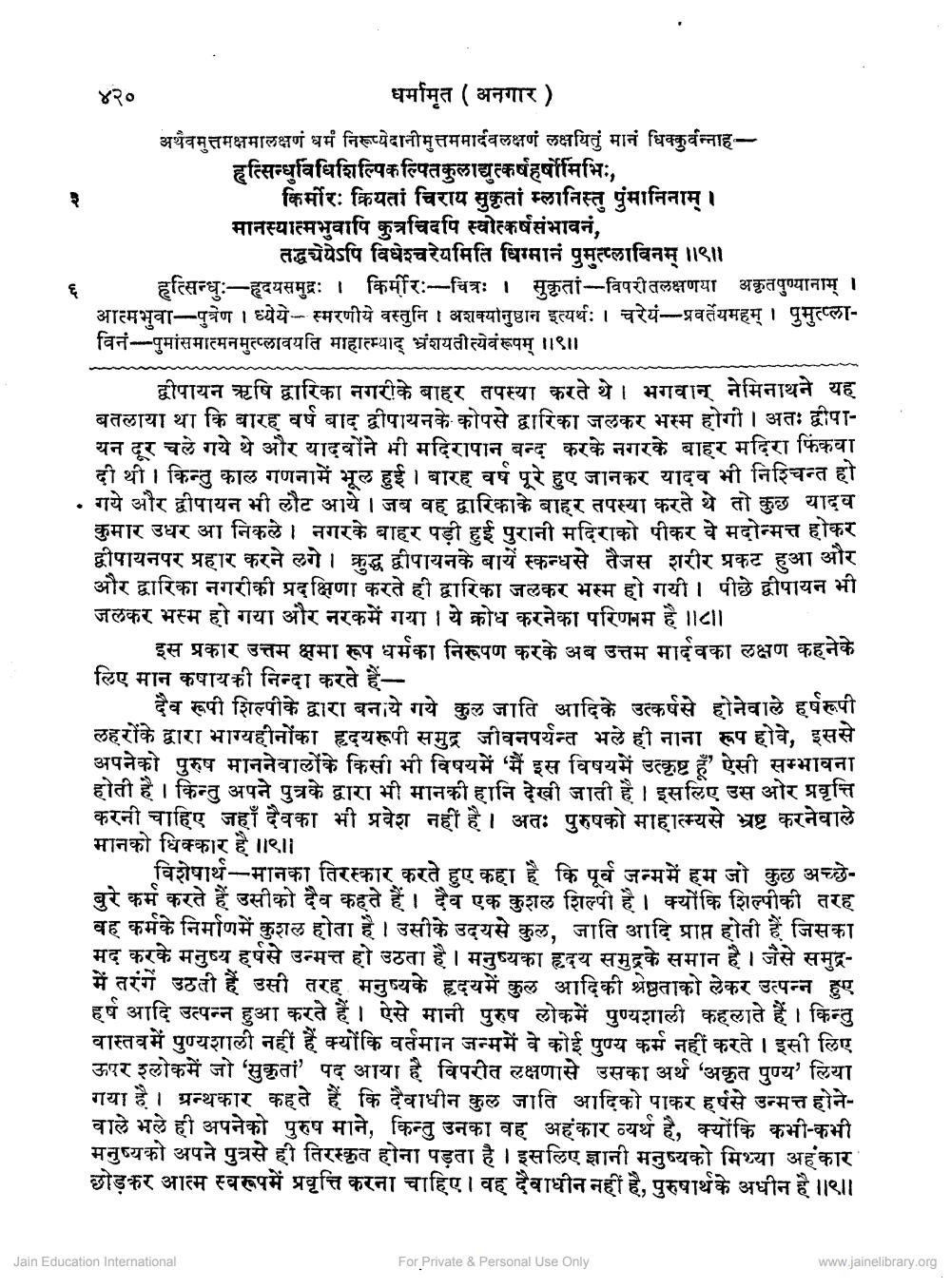________________
४२०
धर्मामृत ( अनगार) अथैवमुत्तमक्षमालक्षणं धर्म निरूप्येदानीमुत्तममार्दवलक्षणं लक्षयितुं मानं धिक्कुर्वन्नाह
हृत्सिन्धुविधिशिल्पिकल्पितकुलाद्युत्कर्षहर्षोमिभिः,
किर्मीरः क्रियतां चिराय सुकृतां म्लानिस्तु घुमानिनाम् । मानस्यात्मभुवापि कुत्रचिदपि स्वोत्कर्षसंभावनं,
तद्धयेयेऽपि विधेश्चरेयमिति धिग्मानं पुमुत्प्लाविनम् ॥९॥ हृत्सिन्धुः-हृदयसमुद्रः । किर्मीर:-चित्रः । सूकृतां-विपरीतलक्षणया अकृतपुण्यानाम् । आत्मभुवा-पुत्रेण । ध्येये-- स्मरणीये वस्तुनि । अशक्योनुष्ठान इत्यर्थः । चरेयं-प्रवर्तेयमहम् । पुमुत्प्लाविनं-पुमांसमात्मनमुत्प्लावयति माहात्म्याद् भ्रंशयतीत्येवंरूपम् ।।९॥
द्वीपायन ऋषि द्वारिका नगरीके बाहर तपस्या करते थे। भगवान् नेमिनाथने यह बतलाया था कि बारह वर्ष बाद द्वीपायनके कोपसे द्वारिका जलकर भस्म होगी। अतः द्वीपायन दूर चले गये थे और यादवोंने भी मदिरापान बन्द करके नगरके बाहर मदिरा फिंकवा दी थी। किन्तु काल गणनामें भूल हुई। बारह वर्ष पूरे हुए जानकर यादव भी निश्चिन्त हो • गये और द्वीपायन भी लौट आये । जब वह द्वारिकाके बाहर तपस्या करते थे तो कुछ यादव कुमार उधर आ निकले। नगरके बाहर पड़ी हुई पुरानी मदिराको पीकर वे मदोन्मत्त होकर द्वीपायनपर प्रहार करने लगे। क्रुद्ध द्वीपायनके बायें स्कन्धसे तैजस शरीर प्रकट हुआ और और द्वारिका नगरीकी प्रदक्षिणा करते ही द्वारिका जलकर भस्म हो गयी। पीछे द्वीपायन भी जलकर भस्म हो गया और नरकमें गया । ये क्रोध करनेका परिणाम है ॥८॥
इस प्रकार उत्तम क्षमा रूप धर्मका निरूपण करके अब उत्तम मार्दवका लक्षण कहनेके लिए मान कषायकी निन्दा करते हैं
दैव रूपी शिल्पीके द्वारा बनाये गये कुल जाति आदिके उत्कर्षसे होनेवाले हर्षरूपी लहरोंके द्वारा भाग्यहीनोंका हृदयरूपी समद जीवनपर्यन्त भले ही नाना रूप है
नपर्यन्त भले ही नाना रूप होवे, इससे अपनेको पुरुष माननेवालोंके किसी भी विषयमें 'मैं इस विषयमें उत्कृष्ट हूँ ऐसी सम्भावना होती है । किन्तु अपने पुत्रके द्वारा भी मानकी हानि देखी जाती है । इसलिए उस ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए जहाँ दैवका भी प्रवेश नहीं है। अतः पुरुषको माहात्म्यसे भ्रष्ट करनेवाले मानको धिक्कार है ॥९॥
विशेषार्थ-मानका तिरस्कार करते हुए कहा है कि पूर्व जन्म में हम जो कुछ अच्छेबुरे कर्म करते हैं उसीको दैव कहते हैं। दैव एक कुशल शिल्पी है। क्योंकि शिल्पीकी तरह वह कर्मके निर्माणमें कुशल होता है । उसीके उदयसे कुल, जाति आदि प्राप्त होती हैं जिसका मद करके मनुष्य हर्षसे उन्मत्त हो उठता है । मनुष्यका हृदय समुद्रके समान है । जैसे समुद्रमें तरंगें उठती हैं उसी तरह मनुष्यके हृदयमें कुल आदिकी श्रेष्ठताको लेकर उत्पन्न हुए हर्ष आदि उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसे मानी पुरुष लोकमें पुण्यशाली कहलाते हैं । किन्तु वास्तव में पुण्यशाली नहीं हैं क्योंकि वर्तमान जन्ममें वे कोई पुण्य कर्म नहीं करते । इसी लिए ऊपर श्लोकमें जो 'सुकृतां' पद आया है विपरीत लक्षणासे उसका अर्थ 'अकृत पुण्य' लिया गया है। ग्रन्थकार कहते हैं कि दैवाधीन कुल जाति आदिको पाकर हर्षसे उन्मत्त होनेवाले भले ही अपनेको पुरुष माने, किन्तु उनका वह अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि कभी-कभी मनुष्यको अपने पुत्रसे ही तिरस्कृत होना पड़ता है । इसलिए ज्ञानी मनुष्यको मिथ्या अहंकार छोड़कर आत्म स्वरूपमें प्रवृत्ति करना चाहिए। वह दैवाधीन नहीं है, पुरुषार्थके अधीन है ॥९॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org