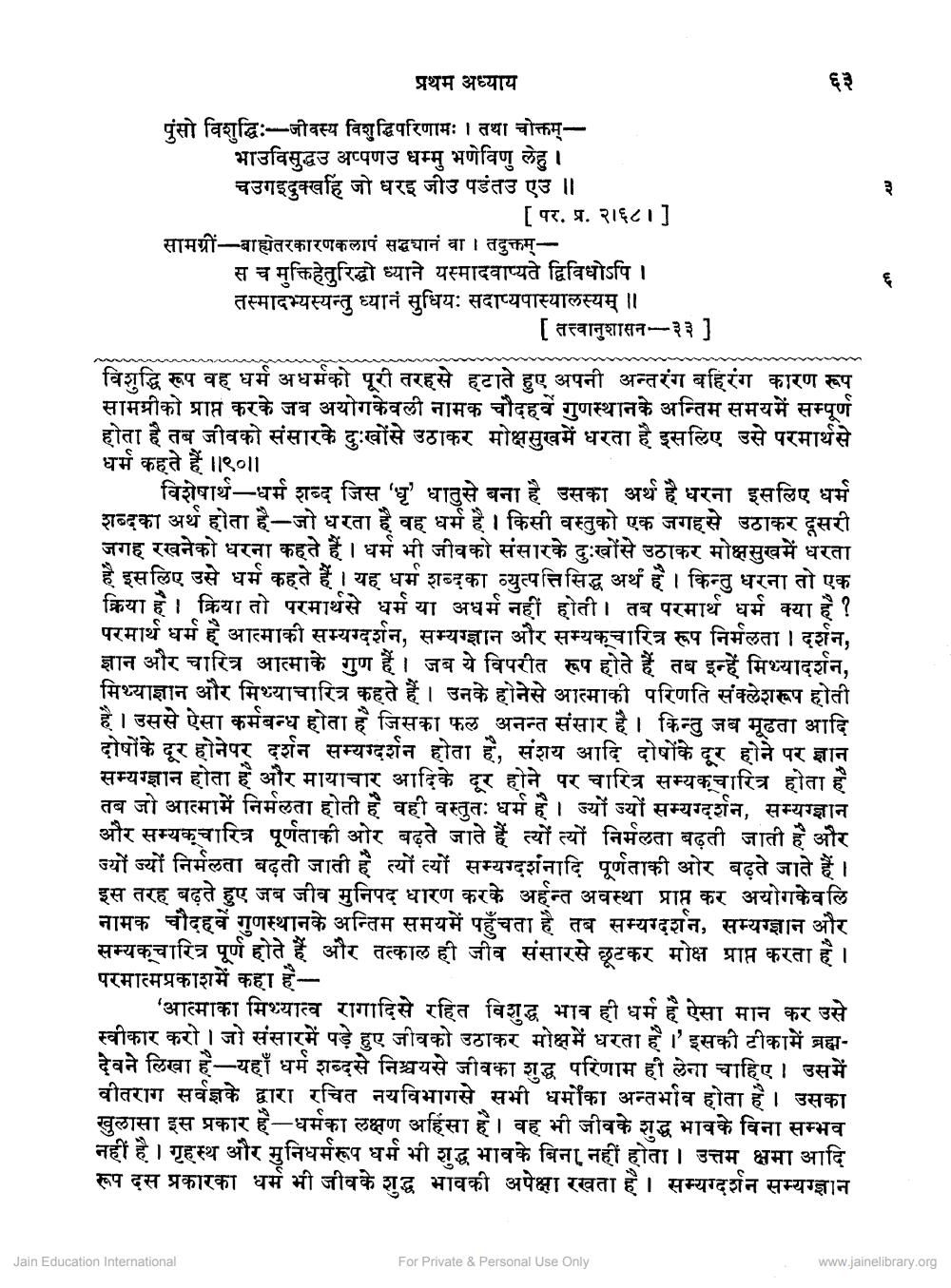________________
प्रथम अध्याय
पुंसो विशुद्धि: - जीवस्य विशुद्धिपरिणामः । तथा चोक्तम्भावसुद्ध अप्पण धम्मु भणेविणु लेहु । चउगइदुक्खहि जो धरइ जीउ पडतउ एउ |
[ पर. प्र. २।६८ । ]
सामग्री - बाह्येतर कारणकलापं सद्धघानं वा । तदुक्तम्स च मुक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोऽपि । तस्मादभ्यस्यन्तु ध्यानं सुधियः सदाप्यपास्यालस्यम् ॥ [ तत्त्वानुशासन - ३३ ]
विशुद्ध रूप वह धर्म अधर्मको पूरी तरहसे हटाते हुए अपनी अन्तरंग बहिरंग कारण रूप सामग्रीको प्राप्त करके जब अयोगकेवली नामक चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समय में सम्पूर्ण होता है तब जीवको संसारके दुःखोंसे उठाकर मोक्षसुखमें धरता है इसलिए उसे परमार्थ से धर्म कहते हैं ||२०||
विशेषार्थ - धर्म शब्द जिस 'धृ' धातुसे बना है उसका अर्थ है धरना इसलिए धर्म शब्दका अर्थ होता है - जो धरता है वह धर्म है। किसी वस्तुको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखनेको धरना कहते हैं । धर्म भी जीवको संसारके दुःखोंसे उठाकर मोक्षसुखमें धरता है इसलिए उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म शब्दका व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ है । किन्तु धरना तो एक क्रिया है । क्रिया तो परमार्थसे धर्म या अधर्म नहीं होती । तब परमार्थ धर्म क्या है ? परमार्थ धर्म है आत्माकी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्र रूप निर्मलता । दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्माके गुण हैं। जब ये विपरीत रूप होते हैं तब इन्हें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कहते हैं । उनके होनेसे आत्माकी परिणति संक्लेशरूप होती है । उससे ऐसा कर्मबन्ध होता है जिसका फल अनन्त संसार है । किन्तु जब मूढता आदि दोषोंके दूर होनेपर दर्शन सम्यग्दर्शन होता है, संशय आदि दोषोंके दूर होने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है और मायाचार आदिके दूर होने पर चारित्र सम्यक चारित्र होता है। तब जो आत्मा में निर्मलता होती है वही वस्तुतः धर्म है । ज्यों ज्यों सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्णताकी ओर बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों निर्मलता बढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों निर्मलता बढ़ती जाती है त्यों त्यों सम्यग्दर्शनादि पूर्णताकी ओर बढ़ते जाते हैं । इस तरह बढ़ते हुए जब जीव मुनिपद धारण करके अर्हन्त अवस्था प्राप्त कर अयोगकेवलि नामक चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें पहुँचता है तब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र पूर्ण होते हैं और तत्काल ही जीव संसारसे छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है । परमात्मप्रकाश में कहा है
Jain Education International
६३
'आत्माका मिथ्यात्व रागादिसे रहित विशुद्ध भाव ही धर्म है ऐसा मान कर उसे स्वीकार करो । जो संसार में पड़े हुए जीवको उठाकर मोक्षमें धरता है।' इसकी टीका में ब्रह्मदेवने लिखा है - यहाँ धर्म शब्दसे निश्चयसे जीवका शुद्ध परिणाम ही लेना चाहिए। उसमें वीतराग सर्वज्ञके द्वारा रचित नयविभागसे सभी धर्मोंका अन्तर्भाव होता है । उसका खुलासा इस प्रकार है - धर्मका लक्षण अहिंसा है । वह भी जीवके शुद्ध भाव के बिना सम्भव नहीं है। गृहस्थ और मुनिधर्मरूप धर्म भी शुद्ध भाव के बिना नहीं होता। उत्तम क्षमा आदि रूप दस प्रकारका धर्म भी जीवके शुद्ध भावकी अपेक्षा रखता है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
For Private & Personal Use Only
३
www.jainelibrary.org